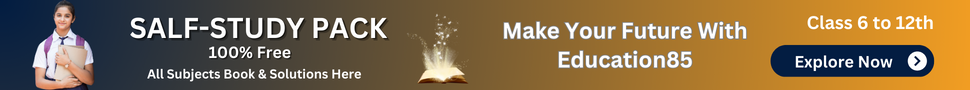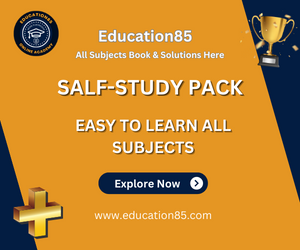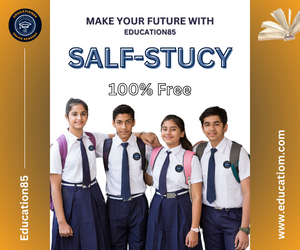“वाख” महादेवी वर्मा की एक मार्मिक कविता है जो जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाती है। कविता में जीवन को सपने की तरह क्षणभंगुर, कमल के पत्ते पर टिकी हुई ओस की बूंदों जैसा नाशवान बताया गया है। समय का निरंतर प्रवाह और उसकी अनवरत गति जीवन को प्रभावित करती है, इस तथ्य को कविता में सुंदरता से व्यक्त किया गया है। कविता में जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज की भी झलक मिलती है, मनुष्य मृत्यु की अनिश्चितता के सामने जीवन में अर्थ खोजने का प्रयास करता है, यह तथ्य भी कविता में उजागर हुआ है। “वाख” में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे पाठक आसानी से कविता के भाव को ग्रहण कर सकते हैं। यह कविता पाठकों को जीवन के क्षणभंगुरता को समझने और वर्तमान क्षण को सराहने के लिए प्रेरित करती है।
प्रश्न- अभ्यास
1. ‘रस्सी’ यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है?
उत्तर :
कविता में ‘रस्सी’ की प्रकृति को अत्यंत नाजुक और क्षणभंगुर बताया गया है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने हाथों में नहीं रख सकते और जो किसी भी क्षण टूट सकती है। यह जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु की निश्चितता की ओर इशारा करता है।
2. कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं?
उत्तर :
“वाख” कविता में कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयास व्यर्थ प्रतीत होने के कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी आंतरिक अस्थिरता है। कवयित्री खुद को एक कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह चित्रित करती हैं, जो आसानी से टूट सकता है। यह उनकी आंतरिक कमजोरियों, अशांति और अस्थिरता को दर्शाता है। उनकी मनःस्थिति अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है, उनके मन में अभी भी कई तरह की बेचैनियाँ, भय और आसक्तियाँ हैं जो उन्हें मुक्ति के मार्ग पर स्थिर रहने से रोकती हैं। बचपन की बेचैनियाँ और उथल-पुथल भी उनकी आंतरिक शांति में बाधा बन रही हैं।
3. कवयित्री का ‘घर जाने की चाह’ से तात्पर्य है?
उत्तर :
“वाख” कविता में ‘घर जाने की चाह’ एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह कवयित्री की आंतरिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें वह अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने और एक उच्चतर सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करती है।
4. भाव स्पष्ट कीजिए-
(क) जेब टटोली कौड़ी न पाई ।
(ख) खा-खाकर कुछ पाएगा नहीं,
न खाकर बनेगा अहंकारी ।
Certainly! Here’s the answer in Hindi:
“जेब टटोली कौड़ी न पाई ।”
इस पंक्ति में कवयित्री ने गहरा निराशा व्यक्त की है। उन्होंने अपने जीवन में संचित धन-दौलत, भौतिक सुखों और सांसारिक उपलब्धियों को ‘जेब’ की संज्ञा दी है। इस ‘जेब’ को खंगालने पर उन्हें कोई सच्ची संतुष्टि या आंतरिक शांति नहीं मिली।
“खा-खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी ।”
इस पंक्ति में जीवन में संतुलन का महत्व बताया गया है। ‘खाना’ यहां केवल भोजन ही नहीं, बल्कि जीवन के भोगों, सुखों का प्रतीक है। अधिक भोग-विलास में लिप्त रहने से भी संतुष्टि नहीं मिलती, वहीं पूर्ण त्याग भी अहंकार को जन्म देता है। इस प्रकार, कविता संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है।
5. बंद द्वार की साँकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है?
उत्तर :
ललद्यद ने “वाख” में बंद द्वार की साँकल खोलने के लिए संतुलन का मार्ग सुझाया है। न तो अधिक भोग और न ही पूर्ण त्याग, बल्कि दोनों के बीच एक मध्य मार्ग अपनाना आवश्यक है। इस संतुलन से ही मन शांत होता है, सांसारिक बंधन टूटते हैं और आंतरिक द्वार खुलता है।
6. ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है ?
उत्तर :
“जेब टटोली कौड़ी न पाई।” इस पंक्ति से यह पता चलता है कि कवयित्री ने धन-दौलत और भौतिक सुखों में बहुत कुछ खो दिया है।
“खा-खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी।” इस पंक्ति से यह पता चलता है कि केवल भोग-विलास में लिप्त रहने से भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती।
7. ‘ज्ञानी’ से कवयित्री क्या अभिप्राय है?
उत्तर :
आध्यात्मिक ज्ञान: “ज्ञानी” संभवतः उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने भीतर की ओर देखा है और सत्य को जान लिया है।
जीवन अनुभव: “ज्ञानी” उस व्यक्ति को भी संदर्भित कर सकता है जिसने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है, जिसने जीवन के उतार-चढ़ाव देखे हैं और उनसे सबक सीखे हैं।
आंतरिक शांति: “ज्ञानी” वह व्यक्ति भी हो सकता है जिसने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है, जिसने अपने मन को शांत किया है और मोह-माया से मुक्त हो गया है।
रचना और अभिव्यक्ति
8. हमारे संतो, भक्तों और महापुरुषों ने बार-बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है- (क) आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है ? (ख) आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए।
उत्तर :
हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि सभी मनुष्य समान हैं, फिर भी आज भी हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग, रंग और अन्य आधारों पर भेदभाव व्याप्त है। यह एक गंभीर समस्या है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं।
(क) भेदभाव से देश और समाज को होने वाली हानि
- सामाजिक एकता कमजोर होती है: भेदभाव समाज में अविश्वास और द्वेष पैदा करता है, जिससे सामाजिक एकता कमजोर होती है।
- विकास में बाधा: भेदभाव के कारण समाज के कुछ वर्ग विकास से वंचित रह जाते हैं, जिससे समग्र विकास बाधित होता है।
- अशांति और हिंसा: भेदभाव अक्सर सांप्रदायिक दंगों और हिंसा का कारण बनता है।
- मानवाधिकारों का हनन: भेदभाव मानवाधिकारों का हनन है और यह व्यक्ति के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाता है।
- देश की छवि खराब होती है: भेदभाव से देश की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब होती है।
(ख) भेदभाव मिटाने के लिए सुझाव
- शिक्षा का प्रसार: शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को यह समझाना होगा कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव गलत है।
- समाज में सकारात्मक बदलाव: समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सभी वर्गों के लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा।
- कानून का प्रभावी कार्यान्वयन: भेदभाव के खिलाफ बने कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।
- मीडिया की भूमिका: मीडिया को समाज में सद्भावना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
- धार्मिक नेताओं की भूमिका: धार्मिक नेताओं को भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और लोगों को एकता का संदेश देना चाहिए।
- सरकारी नीतियां: सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो भेदभाव को खत्म करने में मदद करें।