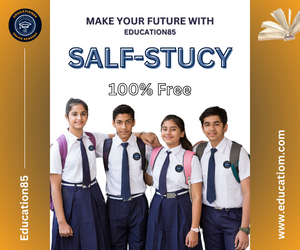मीरा बाई की यह वाणी उनके हृदय की गहराई से निकली हुई एक सच्ची पुकार है, जो सीधे उनके प्रियतम श्रीकृष्ण तक पहुँचती है। “मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई” यह केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि मीरा के अटूट विश्वास और प्रेम का सार है। वे इस संसार में किसी और को अपना नहीं मानतीं, उनके जीवन का एकमात्र सत्य, एकमात्र सहारा तो गिरिधर गोपाल ही हैं।
इस प्रेम की अनन्यता में मीरा ने सांसारिक बंधनों को बड़ी सहजता से तोड़ दिया है। कुल की मर्यादा, परिवार की प्रतिष्ठा, ये सब उनके कृष्ण प्रेम के आगे फीके पड़ गए। उन्हें अब इस बात की कोई चिंता नहीं कि दुनिया उनके बारे में क्या कहती है। उनकी तो अब एक ही चाह है, साधु-संतों की संगति में रहना और कृष्ण की भक्ति के रस में डूबे रहना। भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए उन्होंने लोक-लाज और संकोच को भी तिलांजलि दे दी है।
मीरा बाई अपनी भावनाओं को और खोलकर व्यक्त करती हैं। जब वह भगवान के सच्चे भक्तों को देखती हैं, तो उनका मन आनंद से भर उठता है। वहीं दूसरी ओर, सांसारिक मोह-माया में फंसे लोगों को देखकर उन्हें दुख होता है। उन्होंने अपने प्रेम के आंसुओं से कृष्ण-प्रेम की बेल को सींचा है। यह उनके अथक प्रेम और समर्पण का ही फल है कि अब उस बेल पर आनंद के मीठे फल लगने लगे हैं, जिससे उनके हृदय को परम शांति और सुख की अनुभूति हो रही है।
अंत में, मीरा स्वयं को गिरिधर गोपाल की दासी बताती हैं और बड़ी ही विनम्रता से उनसे प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हें इस भवसागर से पार लगाएं और अपनी शरण में ले लें। इस पूरी रचना में मीरा बाई की कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति, सांसारिक बंधनों से मुक्ति की तीव्र इच्छा और पूर्ण समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। यह कविता उनके गहरे प्रेम और आध्यात्मिक यात्रा का एक सुंदर और हृदयस्पर्शी चित्रण है।
पद के साथ
1)मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है?
उत्तर:मीरा कृष्ण को अपना प्रेमी और स्वामी मानती हैं। उनका प्रेम निश्छल और अनन्य भक्ति से भरा है। कृष्ण उनके लिए मुरलीधर, श्यामसुंदर और सखा हैं। मीरा के हृदय में बसने वाले कृष्ण मनोहर रूप में हैं—बाँसुरी बजाते, मोरपंख लगाए, पीताम्बर पहने और मुस्कुराते हुए। वे ही उनका सब कुछ हैं।
2)भाव व शिल्प-सौंदर्य स्पष्ट कीजिए-
(क)अंसुवन जल सींचि-सीचि, प्रेम-बेलि बोयी
अब त बेलि फैलि गई आणंद-फल होयी
(ख)दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोयी
दधि मथि घृत काढ़ि लियो, डारि दयी छोयी
उत्तर:(क) प्रेम-बेल का चित्रण
भाव-सौंदर्य: इन पंक्तियों में कवि ने प्रेम को एक बेल के रूप में दर्शाया है, जिसे आँसुओं के जल से सींचकर बोया गया है। यह बेल अब इतनी फल-फूल गई है कि उससे आनंद रूपी फल मिल रहे हैं। यहाँ कवि ने प्रेम की निरंतर साधना और उसके मधुर परिणाम को दर्शाया है।
शिल्प-सौंदर्य: यहाँ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जहाँ प्रेम को ‘बेल’ और आनंद को ‘फल’ कहा गया है। “सींचि-सीचि” और “फैलि-फल” में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखती है। भाषा की दृष्टि से यह ब्रजभाषा की सरलता और मिठास से युक्त है।
(ख) भक्ति का मथन
भाव-सौंदर्य: इस उदाहरण में कवि ने भक्ति के सार को दूध मथने की प्रक्रिया से समझाया है। जैसे दही को मथने पर घी (सारतत्व) निकलता है और छाछ छोड़ दी जाती है, उसी प्रकार सच्ची भक्ति से जीवन का वास्तविक आनंद और सार प्राप्त होता है, और व्यर्थ की चीजें छूट जाती हैं।
शिल्प-सौंदर्य: यहाँ भी रूपक अलंकार का प्रभावी प्रयोग है, जहाँ भक्ति को ‘दूध मथना’ और उसके सार को ‘घी’ बताया गया है। “मथनियाँ”, “विलोयी”, “छोयी” जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग लोकजीवन से जुड़ाव दिखाता है। यह पद दोहा छंद में रचित है, जिससे इसमें गेयता और लयबद्धता है।
सारांश: कबीरदास जी ने इन दोनों पदों में प्रेम और भक्ति के गहन आध्यात्मिक अनुभवों को दैनंदिन जीवन के सरल उदाहरणों और रूपकों के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है।
3)मीरा जगत को देखकर रोती क्यों हैं?
उत्तर:मीराबाई संसार की नश्वरता और मायावी स्वरूप को देखकर रोती हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि लोग क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं और भगवान कृष्ण की सच्ची भक्ति से विमुख हैं। मीरा को यह स्पष्ट हो गया था कि यह संसार असत्य है और यहाँ सब कुछ नाशवान है, जबकि लोग इसी को सत्य मानकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनका रोना संसार के प्रति उनकी करुणा और ईश्वर प्रेम का प्रतीक है।
पद के आसपास
1)कल्पना करें, प्रेम-प्राप्ति के लिए मीरा को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा?
उत्तर:मीरा को कृष्ण-भक्ति के लिए कई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं। राजपरिवार और समाज ने उनके संन्यासी जीवन को नहीं स्वीकारा। परिवार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि जहर देने जैसे प्रयास भी हुए। लोगों ने उनकी भक्ति को पागलपन कहा और उनका उपहास उड़ाया। तीर्थयात्राओं के दौरान उन्हें शारीरिक कष्ट भी सहने पड़े। लेकिन मीरा ने हर बाधा पार कर कृष्ण के प्रति अपना अटूट प्रेम दिखाया।
2)लोक-लाज खोने का अभिप्राय क्या है?
उत्तर:सही कहा गया है कि मीराबाई का जीवन “लोक-लाज खोना” मुहावरे का सटीक उदाहरण है। एक शाही बहू होते हुए भी, उन्होंने सामाजिक अपेक्षाओं के विपरीत महलों का त्याग कर कृष्ण भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने मंदिरों में नाचा-गाया और साधु-संतों के साथ समय बिताया, जो उस समय के सामाजिक नियमों के विरुद्ध था और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाता था। लोगों की निंदा की परवाह किए बिना, मीराबाई ने अपनी अटूट कृष्ण भक्ति को प्राथमिकता दी, जिससे उन्होंने सांसारिक शर्म और संकोच का त्याग कर दिया। उनके भजन उनकी इसी बेफिक्री और दृढ़ भक्ति के प्रमाण हैं। इस प्रकार, मीराबाई ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए लोक-लाज का पूर्णतः त्याग किया।