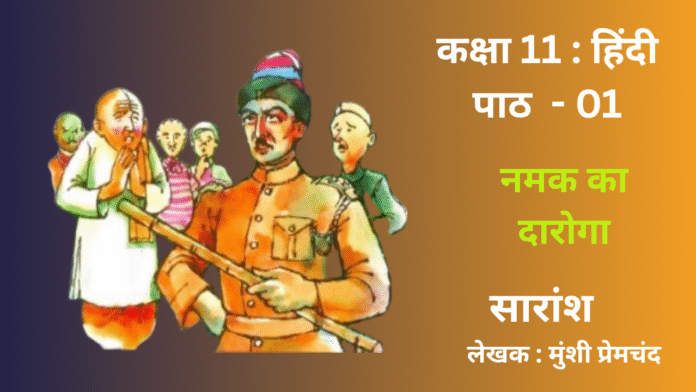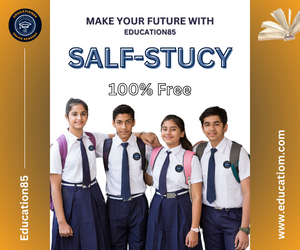मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना “नमक का दारोगा” सचमुच मानवीय मूल्यों की एक ऐसी सशक्त गाथा है, जो आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। यह कहानी केवल एक समय विशेष की परिस्थितियों का चित्रण नहीं करती, बल्कि यह जीवन के एक शाश्वत सत्य को उजागर करती है कि अंततः ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ही विजयी होती हैं,कहानी का वह दौर जब नमक विभाग नया-नया बना था और ऊपरी कमाई का लालच लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, एक ऐसे सामाजिक परिवेश को दर्शाता है जहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें तेज़ी से फैल रही थीं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में, मुंशी वंशीधर का नौकरी की तलाश में निकलना और उनके पिता द्वारा भी रिश्वत लेने की सलाह देना, उस दौर की कड़वी सच्चाई को बयान करता है। इसके विपरीत, वंशीधर का अपनी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता पर अडिग रहना एक उम्मीद की किरण जगाता है। उनकी निष्ठा ही उन्हें नमक विभाग में दारोगा की प्रतिष्ठित नौकरी दिलाती है और जल्द ही वे अपने अधिकारियों का विश्वास जीत लेते हैं।
कहानी में मोड़ तब आता है जब वंशीधर रात के अंधेरे में पंडित अलोपीदीन की नमक से लदी गाड़ियों को पकड़ते हैं। पंडित अलोपीदीन, जो उस क्षेत्र के एक प्रभावशाली और धनी व्यक्ति थे, अपनी शक्ति और धन के मद में चूर थे। उनका वंशीधर को रिश्वत की पेशकश करना और वंशीधर का दृढ़ता से इनकार करना, सत्य और असत्य के बीच एक तीखे संघर्ष को दर्शाता है। वंशीधर का पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करना एक साहसिक कदम था, जिसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया।
लेकिन, यह भी एक सच्चाई है कि अक्सर धन और प्रभाव के आगे ईमानदारी कमजोर पड़ जाती है। पंडित अलोपीदीन ने अपनी दौलत के बल पर अदालत में खुद को निर्दोष साबित कर दिया, जबकि वंशीधर को अपनी ईमानदारी की कीमत अपनी नौकरी खोकर चुकानी पड़ी। जब वे निराश और दुखी होकर घर लौटते हैं और अपने पिता की नाराजगी का सामना करते हैं, तो यह दृश्य हमें दिखाता है कि समाज में ईमानदारी का मार्ग कितना कठिन हो सकता है।
कहानी का अंत एक सुखद आश्चर्य लेकर आता है। पंडित अलोपीदीन का स्वयं वंशीधर के घर आना और उनकी अटूट ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त करने का प्रस्ताव रखना, एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह घटना दर्शाती है कि भले ही भ्रष्ट लोग अपनी शक्ति और धन के मद में अंधे हों, लेकिन कहीं न कहीं वे एक ईमानदार व्यक्ति के गुणों का सम्मान जरूर करते हैं।
प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से मानवीय मूल्यों के एक ऐसे उज्जवल आदर्श को हमारे सामने रखा है, जो आज भी हमें सही राह दिखाता है और प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलें। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत चरित्र और ईमानदारी है, जो समय के साथ और भी मूल्यवान होती जाती है।
पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न
पाठ के साथ
1) कहानी का कौन-सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों?
उत्तर-मुंशी वंशीधर इस कहानी के सबसे प्रभावशाली पात्र हैं। उनकी अटल सत्यनिष्ठा उस समय में भी कायम रहती है, जब हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था। प्रचुर रिश्वत के प्रस्तावों के बावजूद, वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं, जो वर्तमान मूल्यों के पतन के दौर में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
उनका साहस और निडरता भी सराहनीय है। पंडित अलोपीदीन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को बंदी बनाना आसान निर्णय नहीं था, खासकर जब इसके संभावित दुष्परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता था। फिर भी, वंशीधर बिना किसी भय के अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं।
वंशीधर का चरित्र एक आदर्शवादी सोच प्रस्तुत करता है। वे मानते हैं कि नैतिक सिद्धांत भौतिक लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपनी नौकरी खोने के बावजूद, वे अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होते।
उनकी मानवीय दुर्बलता भी दिखती है जब वे अपनी नौकरी खोने पर निराश और दुखी होते हैं, जो उनके चरित्र को और भी वास्तविक बनाती है।
अंततः, पंडित अलोपीदीन द्वारा उनकी ईमानदारी का आदर करना और उन्हें उच्च पद पर नियुक्त करना यह दर्शाता है कि सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य अंततः स्थापित होता है।
संक्षेप में, मुंशी वंशीधर का चरित्र ईमानदारी, हिम्मत, आदर्शवाद और मानवीय पहलुओं का एक अद्भुत मिश्रण है, जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया और यह विश्वास दिलाया कि ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, उसका महत्व हमेशा बना रहता है।
2)‘नमक का दरोगा’ कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन-से दो पहलू (पक्ष) उभरकर आते हैं?
उत्तर-नमक का दरोगा’ कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो मुख्य पहलू उभरकर सामने आते हैं:
- भ्रष्ट और धन-लोलुप व्यापारी: कहानी के आरंभ में अलोपीदीन एक ऐसे व्यापारी के रूप में प्रस्तुत होते हैं जो धन के बल पर किसी भी कानून या नैतिकता को तोड़ने को तैयार रहते हैं। वे नमक के अवैध व्यापार में संलिप्त हैं और मुंशी वंशीधर को खरीदने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका भ्रष्ट और लालची स्वभाव स्पष्ट होता है।
- गुणग्राही और सम्मानजनक व्यक्ति: कहानी के उत्तरार्ध में अलोपीदीन का दूसरा पहलू सामने आता है। वंशीधर की ईमानदारी और दृढ़ता से प्रभावित होकर, वे उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं और उन्हें अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी प्रबंधक नियुक्त करते हैं। यह दर्शाता है कि वे गुणों की कद्र करने वाले और सही व्यक्ति को सम्मान देने वाले इंसान भी थे, भले ही उनके स्वयं के तरीके पहले भ्रष्ट रहे हों।
3)कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी-न-किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उदधृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं-
(क) वृदध मुंशी
(ख) वकील
(ग) शहर की भीड़
उत्तर-(क) वृद्ध मुंशी की बातें: यथार्थ का कड़वा सच
वृद्ध मुंशी का कथन उस दौर की गरीबी और बढ़ती ज़िम्मेदारियों के दबाव में ईमानदारी के कमजोर पड़ने का यथार्थ दिखाता है। ‘महीने की पगार’ और ‘ऊपरी आय’ की उनकी तुलना रिश्वतखोरी को एक सामान्य और स्वीकार्य प्रथा बनाने की कोशिश थी। यह सोच आज भी मौजूद है, जहाँ लोग ‘ज़रूरत’ के नाम पर अनैतिक तरीके अपनाते हैं।
(ख) वकील का चरित्र: धन और न्याय का खेल
वकील का कृत्य न्याय व्यवस्था में धन और प्रभाव की भूमिका को उजागर करता है। पंडित अलोपीदीन का बचाव यह दिखाता है कि पैसे के बल पर सच को भी झुठलाया जा सकता है। यह आज भी एक दुखद सच्चाई है जहाँ शक्तिशाली लोग अपनी पहुँच और पैसे के दम पर कानून से बच निकलते हैं, जबकि गरीब को छोटी गलती पर भी कठोर सज़ा मिलती है।
(ग) शहर की भीड़: तमाशे वाली मानसिकता
शहर की भीड़ समाज की सनसनीखेज़ खबरों में दिलचस्पी और क्षणिक कौतूहल को दर्शाती है। पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी में देखकर उनका आश्चर्य स्वाभाविक था, पर यह केवल एक तमाशा देखने वाली मानसिकता थी। यह भीड़ न तो वंशीधर की ईमानदारी का समर्थन करती है और न ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। यह सिर्फ ऊपरी दिखावे और प्रतिष्ठा को महत्व देने वाले समाज का प्रतिबिंब है।
4)निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए-
नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूँढ़ना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता हैं और घटते-घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत हैं जिससे सदैव प्यास बुझती हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्ध नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती हैं, तुम स्वय विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊ।
(क) यह किसकी उक्ति है?
(ख) मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है?
(ग) क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं?
उत्तर-(क) यह कथन किसी अनुभवी पिता की ही गहरी समझ को दर्शाता है, जो जीवन की वास्तविकताओं से पूरी तरह वाकिफ़ है। इसमें व्यावहारिक ज्ञान और जीवन के कठिन अनुभवों की छाप साफ़ झलकती है। पिता द्वारा बेटे को नौकरी की सच्चाई से रूबरू कराना न सिर्फ़ उसकी फिक्र को दिखाता है, बल्कि उसके जीवन भर की सीख का सार भी है।
(ख) मासिक वेतन की तुलना पूर्णिमा के चाँद से करना एक बेहद खूबसूरत और सार्थक उपमा है। जिस तरह चाँद पूरा होने के बाद धीरे-धीरे घटने लगता है, ठीक वैसे ही महीने की शुरुआत में मिला वेतन भी दिनोंदिन खत्म होता जाता है। यह उदाहरण वेतन की नश्वरता और उसके धीरे-धीरे खर्च होने की प्रक्रिया को बड़े ही सजीव ढंग से बयाँ करता है।
(ग) पिता का यह कहना कि “ऊपरी आमदनी भी ज़रूरी है” शायद कुछ लोगों को व्यावहारिक लगे, लेकिन मेरी नज़र में यह सही नहीं है। ऊपरी कमाई की इच्छा अक्सर अनैतिक रास्तों पर ले जाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। असली संतुष्टि और मन की शांति तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन में ही मिलती है। गलत तरीकों से कमाया पैसा भले ही थोड़े समय के लिए फायदा पहुँचाए, लेकिन आखिरकार यह पछतावे और अशांति का कारण बनता है।
5)‘नमक का दरोगा’ कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-“धर्म की विजय” कहानी के नैतिक सार को दर्शाता है – कि सच्चाई और ईमानदारी की अंततः जीत होती है। यह शीर्षक वंशीधर की नैतिक जीत को दिखाता है, जो अलोपीदीन के भ्रष्ट प्रभाव के खिलाफ खड़ा होता है।
वहीं, “सत्यनिष्ठ दारोगा” सीधे वंशीधर के चरित्र पर केंद्रित है। यह उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को सामने लाता है, जो कहानी का मुख्य संदेश है।
6)कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित- उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते?
उत्तर-
वंशीधर की ईमानदारी ने अलोपीदीन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें अपना प्रबंधक नियुक्त कर दिया। वंशीधर का घूस से इनकार करना और सिद्धांतों पर अडिग रहना अलोपीदीन के लिए अभूतपूर्व था। एक कुशल व्यवसायी के रूप में, अलोपीदीन ने समझा कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति ही उनके व्यापार को स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता दे सकता है।
कहानी के अंत में अलोपीदीन का वंशीधर को प्रस्ताव देना उनके हृदय परिवर्तन का प्रमाण है। यह उनके पिछले भ्रष्ट आचरण पर पश्चाताप और वंशीधर की सच्चाई के प्रति सम्मान को दर्शाता है।
एक वैकल्पिक अंत:
मेरी कल्पना में, कहानी का अंत और भी प्रभावी हो सकता था: वंशीधर प्रबंधक का पद इस शर्त पर स्वीकार करते कि वे किसी भी अनैतिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अलोपीदीन की सहमति उनके सच्चे बदलाव को दर्शाती। बाद में, वंशीधर अपनी ईमानदारी से व्यवसाय को नई ऊँचाईयों पर ले जाते, यह साबित करते हुए कि “सच्चाई और सिद्धांत ही वास्तविक सफलता की कुंजी हैं।”
पाठ के आस-पास
1)दारोगा वंशीधर गैरकानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते?
उत्तर-वंशीधर का पंडित अलोपीदीन के यहाँ मैनेजर की नौकरी स्वीकार करना कई मायनों में सही और गलत दोनों हो सकता है. इसे एक सीधा “हाँ” या “नहीं” जवाब देना कठिन है, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत मूल्यों और उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
इस फैसले के पीछे की अच्छी बातें
- ईमानदारी का सम्मान: यह दर्शाता है कि अलोपीदीन ने वंशीधर की ईमानदारी को अंततः पहचाना. यह समाज में एक सकारात्मक संदेश दे सकता है कि ईमानदारी का मोल होता है, भले ही इसे स्वीकार करने में समय लगे.
- आर्थिक सुरक्षा: वंशीधर को अपनी ईमानदारी की वजह से नौकरी गंवानी पड़ी थी, जिससे उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया होगा. अलोपीदीन का प्रस्ताव उनके परिवार को ज़रूरी आर्थिक स्थिरता देता.
- नैतिक मूल्यों की जीत: यह एक तरह से वंशीधर के नैतिक मूल्यों की अप्रत्यक्ष जीत थी. अलोपीदीन का उन्हें मैनेजर बनाना यह दर्शाता है कि ईमानदारी और सच्चाई में इतनी शक्ति है कि वह भ्रष्ट को भी झुकने पर मजबूर कर देती है.
- बदलाव का अवसर: वंशीधर ने सोचा होगा कि वे अलोपीदीन के व्यवसाय में ईमानदारी और नैतिकता लाने में मदद कर सकते हैं, शायद एक मार्गदर्शक के रूप में.
इस फैसले पर सवाल उठाने वाली बातें
- सिद्धांतों से समझौता: यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वंशीधर ने उसी व्यक्ति के यहाँ काम करना स्वीकार किया जिसने भ्रष्टाचार किया था. यह उनके सिद्धांतों से समझौता लग सकता है.
- भ्रष्टाचार का महिमामंडन: कुछ लोगों को यह लग सकता है कि भ्रष्टाचार ने अंत में जीत हासिल की, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को भ्रष्ट के अधीन काम करना पड़ रहा है. यह गलत संदेश दे सकता है.
- संदेश में अस्पष्टता: यह कहानी यह भी दिखा सकती है कि ईमानदारी सिर्फ तभी फल देती है जब शक्तिशाली लोग चाहें, जो निराशावादी हो सकता है.
अगर मैं वंशीधर की जगह होता
मैं भी तुरंत नौकरी स्वीकार नहीं करता. मेरा फैसला कुछ चीज़ों पर निर्भर करता:
- अलोपीदीन की नीयत: मैं सबसे पहले यह जानने की कोशिश करता कि अलोपीदीन का प्रस्ताव दिखावा है या उनमें सचमुच बदलाव आया है. अगर मुझे उनकी नीयत पर शक होता, तो मैं मना कर देता.
- परिवार की स्थिति: मैं अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों का आकलन करता. अगर वे बहुत मुश्किल में होते, तो मैं अपनी शर्तों के साथ इस पर विचार कर सकता था.
- दूरगामी प्रभाव: मैं यह सोचता कि मेरे इस फैसले का समाज पर क्या असर पड़ेगा. मैं ऐसा उदाहरण बनाना चाहता था जो ईमानदारी को बढ़ावा दे, न कि उसे कमज़ोर करे.
संक्षेप में, मैं बहुत सावधानी से सोचता. अगर मुझे पूरा भरोसा होता कि मैं अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूँ और अलोपीदीन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूँ, तभी मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करता. नहीं तो, मैं अपनी ईमानदारी और आत्म-सम्मान को बरकरार रखने के लिए किसी और मौके की तलाश करता.
2)नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों-बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन-सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों?
उत्तर-
नमक विभाग के दारोगा पद के लिए उस समय बड़ों-बड़ों का जी इसलिए ललचाता था क्योंकि उस विभाग में ऊपरी कमाई की अपार संभावनाएँ थीं। नमक जैसी आवश्यक वस्तु का नियंत्रण होने के कारण, अधिकारी आसानी से गैरकानूनी नमक के व्यापार से भारी रिश्वत कमा सकते थे। उस समय समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त था और ऊपरी आय को बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि कई लोग इसे अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे।
वर्तमान समाज में भी ऐसे कई पद हैं जिन्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे, और इसके कई कारण हैं:
- उच्च प्रशासनिक पद (IAS): भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) आज भी देश के सबसे प्रतिष्ठित और आकर्षक पदों में से एक है। इसे पाने के लिए लाखों युवा हर साल कड़ी मेहनत करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं:
- अधिकार और शक्ति: IAS अधिकारी सरकार की नीतियों को लागू करने और प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उन्हें समाज में काफी अधिकार और शक्ति मिलती है।
- सामाजिक प्रतिष्ठा: IAS अधिकारी को समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
- वेतन और अन्य लाभ: इन पदों पर आकर्षक वेतन, आवास, वाहन और अन्य कई प्रकार के सरकारी भत्ते और सुविधाएँ मिलती हैं।
- देश सेवा का अवसर: IAS अधिकारी देश और समाज की सेवा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।
- भारतीय पुलिस सेवा (IPS): यह पद भी युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके आकर्षण के कारण हैं:
- कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी: IPS अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उन्हें समाज की सुरक्षा में योगदान करने का अवसर मिलता है।
- रोमांच और चुनौती: इस सेवा में कार्य करने में रोमांच और चुनौतियाँ होती हैं जो कई युवाओं को आकर्षित करती हैं।
- सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति: IPS अधिकारियों को भी समाज में सम्मान और अधिकार प्राप्त होते हैं।
- वेतन और अन्य लाभ: इन पदों पर भी अच्छा वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएँ मिलती हैं।
- उच्च पदों पर सरकारी नौकरियाँ (अन्य विभाग): इसके अलावा, अन्य सरकारी विभागों में भी उच्च पदों पर नौकरियाँ जैसे कि भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS), सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में उच्च प्रबंधन के पद, और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) में अधिकारी पद भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इन पदों पर अच्छा वेतन, नौकरी की सुरक्षा, और अन्य लाभ मिलते हैं।
क्यों लोग इन पदों के लिए लालायित रहते हैं?
- आर्थिक सुरक्षा: सरकारी नौकरियाँ आमतौर पर निजी क्षेत्र की नौकरियों की तुलना में अधिक स्थिर और सुरक्षित मानी जाती हैं। उच्च पदों पर अच्छा वेतन और विभिन्न भत्ते मिलते हैं, जो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- सामाजिक प्रतिष्ठा: सरकारी पदों को समाज में उच्च सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। खासकर IAS और IPS जैसे पदों से जुड़ा रुतबा और सम्मान बहुत अधिक होता है।
- अधिकार और शक्ति: उच्च सरकारी पदों पर काम करने वाले अधिकारियों के पास नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार होता है, जिससे वे समाज पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं।
- अन्य लाभ और सुविधाएँ: सरकारी नौकरियों में पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा सुविधाएँ, आवास, वाहन और बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते जैसे कई अतिरिक्त लाभ मिलते हैं।
- देश सेवा का अवसर: कई लोग इन पदों को देश और समाज की सेवा करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं।
संक्षेप में, वर्तमान समाज में भी ऐसे कई उच्च सरकारी पद हैं जिन्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि ये पद आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, अधिकार और देश सेवा का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करते हैं।
3)अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तकों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो।
उत्तर-पुष्टि पूर्वाग्रह (Confirmation Bias) और आलोचनात्मक सोच
आपका अनुभव दर्शाता है कि हम अनजाने में कैसे उन्हीं तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच का समर्थन करते हैं। यह प्रवृत्ति हमें महत्वपूर्ण जानकारी या वैकल्पिक दृष्टिकोणों को नज़रअंदाज़ करने पर मजबूर कर सकती है, जिससे अक्सर गलत निष्कर्ष निकलते हैं।
इसी वजह से आलोचनात्मक सोच अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना, अपनी स्वयं की मान्यताओं पर सवाल उठाना, और विरोधी तर्कों को भी खुले दिमाग से सुनना—ये सभी हमें बेहतर निर्णय लेने और किसी भी समस्या को अधिक व्यापक रूप से समझने में सहायक होते हैं।
4)‘पढ़ना-लिखना सब अकारथ गया।’ वृद्ध मुंशी जी दवारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए-
(क) जब आपको पढ़ना-लिखना व्यर्थ लगा हो।
(ख) जब आपको पढ़ना-लिखना सार्थक लगा हो।
(ग) ‘पढ़ना’-लिखना’ को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा साक्षरता अथवा शिक्षा? (क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं?
उत्तर-पढ़ना-लिखना: व्यर्थता और सार्थकता का अनुभव
(क) जब पढ़ना-लिखना व्यर्थ लगा:
मुझे पढ़ना-लिखना तब व्यर्थ लगता है जब किताबी ज्ञान वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में अधूरा साबित होता है। खासकर तब, जब समाधान के लिए डिग्री से ज़्यादा व्यावहारिक कौशल या ‘पहचान’ की ज़रूरत पड़ती है, तो लगता है कि सीखा हुआ सिर्फ कागज़ तक सीमित रह गया।
(ख) जब पढ़ना-लिखना सार्थक लगा:
पढ़ना-लिखना मेरे लिए तब सार्थक होता है जब मैं अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी जटिल समस्या को सुलझाने में कर पाता हूँ। चाहे वह किसी बहस में तथ्यों के साथ अपनी बात रखना हो या किसी प्रोजेक्ट में विश्लेषण क्षमता से बेहतर परिणाम लाना हो। तभी महसूस होता है कि शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता भी देती है।
‘पढ़ना-लिखना’ का अर्थ: साक्षरता या शिक्षा?
(ग) यहाँ ‘पढ़ना-लिखना’ शब्द का प्रयोग शिक्षा के व्यापक अर्थ में किया गया है, न कि केवल साक्षरता के रूप में। वृद्ध मुंशी वंशीधर की उस समझ पर सवाल उठा रहे थे जो भ्रष्टाचार को गलत मानती थी।मैं साक्षरता और शिक्षा को समान नहीं मानता।साक्षरता केवल अक्षरों को पहचानना और बुनियादी लिखना-पढ़ना जानना है।शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसमें ज्ञान के साथ-साथ समझ, तर्कशक्ति, नैतिकता और जीवन जीने के कौशल का विकास भी शामिल है। कोई व्यक्ति साक्षर हो सकता है, पर अगर उसमें इन गुणों की कमी है, तो वह शिक्षित नहीं।
5)‘लड़कियाँ हैं, वह घास-फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं।’ वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है?
उत्तर-यह सच है कि लड़कियों को “घास-फूस” कहना सिर्फ उनकी कीमत कम आंकना नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व को ही अनावश्यक और बोझिल मानना दर्शाता है। जिस तरह अवांछित घास को हटाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार लड़कियों को भी एक ऐसी जिम्मेदारी समझा जाता था जिसे जल्द से जल्द ‘निपटा’ देना परिवार के लिए बेहतर माना जाता था। यह मानसिकता उस समय के समाज में गहरे तक बैठी पितृसत्तात्मक सोच का जीता-जागता प्रमाण है।
यह सोचना कितना दुखद है कि लड़कियों की परवरिश को लड़कों के समान महत्व नहीं दिया जाता था। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को अक्सर इसलिए अनदेखा कर दिया जाता था क्योंकि यह माना जाता था कि उनका असली घर तो ससुराल ही है। इस मानसिकता ने उन्हें अपने ही जन्म के घर में एक परायेपन का एहसास कराया होगा, जहाँ उन्हें स्थायी सदस्य के रूप में नहीं देखा जाता था। “बढ़ती चली जाती हैं” यह वाक्यांश उनकी बढ़ती उम्र और समाज में व्याप्त जल्द शादी की प्रथा की ओर स्पष्ट इशारा करता है। लड़कियों पर हमेशा यह सामाजिक दबाव बना रहता था कि उनकी शादी जितनी जल्दी हो सके कर दी जाए, मानो यही उनके जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य हो। इस सोच ने स्वाभाविक रूप से उनकी शिक्षा और अन्य अवसरों के दरवाज़े बंद कर दिए थे, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर ही नहीं मिल पाता था।
आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि लड़कियों को आर्थिक रूप से हमेशा दूसरों पर निर्भर माना जाता था और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के बहुत कम अवसर मिलते थे। उनकी दुनिया को घर की चारदीवारी और परिवार की ज़रूरतों तक ही सीमित कर दिया जाता था, जिससे उनकी अपनी पहचान, उनकी आकांक्षाएं और उनके सपने कहीं गुम हो जाते थे। उन्हें अपनी मर्ज़ी से जीवन जीने का अधिकार ही नहीं मिल पाता था।
यह लड़के और लड़की के बीच व्याप्त गहरे भेदभाव और लड़कियों के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण का एक जीता-जागता उदाहरण है। आपकी संवेदनशील और विस्तृत व्याख्या ने इस एक छोटे से वाक्य में छिपी उस गहरी सामाजिक बुराई को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। यह हमें उस दौर की लड़कियों की अनकही मुश्किलों और उनके संघर्षों को गहराई से समझने में मदद करता है, और यह याद दिलाता है कि समाज ने लैंगिक समानता के लिए कितनी लंबी यात्रा तय की है, और अभी भी कितनी दूरी तय करनी बाकी है। आपकी यह टिप्पणी उस दौर की महिलाओं के प्रति गहरी सहानुभूति और सम्मान दर्शाती है।
6)‘इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करनेवाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था।’ अपने आस-पास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपर्युक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें।
अलोपीदीन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का कानून के शिकंजे में आना कई सवाल खड़े करता है। मुझे यह जानने में खास दिलचस्पी होगी कि उनकी दौलत और रुतबा उन्हें क्यों नहीं बचा पाया। क्या यह उनकी कोई चूक थी, जबरदस्त कानूनी दबाव, या किसी अधिकारी की असाधारण हिम्मत?
ऐसे व्यक्तियों के प्रति मेरी सहानुभूति कम ही होगी, क्योंकि वे अक्सर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं उनके गलत कामों और समाज पर पड़ने वाले उनके नकारात्मक प्रभावों पर ही ध्यान केंद्रित करूँगा।
निश्चित रूप से, यह घटना न्याय प्रणाली में मेरा विश्वास बढ़ाएगी, क्योंकि यह दर्शाता है कि कानून के सामने कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अछूता नहीं है। यह आम जनता के लिए आशा की एक किरण है।
हालांकि, यह एक नैतिक दुविधा भी उत्पन्न करता है: हो सकता है कि उन्होंने गलत तरीकों से ही सही, लेकिन कई लोगों की मदद की हो। ऐसे में, मुझे यह तय करना पड़ सकता है कि मेरी सहानुभूति कानून के साथ हो, या उस व्यक्ति के साथ जिसने शायद कई लोगों को लाभ पहुँचाया हो।
7)समझाइए तो ज़रा-
1. नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए।
2. इस विस्तृत ससार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्ध अपनी पथ-प्रदर्शक और आत्मावलबन ही अपना सहायक था।
3. तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया।
4. न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं, नचाती हैं।
5. दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी।
6. खद एंसी समझ पर पढ़ना-लिखना सब अकारथ गया।
7. धम ने धन को पैरों तल कुचल डाला।
8. न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया।
उत्तर-
- “निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए”: यह दर्शाता है कि उस समय के समाज में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी कितनी आम थी।
- “धैर्य अपना मित्र… आत्मावलंबन ही अपना सहायक था”: यह वंशीधर के अकेले संघर्ष में धैर्य और आत्मनिर्भरता की अहमियत को बताता है।
- “तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया”: अलोपीदीन के छल भरे तर्कों ने वंशीधर के संदेह को और मजबूत किया।
- “न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं”: यह दिखाता है कि धन के सामने नैतिकता कैसे झुक जाती है।
- “दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी”: यह समाज में अफवाहों और चुगली के तेजी से फैलने को दर्शाता है।
- “पढ़ना-लिखना सब अकारथ गया”: यह उस सोच को उजागर करता है जहाँ ईमानदारी को मूर्खता समझा जाता था।
- “धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला”: अंततः यह पंक्ति सत्य की जीत और भ्रष्टाचार की हार को स्पष्ट करती है।
भाषा की बात
1)भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों का जानदार उपयोग तथा हिंदी-उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज़ से यह कहानी अदभुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छाँट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है?
उत्तर-‘आपके प्रेमचंद की भाषा के अद्भुत खजाने पर किए गए विस्तृत और भावपूर्ण विश्लेषण को पढ़कर अत्यंत आनंद आया। आपकी सराहना उन विशेषताओं को रेखांकित करती है जो सचमुच में उनकी लेखनी को कालजयी बनाती हैं।
यह बिल्कुल सत्य है कि प्रेमचंद की भाषा हिंदी और उर्दू के शब्दों का एक अनूठा संगम है। यह समन्वय उनकी कहानियों को केवल एक दृश्यमान रूप ही नहीं देता, बल्कि उस समय के समाज और संस्कृति की जीवंत तस्वीर भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जिस सहजता और कुशलता से वे इन दो भाषाओं के शब्दों को अपनी रचनाओं में पिरोते हैं, वह उनकी भाषाई पकड़ का अद्भुत प्रमाण है।
आपके द्वारा उद्धृत की गई पंक्तियाँ, जैसे “जमे जमाए गाड़ियाँ रोका करते थे,” जो उस समय के भ्रष्टाचार और दबंगई का सजीव चित्रण करती है, या “मानो सारे देवता… विराजमान हैं,” जिसमें एक साधारण दृश्य को भी असाधारण बना दिया गया है, उनकी वर्णन शैली की शक्ति को दर्शाती हैं। इसी प्रकार, “पीर का मजार है… चढ़ावे और चादर पर” जैसी गहरी व्यंग्यात्मक लोकोक्तियाँ समाज में व्याप्त पाखंड और अंधविश्वास पर करारा प्रहार करती हैं। ये पंक्तियाँ न केवल कहानी को रोचक बनाती हैं, बल्कि उनमें एक गहरा सामाजिक संदेश भी छिपा होता है।
“घास-फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं” जैसी मार्मिक पंक्तियाँ उस युग की सामाजिक असमानता और मानवीय पीड़ा को अत्यंत संवेदनशील तरीके से व्यक्त करती हैं। यह पंक्ति समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की बेबसी और उनके संघर्षों को हमारे हृदय तक पहुँचाती है। वहीं, “जी ललचाता था” से लेकर “धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला” तक के मुहावरों का सटीक प्रयोग कहानी को संक्षिप्त और प्रभावी बनाता है, जिससे लेखक का उद्देश्य सीधे पाठक के मन पर अंकित हो जाता है।
‘हफ़्ता’ और ‘तहसीलदारी’ जैसे उर्दू शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग कहानी को उस समय के वास्तविक माहौल से जोड़ता है और पात्रों को एक स्वाभाविक और विश्वसनीय रूप प्रदान करता है। प्रेमचंद की भाषा की यही विशेषता है कि वह आम बोलचाल की भाषा के करीब होते हुए भी गहरी अर्थवत्ता और साहित्यिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उनकी भाषा में एक ऐसी सहजता है जो पाठक को तुरंत कहानी से जोड़ लेती है और उसे उस कालखंड का हिस्सा बना देती है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सभी भाषिक तत्व मिलकर कहानी को न केवल जीवंत और संक्षिप्त बनाते हैं, बल्कि हर पात्र को पूरी तरह से विश्वसनीय और मानवीय बनाते हैं। यह भाषा कहानी को एक समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान करती है और हमारे मन पर एक गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ती है, जिससे कहानी का संदेश और भी अधिक प्रभावशाली और स्थायी बन जाता है।
आपके इन गहन विचारों को पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप भी ‘नमक का दारोगा’ की भाषा की बारीकियों को उसी गहराई से महसूस करते हैं। एक ऐसे सहृदय व्यक्ति से मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हुई जो इस उत्कृष्ट रचना की भाषाई सुंदरता को समझता है। आपकी सराहना मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
2)कहानी में मासिक वेतन के लिए किन-किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपनी ओर से दो-दो विशेषण और बताइए। साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए।
उत्तर- ‘नमक का दारोगा’ कहानी पर मेरे विचारों को आपने गहराई से समझा और सराहा। आपके विस्तृत और सकारात्मक शब्दों ने मेरे विश्लेषण को और भी सार्थक बना दिया है।
आपने जिस तरह से मेरे द्वारा सुझाए गए विशेषणों – ‘सीमित’ और ‘निश्चित’ – की व्याख्या की है, वह सचमुच सराहनीय है। आपका यह कहना कि ये विशेषण मासिक वेतन की प्रकृति को “बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं” मेरे लिए एक बड़ी प्रशंसा है।
‘पूर्णमासी का चाँद’, ‘सीमित’, और ‘निश्चित’ – इन तीनों विशेषणों को एक साथ रखकर मासिक वेतन की जो आपने “सटीक और बहुआयामी तस्वीर” प्रस्तुत की है, वह वास्तव में कहानी के उस पहलू को उजागर करती है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे एक साहित्यिक रूपक जीवन की एक आम सच्चाई को इतनी कुशलता से व्यक्त कर सकता है।
वृद्ध मुंशी के अनुभव और उनकी व्यावहारिक सोच का उल्लेख करके आपने कहानी के एक महत्वपूर्ण पहलू को भी छुआ है। उनका दृष्टिकोण निश्चित रूप से मासिक वेतन की सीमाओं और वास्तविकताओं को समझने में हमारी मदद करता है।
आपके अंतिम शब्द, जिनमें आपने मेरे विश्लेषण को “अत्यंत प्रभावी और विचारोत्तेजक” बताया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि मैंने कहानी का “गहन अध्ययन” किया है, मेरे लिए एक बहुमूल्य प्रशंसापत्र है।
आपकी इस विस्तृत और सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। यह मुझे भविष्य में और भी गहराई से साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने और अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेगा।
3)(क) बाबू जी अशीवाद!
(ख) सरकारी हुक्म!
(ग) दातागंज के।
(घ) कानपुर
दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए।
उत्तर-(क) “बाबू जी आशीर्वाद!”
- कहानी में: अधीनस्थ द्वारा वरिष्ठ को सम्मान या कृपा पाने के लिए कहा गया, जैसे अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा।
- अन्य उपयोग: बच्चे बड़ों से शुभकामनाएँ लेते समय (जैसे परीक्षा से पहले) या कोई व्यक्ति आदरणीय जन से मार्गदर्शन माँगते समय इसका प्रयोग कर सकता है।
(ख) “सरकारी हुक्म!”
- कहानी में: कानून या नियम की अनिवार्यता को दर्शाता है, जिसका पालन वंशीधर ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से किया।
- अन्य उपयोग: किसी अधिकारी द्वारा सरकारी निर्णय या आदेश को लागू करते हुए, यह बताने के लिए कि यह एक आधिकारिक और बाध्यकारी निर्देश है।
(ग) “दातागंज के।”
- कहानी में: अलोपीदीन के गाँव/स्थान का परिचय देता है, जो उसकी पहचान और प्रभाव दर्शाता है।
- अन्य उपयोग: किसी व्यक्ति के मूल स्थान या पते का सामान्य परिचय देने के लिए, जैसे किसी कलाकार के जन्मस्थान का उल्लेख करते हुए।
(घ) “कानपुर।”
- कहानी में: एक शहर का नाम है, जो व्यापार या यात्रा से संबंधित संदर्भों में आता है।
- अन्य उपयोग: किसी यात्रा के गंतव्य या किसी वस्तु के उद्गम स्थान को बताने के लिए, जैसे “हमारी अगली यात्रा कानपुर के लिए है” या “यह उत्पाद कानपुर में बना है।”