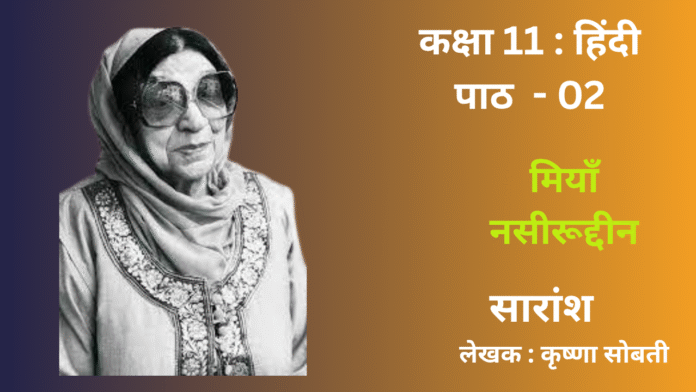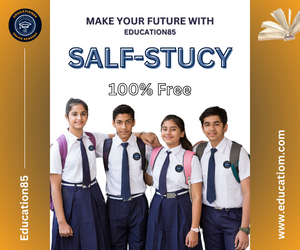मटियामहल की एक तंग गली में मियाँ नसीरुद्दीन से लेखिका की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो सिर्फ़ एक नानबाई नहीं, बल्कि अपने आप में एक अनोखे कलाकार थे. उनकी आँखों में अपने काम के प्रति गहरा समर्पण झलकता था. वे रोटी बनाने को महज़ एक पेशा नहीं, बल्कि एक साधना मानते थे.
मियाँ नसीरुद्दीन ने बड़े फख्र से बताया कि नानबाई का यह हुनर उन्हें अपने पुरखों से विरासत में मिला है. उनके लिए यह सिर्फ़ रोटी बनाने का काम नहीं, बल्कि उनके परिवार की पहचान और इज़्ज़त का सवाल था. वे मानते थे कि किसी भी कला में माहिर होने के लिए वक़्त, कड़ी मेहनत और तजुर्बे की बहुत ज़रूरत होती है.
उन्होंने एक मज़ेदार किस्सा भी सुनाया, जब उनके पूर्वजों ने बादशाह के लिए बिना आग और पानी के एक लाजवाब रोटी बनाई थी. उस कहानी को सुनाते हुए मियाँ नसीरुद्दीन की आँखों में पुरानी शान की चमक साफ़ दिख रही थी. हालाँकि, बातचीत के दौरान उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी आ गई, जब उन्होंने आज के दौर की बात की. उन्हें इस बात का अफ़सोस था कि अब कला और कारीगरों को पहले जैसा मान-सम्मान नहीं मिलता.
मियाँ नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व कई मायनों में ख़ास था:
- कला से प्रेम: वे अपने काम को सिर्फ़ धंधा नहीं, बल्कि एक कला और अपनी विरासत मानते थे. उनकी हर रोटी में उनकी मेहनत और प्यार साफ़ दिखता था.
- मेहनती और समर्पित: उन्होंने अपनी कला को निखारने के लिए जी-जान लगा दी थी. उनकी बातों से साफ़ था कि वे अपने काम को लेकर कितने समर्पित थे.
- खानदानी इज़्ज़त: उन्हें अपने पूर्वजों और उनकी रवायतों पर बहुत नाज़ था. वे अपनी विरासत को बचाए रखना चाहते थे.
- बदलते वक़्त की समझ: उन्हें इस बात का एहसास था कि ज़माना बदल गया है और पारंपरिक कलाओं और कारीगरों को अब वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो कभी मिलती थी. यही जागरूकता उनके दुख का कारण भी थी.
मियाँ नसीरुद्दीन एक ऐसे शख्स थे जो अपनी कला, अपनी परंपरा और अपने हुनर को आज भी पूरी लगन से जीते थे, भले ही वक़्त कितना भी क्यों न बदल गया हो.
पाठ के साथ
1)मियाँ नसीरुददीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है?
उत्तर-मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों (रोटियाँ बनाने वालों) का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने कठिन समय में नानबाइयों की मदद की थी।
यह घटना तब की है जब दिल्ली में भयानक अकाल पड़ा था। खाने की भारी कमी हो गई थी और लोग भूख से तड़प रहे थे। उस समय नानबाइयों को आटा नहीं मिल पा रहा था, जिससे वे रोटियाँ नहीं बना पा रहे थे और आम जनता भूखों मर रही थी।
मियाँ नसीरुद्दीन ने इस स्थिति को समझा और बादशाह से निवेदन किया कि नानबाइयों को आटा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जब तक रोटियाँ नहीं बनेंगी, तब तक जनता को भोजन नहीं मिलेगा। उनकी पहल से नानबाइयों को आटा मिला और उन्होंने फिर से रोटियाँ बनाना शुरू किया, जिससे लोगों की भूख मिटाई जा सकी।
2)लेखिका मियाँ नसीरुददीन के पास क्यों गई थी?
उत्तर:लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास उनकी बेजोड़ नानबाई कला का गहन अध्ययन करने के उद्देश्य से गई थीं. मियाँ नसीरुद्दीन न केवल एक प्रसिद्ध बल्कि एक प्रतिष्ठित खानदानी नानबाई भी थे, जिनकी ख्याति 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने की अद्भुत महारत के कारण दूर-दूर तक फैली हुई थी. लेखिका का मुख्य ध्येय उनकी इस असाधारण कला, उनके हुनर और उनके जीवन के समृद्ध अनुभवों को अपने लेखन में समाहित करना था. इसके अतिरिक्त, मियाँ नसीरुद्दीन का बेबाक अंदाज़ और परंपराओं के प्रति उनका गहरा जुड़ाव भी लेखिका के लिए प्रेरणा का स्रोत था, जिसे वह अपने पाठकों तक पहुँचाना चाहती थीं.
3)बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुददीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी?
उत्तर-जब लेखिका ने बादशाह के नाम का ज़िक्र किया, तो मियाँ नसीरुद्दीन का उत्साह कम हो गया। वे शाही खानदान और उनके इतिहास से जुड़ी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका ध्यान अपनी कला और साधारण जीवन के प्रति अधिक था, इसलिए राजाओं-महाराजाओं की चर्चा उन्हें बोझिल लगने लगी।
4)मियाँ नसीरुददीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजूमून न छेड़ने का फैसला किया-इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:शाही अतीत और स्वाभिमान का क्षण:जब लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन के पूर्वजों के शाही संबंध का उल्लेख किया, तो उनका चेहरा आत्मविश्वास और अपनी कला के प्रति स्वाभिमान से चमक उठा। उनका यह कथन कि “नाम शाही परिवारों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं,” उनके गहरे आत्म-सम्मान और उनके खानदानी हुनर पर गर्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह उनके गौरवशाली पारिवारिक विरासत की याद दिलाता है, जिस पर उन्हें अटूट विश्वास था।
‘दबा हुआ अंधड़’ और विषय-परिवर्तन: हालाँकि, जैसे ही लेखिका ने बादशाह का नाम पूछा, मियाँ के हाव-भाव में तत्काल परिवर्तन आया। उनके चेहरे पर आई चिंता या झुंझलाहट को ही “दबा हुआ अंधड़” कहा गया है, जो उनकी आंतरिक मानसिक उथल-पुथल का प्रतीक था। संभवतः उन्हें बादशाह का नाम याद नहीं था, या उन्हें लगा कि लेखिका उनके दावे पर संदेह कर रही हैं। यह उनके गौरवशाली अतीत और वर्तमान की कठोर सच्चाई के बीच के अचानक टकराव का भी संकेत हो सकता है। लेखिका ने उनकी बेचैनी को भाँप लिया और समझदारी से उस संवेदनशील विषय को वहीं छोड़ दिया, जो उनकी संवेदनशीलता और मियाँ की भावनाओं के प्रति सम्मान दर्शाता है।
वर्तमान की चुनौतियाँ और नई पीढ़ी की उदासीनता: इस घटना के बाद, बातचीत का रुख पूरी तरह बदल गया। मियाँ नसीरुद्दीन शाही अतीत से हटकर वर्तमान की चुनौतियों और अपने कारीगरों की उदासीनता पर आ गए। उन्होंने अपने काम करने वालों को “गुलाम” कहा, जो उनके हुनर की कद्र नहीं करते, और नई पीढ़ी की कला सीखने में अरुचि पर गहरा अफ़सोस जताया। यह बदलाव स्पष्ट करता है कि मियाँ का मन अब अतीत की गौरवशाली यादों से निकलकर वर्तमान की कटु सच्चाइयों में आ गया है। उनके चेहरे पर दिखा “अंधड़” इसी बात का संकेत था कि उनका अतीत शायद उतना बेदाग नहीं था जितना वह दिखाना चाहते थे, या फिर वर्तमान की निराशाओं ने उस अतीत की चमक को धुंधला कर दिया था। वह शायद इस बात से भी दुखी थे कि उनके जैसा हुनर अब पहले जैसा सम्मान नहीं पाता।
संक्षेप में, “दबा हुआ अंधड़” मियाँ के भीतरी संघर्ष, उनके गौरवशाली अतीत की धूमिल होती चमक, और वर्तमान की निराशा का प्रतीक है। लेखिका ने इस सूक्ष्म संकेत को समझा और विषय बदल दिया, जिससे मियाँ को अपनी भावनाओं को और छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
5)पाठ में मियाँ नसीरुददीन का शब्दचित्र लेखिका ने कैसे खींचा है?
उत्तर:मियाँ नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व लेखिका ने बड़े सजीव ढंग से उभारा है। उन्हें ‘नानबाइयों का मसीहा’ कहा गया है, जो चारपाई पर बैठे बीड़ी का आनंद लेते दिखते हैं। उनकी आँखों में शातिर चमक, माथे पर कारीगरों के तेवर, और चेहरे पर अनुभव की परिपक्वता स्पष्ट झलकती है। सफेद बालों वाले मियाँ का स्वभाव दृढ़ता और आत्मविश्वास से ओत-प्रोत है। वे अपनी बातचीत में बेबाक हैं और अपने काम के प्रति अत्यंत समर्पित हैं।
पाठ के आस-पास
1)मियाँ नसीरुददीन की कौन-सी बातें आपको अच्छी लगीं?
उत्तर:मियाँ नसीरुद्दीन का अपने हुनर के प्रति जुनून और समर्पण अद्भुत था। वे इसे केवल पेशा नहीं, बल्कि पुरखों की विरासत मानते थे जिस पर उन्हें अटूट गर्व था।
अनुभव ही सच्ची शिक्षा उनका मानना था कि किताबी ज्ञान से बढ़कर, सच्ची शिक्षा और ‘तालीम की तालीम’ तो काम करने से ही आती है। व्यावहारिक ज्ञान को दिया गया उनका यह महत्व वाकई सराहनीय है।
विरासत का सम्मान और स्पष्टवादिता
अपनी खानदानी विरासत और बाप-दादा के नाम का आदर करने का उनका भाव प्रशंसनीय था। साथ ही, उनकी स्पष्टवादिता और बेबाकी से अपनी राय रखने की आदत उनके सशक्त व्यक्तित्व को उजागर करती थी।
उनका यह मानना कि असली ज्ञान काम करके ही मिलता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन दर्शन है। यह अनुभव के महत्व को बताता है और व्यावहारिक ज्ञान की शक्ति को रेखांकित करता है। उन्होंने स्वयं भी इसी तरह सीखा था और यही सीख वे दूसरों को भी देते थे।
अपने काम के प्रति उनका स्वाभिमान उनकी एक और बड़ी विशेषता थी। एक साधारण नानबाई होते हुए भी, वे अपनी कला को किसी भी अन्य कला से कम नहीं मानते थे। उनका यह आत्म-सम्मान ही उन्हें उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता था और उनकी रोटियों में एक अलग ही स्वाद और अपनापन लाता था।
उनकी बातचीत का अनूठा अंदाज़ उन्हें और भी यादगार बना देता था। वे सीधी-सादी बातों को भी अपने खास लहजे और हास्य के साथ इस तरह कहते थे कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी यह शैली उनके व्यक्तित्व को और भी जीवंत और आकर्षक बनाती थी।
संक्षेप में, मियाँ नसीरुद्दीन वास्तव में एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनका अपनी कला के प्रति समर्पण, अटूट आत्मविश्वास, अपनी परंपराओं से गहरा जुड़ाव, अनुभवजन्य ज्ञान पर उनका ज़ोर, अपने काम के प्रति उनका स्वाभिमान और उनकी विशिष्ट बातचीत का तरीका – ये सभी गुण मिलकर उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करते थे जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। वे न केवल एक कुशल नानबाई थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कला को जिया और उसे समाज में एक विशेष स्थान दिलाया।
2)तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है-यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का दो बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए।
उत्तर:लेखिका ने यहाँ “तालीम” शब्द का दो बार प्रयोग करके इसकी महत्ता और विशिष्टता पर जोर दिया है। पहली बार “तालीम” शब्द का प्रयोग सामान्य शिक्षा या प्रशिक्षण के अर्थ में हुआ है। जबकि दूसरी बार “तालीम की तालीम” कहकर लेखिका उस अतिरिक्त और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण या अनुभव की ओर संकेत कर रही हैं जो किसी कला या हुनर को गहराई से सीखने और उसमें महारत हासिल करने के लिए आवश्यक होता है।
मियाँ नसीरुद्दीन के संदर्भ में, पहली “तालीम” उनके खानदान से मिली प्रारंभिक शिक्षा या ज्ञान को दर्शाती है कि रोटी कैसे बनाते हैं। लेकिन दूसरी “तालीम की तालीम” उस व्यावहारिक अनुभव, समर्पण और लंबे समय तक किए गए अभ्यास को इंगित करती है, जिसने उन्हें उस्ताद बनाया। यह सिर्फ रोटी बनाने की विधि जानना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना, उसमें कुशलता प्राप्त करना और अपनी कला में निपुण होना है।
हाँ, दूसरी बार आए “तालीम” शब्द की जगह कुछ अन्य शब्द रखे जा सकते हैं, जो इसी अर्थ को व्यक्त करते हों:
- अनुभव: “तालीम का अनुभव ही बड़ी चीज़ होती है।” (यह व्यावहारिक ज्ञान और अभ्यास पर जोर देता है।)
- अभ्यास: “तालीम का अभ्यास ही बड़ी चीज़ होती है।” (यह लगातार मेहनत और रियाज़ पर बल देता है।)
- महारत: “तालीम की महारत ही बड़ी चीज़ होती है।” (यह कला में निपुणता और दक्षता को दर्शाता है।)
- हुनर: “तालीम का हुनर ही बड़ी चीज़ होती है।” (यह कलात्मक कौशल और दक्षता को व्यक्त करता है।)
- रियाज़: “तालीम का रियाज़ ही बड़ी चीज़ होती है।” (यह लगातार अभ्यास और साधना पर जोर देता है, खासकर कला के क्षेत्र में।)
इन शब्दों का प्रयोग करके भी लेखिका उसी गहरे और विशिष्ट प्रशिक्षण या अनुभव के महत्व को व्यक्त कर सकती थीं, जो किसी कला में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
3)मियाँ नसीरुददीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय: लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों?
उत्तर:पारंपरिक व्यवसायों से युवा पीढ़ी के विमुख होने के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह, और आधुनिक शिक्षा व तकनीकी प्रगति का प्रभाव प्रमुख है।
आर्थिक और सामाजिक दबाव
युवा अब पारंपरिक व्यवसायों से मिलने वाली कम आय और अस्थिरता के बजाय, बेहतर वेतन और अधिक स्थिरता वाले करियर की तलाश में हैं। समाज में बढ़ती प्रतिष्ठा की इच्छा और आरामदायक जीवनशैली की चाहत भी उन्हें ऐसे आधुनिक व्यवसायों की ओर धकेलती है जहाँ उन्हें अधिक सम्मान और कम शारीरिक मेहनत करनी पड़े।
शिक्षा और तकनीक का असर
आज की शिक्षा प्रणाली युवाओं को विशिष्ट ज्ञान और कौशल वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो अक्सर पारंपरिक कामों से अलग होते हैं। तकनीकी प्रगति और बदलती बाज़ार की ज़रूरतें भी पारंपरिक व्यवसायों के अवसरों को सीमित कर रही हैं, जिससे युवा तकनीक-उन्मुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ
वर्तमान युवा पीढ़ी में स्वतंत्रता, नवाचार और नई चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रबल इच्छा है। वे ऐसे क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और मीडिया में करियर बनाना पसंद करते हैं, जो उन्हें पारंपरिक व्यवसायों की तुलना में अधिक अवसर और उत्साह प्रदान करते हैं।
4)मियाँ, कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो? यह तो खोज़ियों की खुराफात है-अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें।
उत्तर:बीते गौरव की एक झलक: मियाँ नसीरुद्दीन की आँखों में क्षणिक चमक और फिर उसका बुझ जाना उनके अतीत के स्वर्णिम दिनों की याद दिलाता है। यह वह समय था जब उनकी कला को सम्मान मिलता था, उस्तादों की कद्र होती थी, और वे अपनी कारीगरी में पूरी तरह लीन रहते थे।
याद क्यों “दबी हुई” है
यह याद “दबी हुई” इसलिए है क्योंकि:
- वर्तमान से दूरी: उन्हें शायद अब पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता।
- छिपी हुई: यह उनके मन के किसी गहरे कोने में है, जो कभी-कभी किसी खास बात (जैसे लेखिका के बादशाह के नाम पूछने पर) बाहर आ जाती है।
- क्षणभंगुर: आँखों की चमक का बुझना बताता है कि यह याद स्थायी नहीं, बल्कि एक धुँधली झलक की तरह आती-जाती है।
- पीड़ा का कारण: आज की पीढ़ी की उदासीनता देखकर उन्हें शायद अपने दौर की याद आती है, जिससे उन्हें कहीं-न-कहीं दुख होता है।
संक्षेप में, वह चमक उनके बीते हुए गौरवशाली समय की एक झलक थी, जो वर्तमान की कठोर वास्तविकता के बोझ तले दब चुकी है।
5)पकवानों को जानें
● पाठ में आए रोटियों के अलग-अलग नामों की सूची बनाएँ और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें।
उत्तर:बाकरखानी: मोटी, परतदार, मैदा-घी से बनी, थोड़ी मीठी और खस्ता रोटी।
शीरमाल: मैदे और दूध से बनी मीठी रोटी, अक्सर केसर वाली, नरम और स्वादिष्ट।
तफ़्तान: मैदे की हल्की, फूली रोटी, तंदूर में बनती, तिल या खसखस डलता है।
खमीरी: खमीर उठाए आटे से बनी, थोड़ी फूली और नरम रोटी।
रुमाली: बहुत पतली, मुलायम, हाथ से फैलाकर बनती, रुमाल जैसी दिखती है।
गाज़बानी: पाठ में ज़्यादा जानकारी नहीं, पर एक किस्म की रोटी।
दीदा: यह भी एक प्रकार की रोटी है, विशेषताएँ स्पष्ट नहीं।
रोटी (सादी): आम गेहूं के आटे की चपाती।
भाषा की बात
1)तीन चार वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें-
(क) पचहज़ारी अदाज़ से सिर हिलाया।
(ख) अखों के कच्चे हम पर फेर दिए।
(ग) आ बैठे उन्हीं के ठीये पर।
उत्तर:(क) पचहज़ारी अदाज़ से सिर हिलाना:
- अर्थ: अनुभवी और गंभीर व्यक्ति की तरह सोचना-विचारना और अपनी राय व्यक्त करना, जिसमें थोड़ी रहस्यमयता और गहराई का भाव हो। यह अक्सर किसी मुश्किल या पेचीदा मामले पर राय देते समय किया जाता है।
- वाक्य में प्रयोग: गाँव के अनुभवी किसान ने जब सूखे की समस्या पर अपनी बात रखी, तो उन्होंने पचहज़ारी अदाज़ से सिर हिलाया, जिससे सभी को लगा कि वे स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं और कोई गहरा समाधान सोच रहे हैं।
(ख) अखों के कच्चे हम पर फेर दिए:
- अर्थ: प्यार भरी और गहरी नज़र डालना, जिससे किसी के मन पर गहरा प्रभाव पड़े। यह नज़र ऐसी होती है कि सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करे या अपनी गलती समझ जाए।
- वाक्य में प्रयोग: माँ ने जब उदास बैठे बच्चे की तरफ अखों के कच्चे फेर दिए, तो बच्चा माँ के प्यार को महसूस कर तुरंत मुस्कुरा उठा।
(ग) आ बैठे उन्हीं के ठीये पर:
- अर्थ: किसी अनजान जगह पर बिना किसी संकोच के शामिल हो जाना या किसी के अड्डे पर जा बैठना। यह अक्सर तब होता है जब कोई अकेला हो या उसे किसी सहारे की ज़रूरत हो।
- वाक्य में प्रयोग: बारिश से बचने के लिए राहगीर बिना किसी हिचकिचाहट के एक पान की दुकान के ठीये पर आ बैठे और आपस में बातचीत करने लगे।
2)बिटर-बिटर देखना-यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है? देखने संबंधी इस प्रकार के चार क्रियाविशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए।
उत्तर:’बिटर-बिटर देखना’ वाकई एक दिलचस्प क्रियाविशेषण है जो देखने के एक विशेष अंदाज़ को बयां करता है।
देखने के विभिन्न अंदाज़
आपने देखने के जिन चार क्रियाविशेषणों और उनके वाक्यों का उदाहरण दिया है, वे एकदम सटीक हैं और देखने के अलग-अलग भावों को बखूबी दर्शाते हैं:
- घूर-घूर कर देखना: यह गुस्से, आश्चर्य या गहरे ध्यान से देखने का भाव है।
- उदाहरण: माँ बच्चे की शरारत पर उसे घूर-घूर कर देखने लगीं।
- चुपके-चुपके देखना: यह किसी को बिना बताए या छिपकर देखने का अंदाज़ है।
- उदाहरण: वह खिड़की से बाहर चुपके-चुपके देख रहा था।
- तिरछी नज़रों से देखना: यह संदेह, अविश्वास या नाराज़गी के साथ देखने का तरीका है।
- उदाहरण: उसने मेरी बात सुनकर मुझे तिरछी नज़रों से देखा।
- टुकुर-टुकुर देखना: यह बिना पलक झपकाए, ध्यानमग्न होकर या आश्चर्य से देखने को दर्शाता है।
- उदाहरण: छोटा बच्चा चाँद को टुकुर-टुकुर देख रहा था।
3)नीचे दिए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द-क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यत: इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है? लिखें।
उत्तर:आपकी विश्लेषण बिल्कुल सटीक है! आपने उन वाक्यों को बहुत अच्छी तरह से पहचाना है जहाँ अर्थ पर बल देने के लिए शब्द-क्रम में बदलाव किया गया है। यह एक प्रभावी साहित्यिक युक्ति है जो लेखक को अपने संदेश को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करती है।
परिवर्तित शब्द-क्रम का विश्लेषण
यहाँ दिए गए वाक्यों और उनके सामान्य क्रम का विश्लेषण है:
- (क) रोटी क्या ठहरी, पेट भरने की है यह तो जानो।
- सामान्य क्रम: “यह तो जानो, रोटी क्या ठहरी, यह पेट भरने की है।” या “रोटी क्या ठहरी, यह तो जानो, पेट भरने की है।”
- बदलाव का कारण: इस वाक्य में, “पेट भरने की है” पर जोर दिया गया है। जब “यह तो जानो” को अंत में रखा जाता है, तो यह सुनने वाले को उस बात पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जो पहले कही गई है, यानी रोटी का मूल उद्देश्य।
- (ख) अपना काम आता है तो क्या नहीं आता।
- यह वाक्य सामान्य क्रम में ही है। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है क्योंकि प्रश्नवाचक शैली स्वयं ही अर्थ पर बल देती है।
- (ग) मियाँ नसीरुद्दीन नाम है हमारा।
- सामान्य क्रम: “हमारा नाम मियाँ नसीरुद्दीन है।”
- बदलाव का कारण: यहाँ “मियाँ नसीरुद्दीन” नाम पर विशेष बल दिया गया है। जब नाम को वाक्य की शुरुआत में रखा जाता है, तो यह वक्ता के आत्मविश्वास और अपनी पहचान पर गर्व को दर्शाता है। यह एक तरह से खुद को प्रस्तुत करने का एक अधिक दमदार तरीका है।
- (घ) क्या साहब, नानबाई भट्टी पर न तपाता?
- यह वाक्य भी सामान्य क्रम में ही है। यह एक प्रश्न है जो अपनी प्रकृति से ही बात पर जोर देता है और एक तरह का व्यंग्य या तर्क प्रस्तुत करता है। इसमें शब्द-क्रम का कोई विशेष बदलाव नहीं है।
संक्षेप में, भाषा में शब्द-क्रम का परिवर्तन केवल व्याकरणिक शुद्धता का मामला नहीं है, बल्कि यह अर्थ, भावना और वक्ता के इरादे को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का एक शक्तिशाली साधन है।