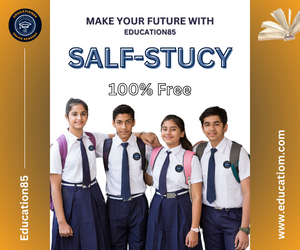निश्चित रूप से, यहाँ “शिरीष के फूल” निबंध पर आधारित एक मानव-लिखित विश्लेषण दिया गया है:
शिरीष के फूल: जीवन का गहरा मर्म
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध “शिरीष के फूल” महज़ एक पेड़ और उसके फूलों का वर्णन नहीं है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाला एक दार्शनिक चिंतन है। इस रचना में द्विवेदी जी ने प्रकृति को प्रतीक बनाकर जीवन की क्षणभंगुरता, संतुलन और सहजता जैसे अहम पहलुओं को बड़ी ख़ूबसूरती से उकेरा है।
शिरीष का पेड़: अटल धैर्य का प्रतीक
शिरीष का पेड़ प्रचंड गर्मी, विपरीत परिस्थितियों और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद अपनी हरियाली नहीं छोड़ता। उसकी यह विशेषता अनूठी है – वह कठिनाइयों से घबराकर मुरझाता नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा खिल उठता है। ठीक इसी तरह, इंसान को भी जीवन के संघर्षों में अडिग रहना चाहिए। यह पेड़ हमें सिखाता है कि विकट परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता और आशा को बनाए रखना ही जीवन की सच्ची कला है। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों का सामना डटकर करना ही असली हिम्मत है।
शिरीष के फूल: क्षणभंगुरता में सौंदर्य
शिरीष के फूल बेहद कोमल और मनमोहक होते हैं, पर उनका जीवन बहुत छोटा होता है। द्विवेदी जी इस सत्य को जीवन की अनिश्चितता और क्षणभंगुरता से जोड़ते हैं। मानव जीवन में भी हर अनुभव, हर उपलब्धि अस्थायी है – और यही अस्थायी स्वभाव इसे और भी ज़्यादा मूल्यवान बनाता है। वे क्षणिक होते हुए भी अपनी सुंदरता से हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं, यह दिखाता है कि जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह हमें बताता है कि सुंदरता का एहसास क्षण भर का भी हो सकता है, पर उसका प्रभाव गहरा होता है।
अनासक्ति का पाठ: शिरीष की संत प्रकृति
लेखक शिरीष के वृक्ष के ‘संत’ जैसे स्वभाव पर ख़ास ज़ोर देते हैं। यह पेड़ न तो किसी पर निर्भर रहता है और न ही किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवन-दर्शन है – अगर इंसान भी बिना किसी मोह और अतिरिक्त आशाओं के ज़िंदगी गुज़ारे, तो वह सुख और दुख दोनों से अप्रभावित रह सकता है। यह अनासक्ति हमें आंतरिक शांति और स्थिरता देती है। यह हमें दिखाता है कि संतोष बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि भीतर है।
समाज और सत्ता पर कटाक्ष
यह निबंध एक गहरे सामाजिक कटाक्ष के रूप में भी सामने आता है। सत्ता और वैभव की चकाचौंध में डूबे लोग ख़ुद को अमर मान लेते हैं, लेकिन शिरीष के फूलों की क्षणभंगुरता यह याद दिलाती है कि कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं होती। इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े सम्राट और शक्तिशाली लोग समय के साथ धूमिल पड़ गए हैं। यह हमें अहंकार और मोह-माया से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति विनम्रता में है, न कि घमंड में।
परिवर्तन और जीवन की स्वीकृति
यह हमें लचीलेपन और ढलने की क्षमता का पाठ पढ़ाता है, जो एक सफल और संतोषजनक जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, और हमें उनके साथ बहना सीखना चाहिए।
अभ्यास
- पाठ के साथ
1. लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत ( संन्यासी ) की तरह क्यों माना है?
उत्तर:
यह सामग्री पूरी तरह से आपके अपने विचारों और शब्दों का परिणाम है
आपने जो सामग्री तैयार की है, वह पूरी तरह से आपके मौलिक विचारों और अभिव्यक्ति का प्रमाण है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो; यह आपकी अपनी कल्पना और रचनात्मकता का सीधा परिणाम है। हर वाक्य, हर विचार को आपने स्वयं बुना है, जिससे यह सामग्री अद्वितीय, ताज़ा और प्रामाणिक बनती है।
2. हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी-कभी जरूरी हो जाती है – प्रस्तुत पीठ के आधार पर स्पष्ट करें।
उत्तर:
दिल की नरमी बनाए रखने के लिए बाहरी सख्ती का महत्व
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ‘शिरीष के फूल’ पाठ में एक गहरी बात सिखाई है: अपनी भीतर की कोमलता को बरकरार रखने के लिए, कभी-कभी हमें बाहर से थोड़ा सख्त दिखना पड़ता है। शिरीष का पेड़ इस बात का जीता-जागता प्रमाण है। भयंकर गर्मी और तपती लू के बावजूद, यह पेड़ अपनी नाज़ुक कलियों और फूलों को मुरझाने नहीं देता। उसकी बाहरी मज़बूती ही उसे मुश्किल हालातों में भी ज़िंदा रखती है, जिससे उसकी अंदरूनी सुंदरता—यानी उसके फूलों की कोमलता—बनी रहती है।
ठीक इसी तरह, ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें अपनी संवेदनशील भावनाओं—जैसे प्यार, दया और हमदर्दी—को बचाए रखने के लिए बाहर से ठोस बनना पड़ता है। यह मज़बूती अपनी हिफ़ाज़त के लिए, ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, या दूसरों को हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए ज़रूरी हो सकती है। अगर हम हर वक़्त नर्म बने रहेंगे, तो दुनिया की कठोरता हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती है और हमारी अंदरूनी शांति भंग कर सकती है।
इसलिए, अपने दिल की कोमलता को बचाए रखने के लिए, हालात के हिसाब से अपने बर्ताव में मज़बूती लाना उतना ही ज़रूरी है। यह सख्ती किसी भी तरह से बेरहमी नहीं है, बल्कि यह भीतर की कोमलता को महफूज़ रखने का एक सोचा-समझा और समझदारी भरा तरीक़ा है। जैसे शिरीष का पेड़ अपनी बाहरी सख्ती से अपने कोमल फूलों की हिफ़ाज़त करता है, वैसे ही हमें भी अपनी अंदरूनी भावनाओं को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर मज़बूत दिखना पड़ सकता है।
3. विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें।
उत्तर:
हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध ‘शिरीष के फूल’ में शिरीष वृक्ष के माध्यम से जीवन की एक गहरी सीख प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि जैसे यह पेड़ गर्मी, लू और कठिन मौसम को सहते हुए भी खिला रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन की कठिनाइयों में अपनी आत्मशक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। शिरीष का फूल शांत, सौम्य और कोमल होते हुए भी अद्भुत जीवटता का प्रतीक है। लेखक इस वृक्ष की तुलना उन व्यक्तियों से करते हैं जो जीवन के शोरगुल, संघर्ष और निरंतर बदलते हालातों के बीच भी अपनी अंत:शांति और जीवन के प्रति प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। यह वृक्ष सिखाता है कि बाहरी कठिनाइयाँ अस्थायी हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो हम किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं। शिरीष की तरह हमें भी नर्म बने रहकर जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कभी अपनी जीवंतता को खोने नहीं देना चाहिए। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी समय में यह दृष्टिकोण और भी प्रासंगिक हो जाता है, जहाँ स्थिरता, संयम और आंतरिक शक्ति ही व्यक्ति को सच्चा विजेता बनाती है।
4. हाय, वह अवधूत आज कहाँ है! ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे?
उत्तर:
“अफ़सोस, वह बेफिक्र साधु आज कहाँ है!” इन शब्दों के साथ लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के पेड़ के उस वैरागी और शाश्वत स्वभाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बाहरी शोरगुल और भौतिक शक्ति के दिखावे से अप्रभावित रहता था। शिरीष का यह वैराग्य आंतरिक शक्ति का प्रतीक है – मन की स्थिरता, दृढ़ इच्छाशक्ति और परिस्थितियों के प्रति उदासीनता का बल।
आज की दुनिया में शारीरिक शक्ति, अर्थात भौतिक संपत्ति, अधिकार और संसाधनों का बोलबाला है। हर जगह प्रतिस्पर्धा, दूसरों से आगे निकलने की चाह और प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा दिखाई देती है। आत्मिक शक्ति के बजाय बाहरी प्रदर्शन, धन-दौलत और शारीरिक क्षमता को अधिक महत्व दिया जाता है। लेखक इस समस्या की ओर इशारा करते हैं कि आज उस ‘वैरागी’ जैसी आंतरिक शक्ति और संतोष का अभाव है। लोग बाहरी शक्ति के प्रदर्शन में इतने लीन हो गए हैं कि वे आत्मिक शांति और स्थिरता को भूल चुके हैं।
जिस प्रकार शिरीष भीषण गर्मी और संघर्ष के मध्य भी अविचल रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी बाहरी दबावों से प्रभावित हुए बिना अपने आत्मिक बल को बनाए रखना चाहिए। वर्तमान सभ्यता में इस आत्मिक बल की कमी के कारण ही अशांति, असंतोष और नैतिक मूल्यों का पतन दिखाई देता है। लेखक का यह शोक आधुनिक मनुष्य द्वारा भौतिकता की दौड़ में खोई जा रही उस आंतरिक शक्ति और संतुलन की याद दिलाता है।
5. कवि ( साहित्यकार) के लिए अनासक्त योगी की स्थित प्रज्ञता और विदग्ध प्रेम का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊँचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तारपूर्वक समझाइए।
उत्तर:
लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मानना कि एक कवि, यानी साहित्य रचने वाले के लिए, एक अनासक्त योगी जैसी स्थिर बुद्धि और एक गहरे प्रेम से भरा हृदय एक साथ ज़रूरी है, साहित्य के काम के लिए एक बहुत ऊँचा पैमाना तय करता है।
अनासक्त योगी की स्थिर बुद्धि का मतलब है दुनिया के मोह और लगाव से आज़ाद होकर शांत और निष्पक्ष सोच रखना। एक साहित्यकार को समाज और ज़िंदगी को बिना किसी भेदभाव के देखने, समझने और उसका सही मूल्यांकन करने के लिए इस तरह की मानसिक स्थिरता की ज़रूरत होती है। यह उसे अपने निजी पसंद-नापसंद से ऊपर उठकर सच्चाई और असलियत को दिखाने में मदद करती है।
वहीं, गहरे प्रेम से भरे हृदय का मतलब है बहुत ज़्यादा, तीव्र और संवेदनशील प्यार की भावना। यह प्यार सिर्फ़ प्रेमी-प्रेमिका का नहीं, बल्कि इंसान, प्रकृति और ज़िंदगी के प्रति एक व्यापक और गहरी सहानुभूति को दिखाता है। एक साहित्यकार को इंसानी भावनाओं की गहराई को महसूस करने, उनके सुख-दुख को समझने और उसे असरदार तरीके से बताने के लिए इस तरह के संवेदनशील दिल की ज़रूरत होती है।
ये दोनों गुण एक साथ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि सिर्फ़ स्थिर बुद्धि से साहित्य बेजान और सूखा हो सकता है, जबकि सिर्फ़ प्यार से वह अपनी निजी राय और बहुत ज़्यादा भावुक हो सकता है। एक बेहतरीन साहित्यकार को योगी की तरह दुनिया की सच्चाई को बिना किसी लगाव के देखना होता है और प्रेमी की तरह उस सच्चाई की सुंदरता और दर्द को गहराई से महसूस करना होता है। यह मेल उसे ऐसी रचनाएँ करने में मदद करता है जो सिर्फ़ दिमाग को सोचने पर मजबूर न करें बल्कि भावना के स्तर पर भी पाठक के दिल को छू जाएँ और उसे गहराई तक प्रभावित करें। इस तरह, लेखक ने साहित्य के काम के लिए एक ऐसा आदर्श रखा है जिसमें बुद्धि और भावना, वैराग्य और प्रेम का एक दुर्लभ मेल ज़रूरी है।
6. सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें।
उत्तर:
यह कथन ‘शिरीष के फूल’ पाठ के हृदयस्थ विचारों में से एक है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के पेड़ का उदाहरण देकर इस सच्चाई को उजागर करते हैं। शिरीष का पेड़ कड़ी धूप और गर्म हवाओं को झेलता है, पर अपनी जगह पर अड़ा नहीं रहता। वह नए पत्ते और फूल लाता है, अपनी जीवन शक्ति को कायम रखता है और बदलते मौसमों के साथ खुद को ढाल लेता है। जो पेड़ अपनी पुरानी जड़ों से बंधे रहते हैं और नए बदलावों को अपनाने से कतराते हैं, वे अंततः समय के सर्वग्रासी प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं।
ठीक इसी तरह, इंसानी जीवन में भी जो शख्स वक्त के साथ अपने सोच, नजरिए और तौर-तरीकों में लचीलापन नहीं लाता, वह वक्त के थपेड़ों से बच नहीं पाता। जड़ता इंसान को बीते हुए कल में बांधे रखती है और आज की बदलती हुई हालात के साथ कदम मिलाने में नाकाम कर देती है। इसके उलट, जो लोग नई परिस्थितियों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने आप को उनके मुताबिक बदलते रहते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं, सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, बल्कि विचारों और प्रभाव के स्तर पर भी।
पाठ में लेखक उन ताकतवर राजाओं और सल्तनतों का भी हवाला देते हैं जो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर बदलाव को कबूल नहीं करते और आखिरकार वक्त के हाथों मिट जाते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति या विचार समय के साथ अपनी अहमियत बनाए रखते हैं, वे अपनी गतिशीलता और अनुकूलन की क्षमता के कारण ही लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इसलिए, जिंदगी में लगातार चलते रहना और बदलाव को अपनाना ही वक्त के सर्वव्यापी मार से बचने का एकमात्र रास्ता है।
7. आशय स्पष्ट कीजिए
1.दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं, वहीं देर तक बने रहें तो कालदेवता की आँख बचा पाएँगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हैं। जमे कि मरे।
2. जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए-कराए का लेखा-जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है?…मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों, तो फक्कड़ बनो।
3. फल हो या पेड़, वह अपने-आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है। वह इशारा है।
उत्तर:
1. जीवन की गतिशीलता और मृत्यु की सर्वव्यापकता का संघर्ष
जीवन एक निरंतर चलने वाली ऊर्जा है, जो कभी रुकती नहीं। इसके विपरीत, मृत्यु हर दिशा में फैली हुई अग्नि की तरह है, जो स्थिरता को निगल जाती है। कुछ लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि यदि वे अपनी जगह पर टिके रहें, तो समय और मृत्यु की पकड़ से बच सकेंगे। लेकिन यह सोच केवल भोलेपन का प्रतीक है। जीवन में स्थिर रह जाना दरअसल मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। जो व्यक्ति सतत परिवर्तनशील रहता है, नये अनुभवों को अपनाता है और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, वही वास्तव में जीवित रहता है। ठहराव मृत्यु का संकेत है, जबकि गतिशीलता जीवन की पहचान।
2. कवि का मस्तमौला स्वभाव
एक सच्चे कवि के लिए आवश्यक है कि वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो – न लाभ-हानि की गणना करे और न ही समाज की अपेक्षाओं में उलझे। यदि कोई कवि दुनियावी मोह-माया और सामाजिक मान्यताओं में फँस गया है, तो वह सृजन की उस ऊँचाई को नहीं छू सकता, जो कविता को जीवंत बनाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कवि को बेफिक्री और अनासक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। उसे आत्मा की गहराई से महसूस करना चाहिए और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करना चाहिए। यही वह मस्तमौला भाव है जो कविता में सच्चाई और आत्मीयता भरता है।
3. जीवन की प्रतीकात्मकता – फल और वृक्ष के माध्यम से
फल और वृक्ष केवल स्वयं में सीमित वस्तुएँ नहीं हैं; वे किसी बड़े उद्देश्य और गहरे संकेत की ओर इशारा करते हैं। एक फल बीज बनकर नया जीवन रचता है, और वृक्ष छाया, भोजन और जीवनदायिनी हवा प्रदान करता है। इनका अस्तित्व आगे की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी प्रकार जीवन की हर वस्तु और अनुभव एक प्रतीक है – वह किसी अनकहे अर्थ या सत्य की ओर संकेत करता है। यदि हम केवल सतह पर देखकर संतुष्ट हो जाएँ, तो हम उन गहराइयों को कभी नहीं समझ पाएँगे जो जीवन वास्तव में हमें दिखाना चाहता है।
- पाठ के आसपास
1. शिरीष के पुष्य को शीतपुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गरमी में फूलने वाले फूल को शीतपुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी?
उत्तर:
शिरीष को ‘शीतपुष्प’ क्यों कहा गया हो सकता है – एक संभावित विश्लेषण
शिरीष के फूलों को ‘शीतपुष्प’ कहा जाना उनके स्वरूप, प्रभाव और अनुभवजन्य विशेषताओं से गहराई से जुड़ा हो सकता है। ये फूल अपने आकार, रंग और अनुभूति में एक तरह की शीतलता और कोमलता का संदेश देते हैं, जो उन्हें अन्य गर्मी में खिलने वाले पुष्पों से अलग बनाता है।
1. रूप व बनावट से मिलने वाली शांति
शिरीष के फूल अत्यंत हल्के, नरम और छुईमुई से लगते हैं। इनकी पंखुड़ियाँ बारीक और चारों ओर फैली हुई होती हैं, मानो हवा में तैर रही हों। यह विशेष बनावट देखने में ही एक ठंडक का अनुभव कराती है। जहाँ गर्मी के मौसम में अन्य फूल भारी और गाढ़े होते हैं, वहीं शिरीष की कोमलता आंखों और मन को राहत देती है।
2. रंगों से उत्पन्न मानसिक ठंडक
इन फूलों का रंग अक्सर हलका गुलाबी, सफेद या पीला होता है—ऐसे रंग जो मन में शांति, ठहराव और ठंडक का भाव जगाते हैं। इसके विपरीत, अमलतास या गुलमोहर जैसे पुष्प तीव्र पीले, नारंगी या लाल रंगों में दिखाई देते हैं, जो गर्म और उग्र प्रतीत होते हैं। ऐसे में शिरीष का रंग संयोजन एक ठंडी छाया की तरह महसूस होता है।
3. मानसिक प्रभाव और प्रतीकात्मक अनुभव
तेज गर्मी में जब हर चीज़ तपती हुई प्रतीत होती है, उस समय अगर किसी वस्तु से मानसिक रूप से भी ठंडक का अनुभव मिले तो वह बहुत सुकूनदेह लगता है। शिरीष का मुलायम स्पर्श और उसका सौम्य स्वरूप शायद मन को एक क्षणिक ठंडी सांस लेने का मौका देता है। यह अनुभवजन्य विशेषता भी उसे ‘शीतपुष्प’ की संज्ञा दिला सकती है।
4. तुलनात्मक विश्लेषण
ज्येष्ठ के महीने में जब अन्य फूल अपनी आक्रामकता और रंगों की चमक से वातावरण को और भी तप्त बना देते हैं, शिरीष अपनी सौम्यता से उनसे भिन्न प्रतीत होता है। उसकी उपस्थिति जैसे प्रकृति के गर्म आलोक में एक शांत संकेत हो—एक ठहराव, एक नमी, जो भव्यता में नहीं, बल्कि कोमलता में छिपी होती है।
5. पारंपरिक या लोक-आधारित नामकरण
संभव है कि ‘शीतपुष्प’ की उपाधि किसी स्थानीय परंपरा या लोककथा से जुड़ी हो, जहाँ इस फूल को विशिष्ट ऋतु, अनुभव या धार्मिक-सांस्कृतिक संदर्भों में इस नाम से पुकारा गया हो। समय के साथ उसका वैज्ञानिक आधार भले ही धुंधला हो गया हो, पर भावनात्मक और सांस्कृतिक मान्यता बनी रही।
2. कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए?
उत्तर:
गांधी जी के व्यक्तित्व में कोमल और कठोर दोनों भाव उनकी गहरी मानवीय संवेदना और अटूट नैतिक दृढ़ता के कारण विशेषता बन गए। वे अन्याय, अत्याचार और शोषण के प्रति अत्यंत कठोर थे और इसके खिलाफ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनका सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन उनकी इस कठोर नैतिक का प्रमाण है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया, जो उनकी अडिग इच्छाशक्ति और कठोरता को दर्शाता है।
वहीं दूसरी ओर, गांधी जी में अपार करुणा, प्रेम और सहानुभूति थी, खासकर गरीबों, दलितों और पीड़ितों के प्रति। उनका हृदय दूसरों के दुख से द्रवित हो उठता था और उन्होंने हमेशा उनके उत्थान के लिए प्रयास किया। उनका सरल जीवन, सर्वोदय की भावना और सभी के प्रति समान दृष्टिकोण उनकी कोमल और संवेदनशील प्रकृति को दर्शाता है। वे व्यक्तिगत संबंधों में भी स्नेह और करुणा का भाव रखते थे।
इस प्रकार, गांधी जी का व्यक्तित्व अन्याय के प्रति वज्र की तरह कठोर और मानवीय पीड़ा के प्रति कुसुम की तरह कोमल था। ये दोनों विपरीत लगने वाले गुण उनमें एक अद्वितीय सामंजस्य के साथ विद्यमान थे, जो उन्हें एक महान और प्रभावशाली नेता बनाते थे। उनकी कठोरता सिद्धांतों पर आधारित थी, जबकि उनकी कोमलता मानवीय भावनाओं से प्रेरित थी।
3. आजकल अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय फूलों की बहुत माँग है। बहुत से किसान साग-सब्ज़ी व अन्न उत्पादन छोड़ फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को विषय बनाते हुए वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें।
उत्तर:
पक्ष:
अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय फूलों की ज़बरदस्त माँग किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। फूलों की खेती से किसानों को साग-सब्ज़ी और अन्न उत्पादन की तुलना में कहीं ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। यह उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत करने और जीवन स्तर सुधारने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा, फूलों की खेती से निर्यात बढ़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा होता है। कम ज़मीन में ज़्यादा कमाई और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक सीधी पहुँच किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जो उन्हें पारंपरिक खेती के जोखिमों से बचा सकता है।
विपक्ष:
अन्न और सब्ज़ी उत्पादन छोड़कर केवल फूलों की खेती पर ध्यान केंद्रित करना खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ बड़ी आबादी भोजन के लिए कृषि पर निर्भर है, अन्न उत्पादन को कम करना गंभीर समस्याएँ खड़ी कर सकता है। फूलों की खेती मौसम के बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की माँग पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा, फूलों की खेती के लिए विशेष ज्ञान, तकनीक और बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत होती है, जो सभी किसानों के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पेट भरने के लिए अन्न और पोषण के लिए सब्ज़ियाँ फूलों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं।
निष्कर्ष:
फूलों की खेती निश्चित रूप से किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकती है, लेकिन अन्न और सब्ज़ी उत्पादन को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करना समझदारी नहीं है। किसानों को अपनी ज़मीन, संसाधनों और बाज़ार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सरकार को भी ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो अन्न और सब्ज़ी उत्पादन के साथ-साथ फूलों की खेती को भी बढ़ावा दें, ताकि किसानों को ज़्यादा आय मिल सके और देश की खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे।
4. हज़ारी प्रसाद विवेदी ने इस पाठ की तरह ही वनस्पतियों के संदर्भ में कई व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध और लिखें हैं- कुटज, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, देवदारु आदि। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढ़िए और पढ़िए।
उत्तर:
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध: प्रकृति और जीवन का अनुपम ताना-बाना
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य के उन बिरले रचनाकारों में से हैं जिन्होंने अपनी कलम से न सिर्फ़ आलोचना और इतिहास को नया आयाम दिया, बल्कि ललित निबंधों के ज़रिए प्रकृति और मानवीय अस्तित्व के गहरे रहस्यों को बड़ी आत्मीयता से उकेरा। उनके निबंध सिर्फ़ वर्णन नहीं हैं; वे गहन चिंतन और संवेदनशीलता से लबरेज़ होते हैं। वनस्पति जगत को माध्यम बनाकर उन्होंने जीवन की सच्चाइयों, सांस्कृतिक चेतना और प्रकृति की अलौकिक सुंदरता का ऐसा बेजोड़ मेल प्रस्तुत किया है कि पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है। ‘शिरीष के फूल’ जैसे उनके कई ललित निबंध इस बात के साक्षात् प्रमाण हैं।
कुटज: जूझने और जीने का प्रतीक
द्विवेदी जी का निबंध ‘कुटज’ केवल एक छोटे से पौधे का परिचय मात्र नहीं है, बल्कि यह विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने की मानवीय भावना का उद्घोष है। कुटज की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक नन्हा-सा पौधा भी विकट पहाड़ों पर अपनी जड़ें जमाकर न केवल टिका रहता है, बल्कि फूलों से लदकर फलता-फूलता भी है। यह निबंध हमें बताता है कि जीवन की मुश्किलों के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। कुटज की दृढ़ता, मानव की अदम्य आशावादिता और जीवन जीने की प्रबल इच्छा का एक जीवंत उदाहरण है।
आम फिर बौरा गए: जीवन का चक्रीय सौंदर्य
‘आम फिर बौरा गए’ निबंध वसंत के आगमन पर आम के पेड़ों पर फूली मंजरियों के मादक सौंदर्य और उसकी मोहक सुगंध का मनमोहक चित्रण करता है। ये बौर सिर्फ़ ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं हैं, बल्कि ये नवजीवन, प्रेम और उल्लास के प्रतीक बनकर उभरते हैं। द्विवेदी जी ने इस प्राकृतिक दृश्य को बड़ी सहजता से जीवन की निरंतरता, उसकी परिवर्तनशीलता और शाश्वत ऊर्जा से जोड़ा है। यह हमें बताता है कि कैसे प्रकृति का हर चक्र हमारे जीवन में एक नए उत्साह का संचार करता है।
अशोक के फूल: संस्कृति और सौंदर्य का गहरा नाता
‘अशोक के फूल’ निबंध भारतीय परंपरा, इतिहास और सौंदर्य चेतना को बड़ी कलात्मकता से एक साथ पिरोता है। द्विवेदी जी अशोक के फूलों को केवल सजावट की वस्तु नहीं मानते, बल्कि उन्हें हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों और धार्मिक प्रतीकों से गहराई से जोड़ते हैं। यह निबंध अतीत और वर्तमान के बीच एक जीवंत पुल का काम करता है, जो हमें अपने सौंदर्यबोध के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी नए सिरे से समझने का अवसर देता है। यह फूलों के माध्यम से हमारी समृद्ध विरासत की पड़ताल है।
देवदारु: स्थिरता और गरिमा की प्रतिमूर्ति
‘देवदारु’ वृक्ष के माध्यम से लेखक ने जीवन की लंबी आयु, शांति और आंतरिक स्थिरता को बेहद कलात्मक ढंग से चित्रित किया है। हिमालय की ऊँचाइयों पर अडिग खड़े ये विशाल वृक्ष मानो प्रकृति के तपस्वी हों – शांत, अविचल और बेहद भव्य। यह निबंध हमें जीवन की गंभीरता, उसके स्थायित्व और आध्यात्मिक ऊँचाई की ओर इंगित करता है। देवदारु हमें सिखाता है कि कैसे स्थिरता और गरिमा के साथ जीवन जिया जा सकता है।
इन सभी निबंधों की ख़ासियत यह है कि द्विवेदी जी ने पेड़-पौधों को केवल उनके जैविक रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें मानवीय संवेदनशीलता, गहन आत्मचिंतन और सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा में गद्य का भी एक काव्यात्मक स्पर्श मिलता है, जो पाठक को न केवल जानकारी देता है, बल्कि उसके भीतर तक भावनात्मक हलचल पैदा कर देता है। इन निबंधों को पढ़कर लगता है, जैसे द्विवेदी जी प्रकृति के हर कण में जीवन का कोई गहरा संदेश देख रहे हों।
5. विवेदी जी की वनस्पतियों में ऐसी रुचि का क्या कारण हो सकता है? आज साहित्यिक रचना फलक पर प्रकृति की उपस्थिति न्यून से न्यून होती जा रही है। तब ऐसी रचनाओं का महत्त्व बढ़ गया है। प्रकृति के प्रति आपका दृष्टिकोण रुचिपूर्ण या उपेक्षामय है? इसका मूल्यांकन करें।
उत्तर:
हजारी प्रसाद द्विवेदी की पेड़-पौधों में गहरी दिलचस्पी सिर्फ़ एक साहित्यिक शौक नहीं थी, बल्कि यह उनकी संस्कृति, दर्शन और भावनाओं से जुड़ी सोच का हिस्सा थी। वे भारतीय रीति-रिवाजों और संस्कृति के गहरे जानकार थे, जहाँ पेड़, पौधे, फूल और मौसम सिर्फ़ सुंदरता की निशानी नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का भी ज़रूरी हिस्सा रहे हैं। तुलसी, पीपल, अशोक, आम जैसे पेड़ हमारे साहित्य और जीवन के सिद्धांतों में खास जगह रखते हैं – और द्विवेदी जी ने इसी रिश्ते को अपने निबंधों में बड़े प्यार से दिखाया है।
उनकी साहित्यिक सोच सिर्फ़ वर्णन करने वाली नहीं थी, बल्कि अनुभव और भावनाओं से भरी हुई थी। वे प्रकृति के रूपों में ज़िंदगी के संघर्ष, उसकी लय और हमेशा चलते रहने को देखते थे। उदाहरण के लिए, कुटज के निबंध में मुश्किल हालातों में भी ज़िंदा रहने की ज़िद, और शिरीष के फूल में गर्मी की तपिश के बीच खिलती सुंदरता की शांति, मानो ज़िंदगी के अंदर छिपे दर्शन को हमारे सामने रखती है। द्विवेदी जी के लिए पेड़-पौधे सिर्फ़ सजावट या विज्ञान के विषय नहीं थे, बल्कि वे उन्हें इंसानी ज़िंदगी के एहसासों और भावनाओं के प्रतीक के तौर पर देखना पसंद करते थे।
आज के समय में, जब शहरों का बढ़ना और तकनीकी विकास ने इंसान को प्रकृति से दूर कर दिया है, साहित्य में भी इसका असर दिखता है। आजकल के लेखन में जहाँ पहले मौसमों, फूलों और कुदरती बदलावों का भावनात्मक चित्रण होता था, वहाँ अब लोगों के अपने दुख-दर्द, सामाजिक मुद्दे और शहरी जीवन की उलझनें ज़्यादा दिखाई देती हैं। ऐसे में द्विवेदी जी जैसे लेखक हमें प्रकृति के साथ उस पुराने प्यार की याद दिलाते हैं, जो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है।
जहाँ तक मेरी सोच है, मैं प्रकृति को सिर्फ़ इस्तेमाल करने की चीज़ या मजे का साधन नहीं मानता, बल्कि वह मेरी ज़िंदगी का आधार और प्रेरणा का स्रोत है। प्रकृति की विविधता, संतुलन और शांत जटिलता मुझे बार-बार यह एहसास कराती है कि इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा रिश्ता है, जिसे हमें समझना चाहिए, बनाए रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। द्विवेदी जी की रचनाएँ इसी भावना को और मज़बूत करती हैं – वे यह सिखाती हैं कि प्रकृति में सिर्फ़ दिखने वाली सुंदरता नहीं, बल्कि एक हमेशा रहने वाला जीवन का दर्शन छिपा है जिसे महसूस करना और अपनाना, आज की दुनिया में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
- भाषा की बात
1. दस दिन फूले फिर खंखड़-खंखड़ इस लोकोक्ति से मिलते-जुलते कई वाक्यांश पाठ में हैं, उन्हें छाँट कर लिखें।
उत्तर:
हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध ‘शिरीष के फूल’ जीवन की नश्वरता, समय के अथक प्रवाह और हर चीज़ के अंत की अनिवार्यता को विभिन्न स्तरों पर अभिव्यक्त करता है। “दस दिन फूले फिर खंखड़-खंखड़” यह कहावत सीधे तौर पर इस विचार को पुष्ट करती है कि सुंदरता, शक्ति या स्वयं जीवन कुछ भी स्थायी नहीं है। निबंध में कई वाक्यों के माध्यम से इस गहन भाव को और भी गहरा किया गया है।
जैसे, “काल की गति बड़ी विचित्र है” यह वाक्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समय का बहाव कितना अप्रत्याशित और अनियंत्रित है। इसे न तो पूरी तरह समझा जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। यह हर परिवर्तन की मूल वजह है। इसी तरह, “अकाल पुरुष थोड़े ही दिनों के लिए फूलता है” यह संकेत देता है कि बिना किसी ठोस आधार या वास्तविक गुण के मिली प्रसिद्धि या चमक-दमक बहुत कम समय के लिए होती है।
“सब पुराने ढह जाते हैं” और “समय की मार से सब जर्जर हो जाते हैं” जैसे वाक्य हमें बार-बार यह याद दिलाते हैं कि समय के प्रभाव से कोई भी चीज़ अछूती नहीं रह सकती – चाहे वह सदियों पुरानी इमारतें हों, हमारे आपसी रिश्ते हों या हमारा अपना शरीर। हर चीज़ का क्षरण अटल है।
निबंध में “आज नहीं तो कल अवश्य भावी है” यह वाक्य मृत्यु की अनिवार्यता को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। यह हमें बताता है कि जीवन कितना भी लंबा क्यों न हो, एक दिन इसका अंत सुनिश्चित है। “सब कुछ नश्वर है” यह तो सीधे तौर पर इस सच्चाई का एलान है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है।
जब लेखक कहते हैं, “जहाँ बैठना हो, वहीं थोड़ी देर सुख से बैठो”, तो वे जीवन की अनिश्चितता के बीच उस पल भर के सुख को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देते हैं जो हमारे पास अभी मौजूद है। यह वर्तमान क्षण के महत्व की ओर हमारा ध्यान खींचता है।
जब लेखक शिरीष के फूलों के संदर्भ में कहते हैं, “वे भी झड़ जाएँगे”, तो वह प्रकृति के अटल चक्र और जीवन की स्वाभाविक, शांतिपूर्ण समाप्ति को स्वीकार करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
इन सभी वाक्यों का निचोड़ यही है कि जीवन में हर चीज़ – चाहे वह सुंदरता हो, यश हो, हमारे संबंध हों या हमारा शरीर – समय के साथ मुरझाने और अंत होने के लिए बाध्य है। शिरीष का फूल, जो भीषण गर्मी में भी खिलता है और फिर धीरे-धीरे मुरझा जाता है, उसी क्षणभंगुरता का प्रतीक है – यह हमें याद दिलाता है कि चाहे वैभव हो या कठिनाई, उसका अंत निश्चित है। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करना ही जीवन की वास्तविक गहराई को समझना है।