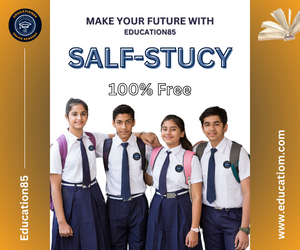रजनी’ कहानी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते व्यावसायिकरण पर एक करारा प्रहार है। कहानी की नायिका रजनी, एक साधारण गृहिणी होते हुए भी, अपने बेटे अमित के कम अंकों के पीछे छिपी शिक्षा की दूषित व्यवस्था के खिलाफ़ आवाज़ उठाती है।
रजनी का दृढ़ निश्चय और न्यायप्रिय स्वभाव उसे इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति देता है। जब शिक्षक श्री पाठक द्वारा निजी ट्यूशन के लिए दबाव डाला जाता है और ऐसा न करने पर अंक काट लिए जाते हैं, तो रजनी इसे शिक्षा के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन मानती है।
वह इस अन्याय को व्यक्तिगत समस्या न मानकर, एक व्यापक सामाजिक बुराई के रूप में देखती है। प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी से शुरुआती समर्थन न मिलने के बावजूद, रजनी हार नहीं मानती। उसकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता उसे अखबार के संपादक से मिलने और अन्य अभिभावकों को एकजुट करने में मदद करती है।
अभिभावकों की बैठक में, रजनी का सुझाव कि निजी ट्यूशन को अनिवार्य करने के खिलाफ नियम बनाया जाए, उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह व्यक्तिगत समस्या को एक सामूहिक आंदोलन में बदल देता है।
अंततः, रजनी की जीत केवल उसकी ही नहीं, बल्कि उन सभी की जीत होती है जो शिक्षा को एक व्यवसाय बनाने के विरुद्ध थे। शिक्षा बोर्ड द्वारा जाँच और गलत प्रथाओं पर रोक लगाना दर्शाता है कि एकजुट प्रयास से बदलाव संभव है। ‘रजनी’ हमें प्रेरित करती है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी हिम्मत और लगन से बड़े परिवर्तन ला सकता है, और हमें अन्याय के खिलाफ़ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए। यह कहानी शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को पुनः स्थापित करने का आह्वान करती है।
पाठ के साथ
1)रजनी ने अमित के मुददे को गंभीरता से लिया, क्योंकि-
(क) वह अमित से बहुत स्नेह करती थी।
(ख) अमित उसकी मित्र लीला का बटा था।
(ग) वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामथ्य रखती थी।
(घ) उस अखबार की सुखियों में आने का शौक था।
उत्तर:रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से इसलिए लिया क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। हालाँकि यह सच है कि अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था और रजनी उससे स्नेह करती थी, उसकी इस मामले में गहरी दिलचस्पी और गंभीरता का मुख्य कारण अन्याय को सह न पाना था। रजनी एक ऐसी महिला थीं जो गलत होते देख चुप नहीं रह सकती थीं और उसमें इतनी हिम्मत और क्षमता थी कि वह उसके खिलाफ खड़ी हो सकें। अन्य विकल्प, जैसे कि अमित का प्रभावशाली व्यक्ति होना या रजनी का स्वभाव से झगड़ालू होना, कहानी में रजनी के चरित्र को सही ढंग से नहीं दर्शाते हैं।
2)जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है, तभी उसके माँ-बाप दयूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है, तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएँ. यह कोई मजबूरी तो है नहीं-प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएँ कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए।
उत्तर:यह संवाद एक विशिष्ट प्रसंग में कहा गया होगा जहाँ किसी अभिभावक या व्यक्ति ने ट्यूशन की आवश्यकता पर अपनी राय व्यक्त की है। यह बात कुछ हद तक सही भी है कि कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है, और अगर कोई शिक्षक अनुचित फायदा उठा रहा है, तो उससे ट्यूशन न लेना बेहतर है।
हालाँकि, यह दृष्टिकोण पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि ट्यूशन केवल कमजोर छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि जो बच्चे अपने ज्ञान को और मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। साथ ही, शिक्षकों पर सामान्यीकरण करना उचित नहीं—अधिकतर शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अगर कोई शिक्षक गलत व्यवहार करे, तो उसकी शिकायत करनी चाहिए न कि सभी को एक ही नजरिए से देखना चाहिए।
3)तो एक और आदोलन का मसला मिल गया-फुसफुसाकर कही गई यह बात-
(क) किसने किस प्रसंग में कही?
(ख) इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है?
उत्तर : (क) यह बात जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कही थी, जब उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और नए आंदोलन की संभावना है।
(ख) इससे पता चलता है कि वह सतर्क, रणनीतिक और आशावादी थे। वह समझते थे कि जनता का आक्रोश बढ़ रहा है और इसे सही दिशा देकर आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है।
4)रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर-
(क) अमित का पर्चा सचमुच खराब होता।
(ख) संपादक रजनी का साथ न देता।
उत्तर:रजनी धारावाहिक की मुख्य समस्या
रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या बच्चों की शिक्षा के व्यवसायीकरण और परीक्षा प्रणाली में व्याप्त धांधली है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक ट्यूशन सेंटर का मालिक, अमित के पिता को यह विश्वास दिलाता है कि अमित का परीक्षा परिणाम उसके ट्यूशन सेंटर की वजह से अच्छा आया है, जबकि असल में वह बच्चों के पर्चे बदलवा कर या गलत जानकारी देकर उन्हें पास करवाता है ताकि लोग उसके सेंटर में आएं। रजनी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है।
क्या होता अगर…
(क) अमित का पर्चा सचमुच खराब होता:
अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता, तो रजनी के लिए ट्यूशन सेंटर के मालिक की धोखाधड़ी को उजागर करना और भी मुश्किल हो सकता था। अमित के पिता को शायद इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि ट्यूशन सेंटर ने कुछ गलत किया है, क्योंकि परिणाम तो खराब होता। ऐसे में, रजनी को शायद अन्य सबूतों या अन्य प्रभावित बच्चों के माता-पिता की मदद लेनी पड़ती ताकि वह अपनी बात साबित कर सके।
(ख) संपादक रजनी का साथ न देता:
अगर संपादक रजनी का साथ न देता, तो रजनी की आवाज दब सकती थी। अख़बार एक महत्वपूर्ण मंच होता है जो समाज में बदलाव ला सकता है। संपादक के समर्थन के बिना, रजनी को अपनी बात जनता तक पहुंचाने में काफी मुश्किल होती। हो सकता है कि उसकी कोशिशें व्यक्तिगत स्तर पर ही रह जातीं और इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश बड़े पैमाने पर न हो पाता। संपादक का समर्थन रजनी को एक मजबूत सहारा देता है जिससे वह अपनी लड़ाई लड़ पाती है।
पाठ के आस-पास
1)गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बदश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता-इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं?
उत्तर:यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी अन्याय में व्यक्ति और व्यवस्था दोनों की भूमिका होती है। जहाँ एक तरफ अध्यापक का गलत आचरण सीधे तौर पर ज़िम्मेदार है, वहीं दूसरी तरफ कमज़ोर और अपारदर्शी व्यवस्था भी इस अन्याय को बढ़ने देती है।
सही मायने में, रजनी का संघर्ष सिर्फ उस अध्यापक के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के ख़िलाफ़ है जो ऐसे शोषण को बढ़ावा देती है या उस पर अंकुश लगाने में विफल रहती है। इसलिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि गलती करने वाले से ज़्यादा दोषी वो व्यवस्था है जो उसे ऐसा करने की अनुमति देती है। एक मजबूत और जवाबदेह प्रणाली ही ऐसे लोगों को पनपने से रोक सकती है और अन्याय को संस्थागत होने से बचा सकती है।
2)स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है?
उत्तर:रजनी का चेहरा स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से कई मायनों में अलग था। परंपरागत रूप से स्त्रियों को अक्सर विनम्र, शांत और घरेलू भूमिकाओं तक सीमित माना जाता है, जो सामाजिक नियमों का पालन करती हैं और अपनी आवाज नहीं उठातीं।
इसके विपरीत, रजनी का चेहरा आत्मविश्वास, दृढ़ता और संघर्षशीलता को दर्शाता था। वह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली, अपने हक के लिए लड़ने वाली और समाज में बदलाव लाने का माद्दा रखने वाली स्त्री थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कमजोरी या लाचारी नहीं थी, बल्कि एक साहसिक और निडर व्यक्तित्व की झलक थी।
वह सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की समस्याओं के लिए भी संघर्ष करती थी, जो उसे ‘कोमल’ या ‘पिछलग्गू’ मानी जाने वाली स्त्री की छवि से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। रजनी का चेहरा यह बताता था कि एक स्त्री मजबूत, स्वतंत्र और परिवर्तन लाने वाली भी हो सकती है।
3)पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्ठक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया तो आप कौन-कौन-से निर्देश देंगे?
उत्तर:दृश्य फिल्माने के संक्षिप्त निर्देश:
लोकेशन: दृश्य के अनुसार सेट तैयार करें (जैसे पार्क या ऑफिस)।
कैमरा एंगल: पहले वाइड शॉट लें, फिर किरदारों के भाव दिखाने के लिए क्लोज-अप।
लाइटिंग: मूड के हिसाब से रोशनी (पार्क के लिए नरम, ऑफिस के लिए तेज)।
एक्टर्स के भाव: चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें।
बैकग्राउंड साउंड: लोकेशन के अनुसार आवाज़ें जोड़ें (पक्षियों की आवाज़ या ऑफिस की धीमी आवाज़ें)।
4)इस पटकथा में दृश्य-संख्या का उल्लेख नहीं है। मगर गिनती करें तो सात दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे?
उत्तर:दृश्यों का विभाजन
- पहला दृश्य: रजनी लीला के घर जाती है और अमित के कम अंकों पर चर्चा करती है.
- दूसरा दृश्य: रजनी हेडमास्टर के कार्यालय में अमित के मुद्दे पर बात करती है.
- तीसरा दृश्य: रजनी शिक्षा निदेशक के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराती है.
- चौथा दृश्य: रजनी संपादक के कार्यालय में अमित की समस्या बताती है.
- पाँचवाँ दृश्य: अभिभावकों की एक बड़ी मीटिंग होती है.
- छठा दृश्य: रजनी शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत करती है (जिसका ज़िक्र है).
- सातवाँ दृश्य: अमित अच्छे अंकों के साथ आता है और लीला रजनी को धन्यवाद देती है, जो कहानी का सुखद अंत दर्शाता है.
भाषा की बात
1)निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए-
(क) वरना तुम तो मुझे काट ही देतीं।
(ख) अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लता, हमलोग खा थोड़े ही सकते हैं।
(ग) बस-बस मैं समझ गया।
उत्तर:काट देना
इसका अर्थ है किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना या गहरी पीड़ा देना, चाहे वह भावनात्मक हो या शारीरिक.
भोग नहीं लगा लेना
इस वाक्यांश का मतलब है कि जब तक कोई ख़ास व्यक्ति (जैसे यहाँ अमित) खाना शुरू न करे, तब तक दूसरे लोग भोजन नहीं कर सकते. यह किसी परंपरा या सम्मान को दर्शाता है.
बस-बस मैं समझ गया
इस वाक्यांश का प्रयोग तब करते हैं जब बोलने वाले को पूरी बात समझ आ गई हो और उसे आगे सुनने की ज़रूरत न हो. यह सामने वाले को रोकने के लिए कहा जाता है.
कोड मिक्सिंग/कोड स्विचिग
1)कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? क्हेरी द्वटरेस्टिग सब्जेक्ट।
ऊपर दिए गए संवाद में दो पंक्तियाँ हैं पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है जबकि शेष हिंदी भाषा का है। दूसरा वाक्य पूरी तरह अंग्रेजी में है। हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में दो भाषाओं (कोड) का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड मिक्सिंग कहलाता है। जबकि एक भाषा में बोलते-बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। पाठ में से कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के तीन-तीन उदाहरण चुनिए और हिंदी भाषा में रूपांतरण करके लिखिए।
उत्तर:पाठ “रजनी” में कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, साथ ही उनका हिंदी में मतलब भी बताया गया है:
कोड मिक्सिंग (एक ही सेंटेंस में दो भाषाएँ):
- जैसा लिखा है: “वरना तुम तो मुझे कट ही देतीं, यू नो।”
- मतलब: “वरना तुम तो मुझे काट ही देतीं, जानती हो।” (यहाँ “यू नो” अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिंदी वाक्य में इस्तेमाल किया गया है।)
- जैसा लिखा है: “अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हमलोग खा थोड़े ही सकते हैं, आई मीन।”
- मतलब: “अमित जब तक तुम्हें प्रणाम नहीं कर लेता, हमलोग खा थोड़े ही सकते हैं, मेरा मतलब है।” (यहाँ “आई मीन” अंग्रेजी का वाक्यांश है जो हिंदी वाक्य में आया है।)
- जैसा लिखा है: “इट्स नॉट माई प्रॉब्लम।”
- मतलब: “यह मेरी समस्या नहीं है।” (पूरा सेंटेंस ही अंग्रेजी का है, पर बातचीत के दौरान हिंदी बोलने वाला इसे ऐसे ही बोल रहा है।)
कोड स्विचिंग (बोलते-बोलते पूरी भाषा बदल देना):
मतलब: “लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता।” (यह पूरा सेंटेंस अंग्रेजी में बोला गया है, जबकि आसपास हिंदी में बातचीत हो रही है।)
जैसा लिखा है: “कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? क्हेरी द्वटरेस्टिग सब्जेक्ट।”
मतलब: “कोई शोध परियोजना है क्या? बहुत दिलचस्प विषय।” (पहले हिंदी में सवाल पूछा गया, फिर पूरी तरह से अंग्रेजी में राय दी गई।)
जैसा लिखा है: “(संपादक का फुसफुसाना) यू आर एब्सोल्यूटली राइट।”
मतलब: “(संपादक का फुसफुसाना) आप बिल्कुल सही हैं।” (संपादक हिंदी में बात सुन रहा है, फिर अचानक पूरी तरह से अंग्रेजी में अपनी सहमति जताता है।)
जैसा लिखा है: “बट आई कांट हेल्प इट।”