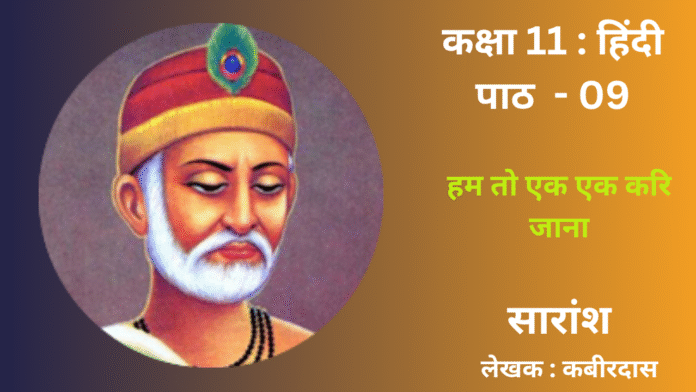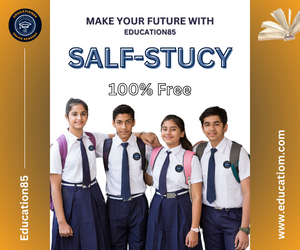‘हम तो एक एक करि जाना’ कबीर द्वारा रचित एक पद है जिसमें उन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन करते हुए ईश्वर की एकता का प्रतिपादन किया है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, उसे अलग-अलग रूपों में देखना अज्ञानता है।
कबीर पहले पंक्ति में ही दृढ़ता से कहते हैं कि उन्होंने तो ईश्वर को एक ही जाना है। वे उन लोगों पर व्यंग्य करते हैं जो ईश्वर को दो मानते हैं और इस प्रकार भ्रम में पड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोगों को नरक की आग में जलना पड़ेगा।
कबीर दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि यह संसार उसी प्रकार एक है जैसे पवन एक ही है, पानी एक ही है और ज्योति (प्रकाश) भी एक ही है जो सभी में समाई हुई है। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है।
कबीर आगे कहते हैं कि यदि कोई कुम्हार एक ही मिट्टी को सानकर अलग-अलग तरह के बर्तन बनाता है, तो क्या उन बर्तनों में कोई अंतर होता है? उसी प्रकार, ईश्वर तो एक ही है, फिर उसे अलग-अलग रूपों में क्यों देखा जाता है?
कबीर अंत में कहते हैं कि जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं कि ईश्वर एक ही है, वे भय और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। वे हर प्राणी में उसी एक ईश्वर को देखते हैं और समदृष्टि रखते हैं। कबीर का यह पद ईश्वर की एकता और अद्वैत के ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करता है।
पद के साथ
1)कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं?
उत्तर:कबीरदास जी ने ईश्वर की एकता पर सरल तर्क दिए हैं। उनके अनुसार:
सभी धर्मों में एक ईश्वर – “अलह-राम के नाम अलग, दोनों एक हैं महराज।” नाम भिन्न, पर सत्ता एक।
ईश्वर सर्वव्यापी – “मोको कहाँ ढूँढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।” वह हर जगह और हृदय में विद्यमान है।
मूर्ति पूजा का विरोध – “पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूँ पहार।” ईश्वर मूर्तियों में नहीं, भक्ति में है।
राम-रहीम एक – “दुई जग दरबार लगे, एक है राम-रहीम।” धर्म अलग, पर देवता एक।
सच्ची भक्ति ज़रूरी – “माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर।” बाहरी आडंबर नहीं, शुद्ध मन से पूजा करो।
कबीर की शिक्षा सरल है: ईश्वर एक है, उसे पाने के लिए प्यार और सच्चाई काफी है।
2)मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है?
उत्तर:मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों (पाँच मूलभूत तत्वों) से हुआ है, जिन्हें प्राचीन भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना गया है। ये पंच तत्व निम्नलिखित हैं:
पृथ्वी (भूमि) – यह तत्व शरीर की ठोस संरचना जैसे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा और ऊतकों के लिए उत्तरदायी है।
जल (आप) – यह शरीर में उपस्थित तरल पदार्थों जैसे रक्त, लार, पसीना और कोशिकाओं के अंदर का द्रव्य का प्रतिनिधित्व करता है।
अग्नि (तेज) – यह तत्व शरीर की ऊर्जा, पाचन क्रिया, उष्मा और चयापचय (मेटाबॉलिज्म) से जुड़ा है।
वायु (प्राण) – यह श्वास, गति और सभी शारीरिक प्रक्रियाओं में होने वाली गतिविधियों का प्रतीक है।
आकाश (शून्य) – यह तत्व शरीर में रिक्त स्थानों जैसे कोशिकाओं के बीच का स्थान, मुख, नाक और आंतरिक अंगों के खाली भागों को दर्शाता है।
इन पंच तत्वों के संतुलन से ही मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है, जबकि इनमें असंतुलन होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद और योग में इन तत्वों को संतुलित करने के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं।
3)जैसे बाढ़ी काष्ट ही कार्ट अगिनि न कार्ट कोई।
सब छटि अंतरि तूही व्यापक धरे सरूपै सोई।
इसके आधार पर बताइए कि कबीर की वृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है?
उत्तर:कबीर के इस दोहे में ईश्वर के स्वरूप को अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक रूप में व्यक्त किया गया है। इन पंक्तियों के अनुसार, कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी में आग छिपी होती है, उसी प्रकार ईश्वर सभी के अंदर विद्यमान है। वे बताते हैं कि ईश्वर किसी बाहरी वस्तु या रूप में सीमित नहीं है, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है और सभी के हृदय में छिपा हुआ है।
कबीर के अनुसार, ईश्वर निराकार (बिना किसी विशेष रूप वाला), सर्वव्यापी और अंतर्यामी (सभी के अंदर देखने-जानने वाला) है। वह किसी एक रूप या नाम तक सीमित नहीं, बल्कि सभी जगह मौजूद है। इस दोहे में कबीर ने ईश्वर की अनुभूति को आंतरिक बताया है, यानी उसे पाने के लिए बाहरी आडंबरों की नहीं, बल्कि अपने मन की शुद्धता और आत्मज्ञान की आवश्यकता है।
इस प्रकार, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक सच्चिदानंद (सत्य, चेतना और आनंद स्वरूप), निर्गुण (गुणों से परे) और सर्वत्र विद्यमान सत्ता है, जिसे साधक अपने अंतःकरण में ही अनुभव कर सकता है।
4)कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है?
उत्तर:कबीरदास जी के विषय में आपकी यह व्याख्या बिलकुल सटीक है। जिस प्रकार कबीर ने स्वयं को ‘दीवाना’ कहा, उसमें उनकी अद्वितीय अंतर्दृष्टि और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का गहरा अर्थ छिपा है।
कबीर का परम सत्य का अनुभव उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करता था। उनका ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके लिए दुनियावी रिश्ते-नाते और समाज के बनाए नियम-कायदे गौण हो जाते थे। जो व्यक्ति इस भौतिक संसार की मोह-माया में लिप्त न हो, और जिसकी चेतना किसी उच्चतर आयाम से जुड़ी हो, उसे यह दुनिया अक्सर ‘पागल’ या ‘दीवाना’ ही मानती है। यह ‘दीवानापन’ दरअसल उनकी गहरी आध्यात्मिक तल्लीनता का प्रतीक था।
इसके अतिरिक्त, कबीर का स्वभाव निर्भीक और स्पष्टवादी था। उन्होंने कभी भी समाज के तथाकथित ठेकेदारों या प्रचलित मान्यताओं का लिहाज़ नहीं किया। उनकी सीधी-सादी, लेकिन खरी-खरी बातें तत्कालीन समाज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थीं। वे उन लोगों के लिए अजीब थे जो सदियों से चली आ रही रूढ़ियों और आडंबरों को ही सत्य मानते थे।
इसलिए, जब कबीर ने स्वयं को ‘दीवाना’ कहा, तो यह केवल उनका आत्म-बोध नहीं था, बल्कि यह उस दुनिया पर एक तीखा व्यंग्य भी था जो उनकी सच्चाई, उनके अनुभव और उनके निर्भीक विचारों को समझने में असमर्थ थी। यह उनके अनोखे आध्यात्मिक अनुभव और अदम्य साहस का एक अनुपम संगम था, जिसने उन्हें समय से परे एक अमर कवि और संत बना दिया।
पद के आस-पास
प्रश्न 1:
अन्य संत कवियों नानक, दादू और रैदास आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर एक परिचर्चा करें।
उत्तर:निर्गुण संत कवियों का भक्ति आंदोलन में योगदान
भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले संत कवियों ने निराकार ईश्वर की भक्ति पर विशेष ज़ोर दिया। इन संतों ने आडंबर और बाहरी दिखावों का पुरज़ोर विरोध किया और प्रेम तथा गुरु के महत्व को सर्वोपरि माना। उनके विचारों ने समाज में गहरा प्रभाव डाला और आज भी प्रासंगिक हैं।
कबीर ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंडों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्होंने अपनी साखियों और सबदों के माध्यम से सीधे तौर पर विद्रोह का बिगुल फूंका और ईश्वर को किसी एक धर्म या जाति में सीमित न करके, उसे हर प्राणी में देखने का संदेश दिया।
गुरु नानक देव ने इसी निराकार भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिख धर्म की नींव रखी। उन्होंने ‘एक ओंकार’ का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और सभी मनुष्य समान हैं। नानक देव ने जातिवाद का खंडन किया और समाज में समानता व भाईचारे का प्रसार किया।
दादू दयाल ने एकता और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने सभी धर्मों की मूल भावना को एक समान बताया और मानव सेवा को ही ईश्वर की सच्ची भक्ति माना। दादू पंथ उनके विचारों पर आधारित है, जो आज भी प्रेम और सहिष्णुता की शिक्षा देता है।
संत रैदास ने अपने जीवन और वाणी से समानता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव को चुनौती दी और बताया कि भक्ति किसी जाति या वर्ण की मोहताज नहीं होती। रैदास के भजन और पद आज भी समाज में समरसता और समानता का भाव जगाते हैं।
इन संत कवियों ने न केवल भक्ति आंदोलन को एक नया आयाम दिया, बल्कि सामाजिक सुधार और मानवीय मूल्यों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उपदेश आज भी हमें प्रेम, एकता और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।