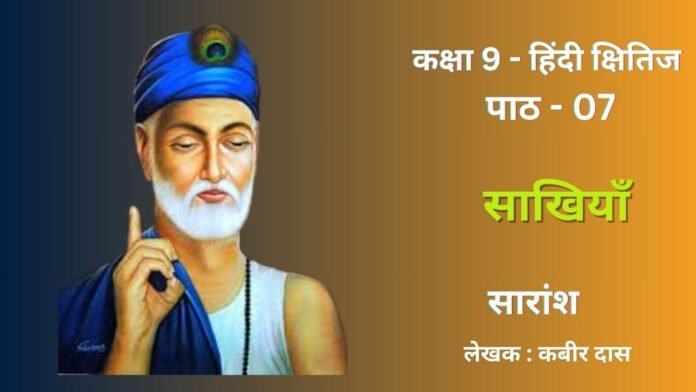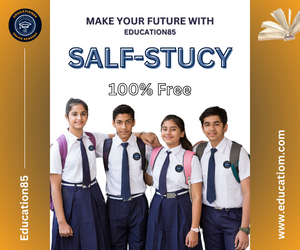NCERT Solutions for Class 9 Hindi Chapter 7
“साखियाँ” कबीर दास की रचना है, जो छोटी-छोटी पंक्तियों (साखियों) का संग्रह है। कबीर दास 15वीं शताब्दी के भारतीय संत कवि थे, जिन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद का विरोध किया और सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उनकी कविता में सरलता, सीधापन और गहन ज्ञान की झलक मिलती है।
“साखियाँ” में कबीर दास ने सरल भाषा और छवियों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया है। उन्होंने अक्सर विरोधाभासों और विडंबनाओं का प्रयोग करके मानवीय समझ की सीमाओं और आंतरिक अनुभव के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने सांसारिक मोह माया से मुक्ति, सभी प्राणियों की एकता और ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वास और बाहरी रीति-रिवाजों की निंदा की और आंतरिक अनुभव के माध्यम से ईश्वर के दर्शन का मार्ग बताया।
NCERT Solutions for Class 9 Hindi Chapter 7
प्रश्न- अभ्यास
साखियाँ
1. ‘मानसरोवर’ से कवि का क्या आशय है?
उत्तर :
कबीर दास ने अपनी कविताओं में ‘मानसरोवर’ शब्द का प्रयोग अत्यंत गहनता से किया है। यह शब्द उनके लिए केवल एक भौगोलिक स्थल का नाम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अवधारणा है। ‘मानसरोवर’ कबीर दास के लिए हमारे हृदय का प्रतीक है, जहां हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। यह ज्ञान का सागर भी है, जहां से हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। ‘मानसरोवर’ हमारे अंतर्मन की भी प्रतिमूर्ति है, जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का सामना करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार, यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी दर्शाता है। कबीर दास ने स्पष्ट किया है कि मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थल में जाने से ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि हमें अपने भीतर, अपने ‘मानसरोवर’ में ही ईश्वर को खोजना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने मन को शांत करके ध्यान लगाते हैं, तभी हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार, ‘मानसरोवर’ कबीर दास की आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो हमें आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है।
2. कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है ?
उत्तर :
कबीर दास ने सच्चे प्रेमी के गुणों को विस्तार से बताया है। उनके अनुसार, सच्चा प्रेमी निष्काम भाव से भक्ति करता है, अर्थात् वह किसी स्वार्थ या फल की आशा के बिना ईश्वर की भक्ति करता है। वह सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है और जाति-पांत से ऊपर उठकर सभी के कल्याण की कामना करता है। सच्चा प्रेमी सत्यनिष्ठ होता है, झूठ और कपट से दूर रहता है। वह सांसारिक सुखों से विरक्त रहकर ईश्वर के अनादि आनंद की तलाश में रहता है। कठिनाइयों और विपत्तियों में भी उसका विश्वास डगमगाता नहीं है। वह दूसरों की सेवा को अपना धर्म मानता है और उनके दुख-दर्द में शामिल होता है। इस प्रकार, सच्चा प्रेमी वह है जो इन सभी गुणों को अपने जीवन में धारण करता है और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण रखता है।
3. तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है?
उत्तर :
कबीर दास के तीसरे दोहे में सहज ज्ञान को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह वह ज्ञान है जो किसी विशेष प्रयास या अध्ययन के बिना, सहज ही प्राप्त होता है। यह आंतरिक अनुभव और अनुभूति पर आधारित होता है, न कि बाहरी ग्रंथों या शिक्षकों पर। कबीर दास मानते हैं कि यह ज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से आता है और हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है। उन्होंने बाहरी ग्रंथों और शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय, स्वयं अनुभव करके सत्य को जानने की बात कही। सहज ज्ञान आंतरिक शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह व्यक्ति को अपने भीतर स्थित ईश्वर को खोजने में मदद करता है। इस प्रकार, कबीर दास ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें जटिल धार्मिक ग्रंथों और रीति-रिवाजों में उलझे रहने की बजाय, अपने भीतर झांककर सत्य को खोजना चाहिए।
4. इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है?
उत्तर :
कबीर दास के अनुसार, सच्चा संत वह होता है जो सभी में ईश्वर को देखता है। जाति-पांत, धर्म-मजहब से ऊपर उठकर वह सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है। वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है और किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखता। सच्चा संत सत्य का पालन करता है और झूठ, कपट से दूर रहता है। वह सांसारिक सुखों से विरक्त रहता है और मोह-माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। वह अपने भीतर ही ईश्वर को खोजता है और सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करता है।
5. अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है?
उत्तर :
कबीर दास ने अपने दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उन्होंने धार्मिक, जातिगत, और अन्य प्रकार के भेदभाव का विरोध किया। कबीर दास सभी मनुष्यों को समान मानते थे और उन्होंने जाति-पांत, धर्म-मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को खारिज किया। उन्होंने सभी प्राणियों में ईश्वर को देखा और सभी के कल्याण की कामना की। कबीर दास ने बाहरी दिखावे और रीति-रिवाजों के बजाय, आंतरिक गुणों को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची सुंदरता आंतरिक होती है, बाहरी रूप मात्र क्षणिक है।
कबीर दास के दोहे हमें इन सभी संकीर्णताओं से मुक्त होकर एक समान समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सभी मनुष्य एक हैं और हमें सभी के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए।
NCERT Solutions for Class 9 Hindi Chapter 7
6. किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
उत्तर :
कबीर दास के अनुसार, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। उन्होंने इस बात को कई दोहों में स्पष्ट किया है।
कबीर दास के विचार:
कबीर दास मानते थे कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कुल, जाति या धर्म के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सोने के बर्तन में विष भी हो सकता है, और एक मिट्टी के बर्तन में अमृत भी। इसी तरह, उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी नीच कर्म कर सकता है, और निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी महान कार्य कर सकता है।
कर्मों का महत्व: कबीर दास के अनुसार, व्यक्ति के कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मानित रहेगा, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो।
कुल का महत्व नहीं: उन्होंने कहा कि कुल या जन्म से व्यक्ति के गुणों का निर्धारण नहीं होता। एक ही परिवार में जन्मे लोग भी अलग-अलग स्वभाव और गुणों के हो सकते हैं।
समाज में समानता: कबीर दास ने सभी मनुष्यों को समान माना और जाति-पाति के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं।
7. काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए-
हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारि ।
स्वान रूप संसार है, भूँकन दे झख मारि ।
Ans :
कबीर दास के इस दोहे में अद्वितीय काव्य सौंदर्य निहित है। उन्होंने ज्ञान को हाथी से और संसार को कुत्ते से जोड़कर एक अद्भुत रूपक का सृजन किया है। यह रूपक ज्ञान की महत्ता को सहजता से उजागर करता है, जहां ज्ञान एक विशाल हाथी की तरह है, जो मनुष्य को संसार के मोह-माया (कुत्ते) से ऊपर उठाता है। “सहज दुलीचा डारि” में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जहां ज्ञान प्राप्ति की सहजता को गलीचा बिछाने जैसा सरल बताया गया है।
इस दोहे में यमक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, “भूँकन दे झख मारि” में ‘भूँकन’ और ‘झख’ शब्दों की पुनरावृत्ति से ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न होता है। यह दोहा न केवल ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि संसार के मोह-माया से मुक्ति पाने का मार्ग भी दर्शाता है। कवि ने सरल भाषा का प्रयोग करते हुए गहनतम विचारों को व्यक्त किया है, जो इस दोहे की सौंदर्य और प्रभावशीलता को और भी बढ़ा देता है।
NCERT Solutions for Class 9 Hindi Chapter 7
सबद
8. मनुष्य ईश्वर को कहाँ-कहाँ ढूँढ़ता फिरता है ?
उत्तर :
मनुष्य सदियों से ईश्वर की खोज में रहा है। इस खोज में उसने कई रास्ते अपनाए हैं। वह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों जैसे धार्मिक स्थलों पर जाता है। तीर्थस्थल जैसे काशी, मथुरा, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि की यात्राएं भी करता है। प्रकृति की गोद में भी वह ईश्वर की खोज करता है – पहाड़ों, नदियों, समुद्रों और जंगलों में। योग, ध्यान और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से भी वह आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करता है। वेद, कुरान, बाइबल जैसे धर्मग्रंथों का अध्ययन करता है और गुरुओं के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है।
हालांकि, कबीर दास के अनुसार, ईश्वर को इन बाहरी स्थानों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में; वह न कर्मकांड करने में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं। कबीर दास ने कहा कि ईश्वर सबके अंदर है और उसे सच्चे मन से खोजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को ढूँढने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी।
9. कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों खंडन किया है?
उत्तर :
कबीर दास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित कई विश्वासों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा, योग, वैराग्य, कर्मकांड आदि बाहरी दिखावे मात्र हैं। इनसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। उन्होंने कहा कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में; वह न कर्मकांड करने में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं।
कबीर दास ने जाति-पाति, धर्म-मजहब के आधार पर भेदभाव को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सबके अंदर है और सभी एक समान हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे मन से उसकी भक्ति करनी चाहिए। बाहरी रीति-रिवाजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है।
10. कबीर ने ईश्वर को ‘सब स्वाँसों की स्वाँस में’ क्यों कहा है?
उत्तर :
कबीर दास ने ईश्वर को “सब स्वाँसों की स्वाँस में” कहकर एक गहरा और सार्वभौमिक सत्य प्रकट किया है। इस कथन का अर्थ है कि ईश्वर हर जीवित प्राणी के अंदर व्याप्त है। वह हर सांस में, हर कण में मौजूद है। ईश्वर केवल मंदिरों, मस्जिदों या धार्मिक स्थलों में नहीं है, बल्कि वह जीवन का स्रोत है, हर प्राणी की आत्मा में निवास करता है। कबीर दास ने इस कथन के माध्यम से हमें बताया कि ईश्वर को पाने के लिए हमें बाहरी दिखावों और रीति-रिवाजों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें मंदिरों, मस्जिदों में नहीं, बल्कि अपने ही हृदय में देखना चाहिए। यह कथन सभी जीवों की एकता और ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। यह हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि सभी जीवों में ईश्वर का वास है।
11. कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आँधी से क्यों की?
उत्तर :
कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से नहीं, बल्कि आँधी से की है। यह तुलना ज्ञान के तीव्र और व्यापक प्रभाव को दर्शाती है। सामान्य हवा धीरे-धीरे बहती है और किसी चीज में ज्यादा बदलाव नहीं लाती है, जबकि आँधी तेज गति से चलती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को प्रभावित करती है। यह पेड़ों को उखाड़ सकती है, घरों को गिरा सकती है और पूरे परिदृश्य को बदल सकती है।
इसी प्रकार, ज्ञान भी व्यक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। यह अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और व्यक्ति को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। ज्ञान व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को बदल सकता है। ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि यह व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकता है। यह व्यक्ति को अपने आप को और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है।
12. ज्ञान की आँधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर :
कबीर दास ने ज्ञान को आँधी की तरह प्रस्तुत किया है, जिसका प्रभाव भक्त के जीवन पर गहरा और परिवर्तनकारी होता है। ज्ञान की यह ‘आँधी’ भक्त के मन में व्याप्त अज्ञानता, शंकाओं और भ्रमों को दूर करती है, मानो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाती हो। यह उसे संसार के मोह-माया के बंधनों से मुक्त करती है, सांसारिक सुख-दुखों से ऊपर उठाती है और ईश्वर की भक्ति में लीन कर देती है। ज्ञान की इस आँधी से भक्त के मन का पवित्रिकरण होता है, वह निष्कलंक हो जाता है और उसे कोई भी सांसारिक विकार प्रभावित नहीं कर पाता। यह आँधी भक्त में आत्मज्ञान का उदय करती है, वह अपने आप को और ईश्वर को एक ही समझने लगता है। इस प्रकार, ज्ञान की आँधी भक्त के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। वह एक साधारण मनुष्य से एक संत बन जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की यह आँधी उसे एक नया जीवन प्रदान करती है, जहां वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है।
NCERT Solutions for Class 9 Hindi Chapter 7
13. भाव स्पष्ट कीजिए-
(क) हिति चित्त की द्वै यूँनी गिराँनी, मोह बलिंडा तूटा |
(ख) आँधी पीछै जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भींनाँ ।
उत्तर :
(क) हिति चित्त की द्वै यूँनी गिराँनी, मोह बलिंडा तूटा
- अर्थ: इस पंक्ति का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति होने पर मनुष्य के हृदय में जो द्वैत भाव यानी दोहरी भावनाएँ होती हैं, जैसे कि प्रेम और द्वेष, सुख और दुःख, वो ध्वस्त हो जाती हैं। मोह का बंधन टूट जाता है।
- भाव: जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। वह द्वैत भाव से ऊपर उठ जाता है और उसे केवल एक ही सत्य दिखाई देता है। मोह के बंधन टूटने का अर्थ है कि व्यक्ति अब संसार के भौतिक सुखों से लगाव नहीं रखता है।
(ख) आँधी पीछै जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भींनाँ
- अर्थ: इस पंक्ति का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य के हृदय में प्रेम की वर्षा होती है। वह ईश्वर के प्रति प्रेम से भर जाता है।
- भाव: यह पंक्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति में आने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। ज्ञान की आँधी के बाद मन शांत हो जाता है और प्रेम की वर्षा होती है। व्यक्ति अब ईश्वर के प्रति प्रेम से ओत-प्रोत हो जाता है।
NCERT Solutions for Class 9 Hindi Chapter 7
रचना और अभिव्यक्ति
14. संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए ।
उत्तर :
कबीर दास एक महान संत और कवि थे जिन्होंने धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रबल संदेश दिया। उन्होंने जाति-पाति, धर्म-मजहब के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। कबीर दास ने सभी मनुष्यों को एक समान माना और सभी में ईश्वर का वास देखा। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म हृदय में होता है, न कि मंदिरों और मस्जिदों में। उन्होंने बाहरी रीति-रिवाजों और दिखावों के बजाय आंतरिक शुद्धि और सच्चे हृदय से की जाने वाली भक्ति को महत्व दिया।
कबीर दास ने सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखा। उन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया और समाज सेवा को धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग माना।
15. निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए-
पखापखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग, निरपख
उत्तर :
- पखापखी: पक्ष-विपक्ष
- अनत: अन्यत्र
- जोग: योग
- जुगति: युक्ति
- बैराग: वैराग्य
- निरपख: निष्पक्ष
NCERT Solutions for Class 9 Hindi Chapter 7
FAQ’s
Class 9 Hindi Chapter 7 “साखियाँ” के रचयिता कौन हैं?
Class 9 Hindi Chapter 7 “साखियाँ” के रचयिता संत कबीर हैं, जो एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे।
“साखियाँ” पाठ का मुख्य संदेश क्या है?
साखियाँ class 9 पाठ में जीवन के नैतिक मूल्यों, सत्य, साधुता और आत्मज्ञान पर बल दिया गया है। कबीर के दोहे हमें सरल भाषा में गहरी सीख देते हैं।
Class 9 Hindi Chapter 7 “साखियाँ” में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है?
इस पाठ में कबीर की साखियाँ सधुक्कड़ी भाषा में लिखी गई हैं, जो ब्रज और अवधी का मिश्रण है और सीधे हृदय में उतरती हैं।
NCERT Solutions for Class 9 Hindi Chapter 7 कैसे सहायक हैं?
यह समाधान छात्रों को साखियाँ class 9 की व्याख्या समझने, कठिन शब्दों के अर्थ जानने और प्रश्नों के उत्तर प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद करते हैं।
“साखियाँ” पाठ छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
Class 9 Hindi Chapter 7 विद्यार्थियों को नैतिकता, आत्मचिंतन और संत कबीर की शिक्षाओं से जुड़ने का अवसर देता है, जो उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक है।