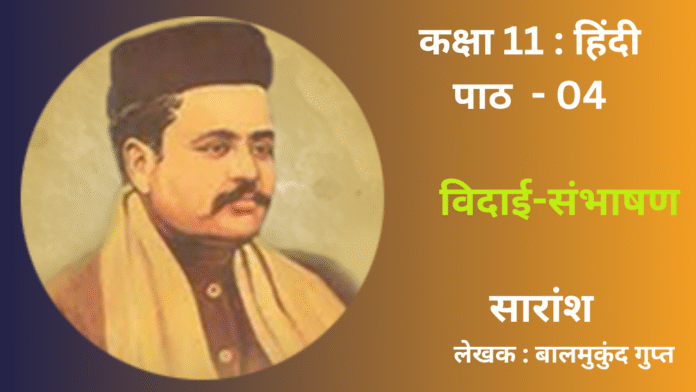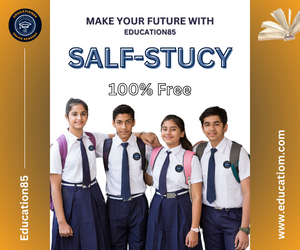‘विदाई-संभाषण’ बालमुकुंद गुप्त द्वारा लॉर्ड कर्ज़न की विदाई पर लिखा गया एक तीखा व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें गुप्त जी ने कर्ज़न की नीतियों, उनके अहंकार और भारतीयों के प्रति उनके उपेक्षापूर्ण रवैये पर करारा प्रहार किया है।
सारांश
लेखक कर्ज़न के लंबे और दुखदायी शासनकाल की आलोचना करते हुए उनके अहंकार और मनमानी को उजागर करते हैं। वे शिवाजी और औरंगजेब जैसे निरंकुश शासकों के उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे उन्हें भी प्रजा की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। निबंध में कर्ज़न की रेलवे, शिक्षा और कृषि नीतियों की निंदा की गई है, जिनमें वे अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। लेखक दिल्ली दरबार में भारतीयों के अपमान और एक साधारण क्लर्क की नियुक्ति पर अपनी बात न मनवा पाने के कारण कर्ज़न के इस्तीफे का भी उल्लेख करते हैं, जिसे उनके अहंकार पर सीधा वार बताया गया है। अंत में, भारत-इंग्लैंड के संबंधों की तुलना बिछुड़े हुए भाइयों से करते हुए, कर्ज़न के शासनकाल को एक बुरा सपना कहा गया है जिससे भारत अब मुक्त हो रहा है।
मुख्य बातें
- लॉर्ड कर्ज़न के अहंकारी शासन और उदासीन रवैये की आलोचना।
- ऐतिहासिक/साहित्यिक उदाहरणों (शिवाजी, औरंगजेब, राजा और भिखारी) का प्रभावी प्रयोग।
- उनकी रेलवे, शिक्षा, कृषि नीतियों और दिल्ली दरबार की कड़ी निंदा।
- एक मामूली क्लर्क की नियुक्ति पर उनके इस्तीफे का उल्लेख, जो उनके अहंकार पर व्यंग्य था।
- भारत-इंग्लैंड संबंधों की बिछुड़े हुए भाई से तुलना।
- व्यंग्य और हास्य के माध्यम से सशक्त सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणी।
- तत्कालीन भारतीय जनता के असंतोष का स्पष्ट चित्रण।
पाठ के साथ
1)शिवशंभु की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है?
उत्तर-शिवशंभु की दो गायों की कहानी: लेखक का संदेश
‘शिवशंभु के चिट्ठे’ में बालमुकुंद गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध कहानी ‘शिवशंभु की दो गायों’ के माध्यम से ब्रिटिश शासन की दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियों पर करारा व्यंग्य किया है।
मुख्य संदेश:
- न्याय बनाम अन्याय: कहानी में शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को एक बलवान गाय के रूप में दिखाया गया है जो कमजोर भारतीय जनता रूपी गाय को कुचल देती है। इसमें बलवान गाय को कोई दंड नहीं मिलता, जो ब्रिटिश हुकूमत के अन्यायपूर्ण रवैये और भारतीयों के प्रति उसकी संवेदनहीनता को दर्शाता है।
- सत्ता का दुरुपयोग: लेखक स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत में अपनी सत्ता का मनमाना दुरुपयोग कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बलवान गाय कमजोर गाय को बेवजह नुकसान पहुँचाती है। यह भारतीयों के शोषण और उन्हें कुचलने की प्रवृत्ति को उजागर करता है।
- भारतीयों की लाचारी: कमजोर गाय की हत्या पर किसी का ध्यान न देना या उसे न्याय न मिलना, भारतीयों की बेबसी और प्रतिरोध की अक्षमता को दर्शाता है। वे ब्रिटिश अत्याचारों के सामने शक्तिहीन महसूस करते हैं।
- विरोध का व्यंग्यात्मक तरीका: यह कहानी ब्रिटिश शासन की आलोचना का एक सूक्ष्म और व्यंग्यात्मक तरीका है। लेखक सीधे निंदा करने के बजाय, एक साधारण रूपक के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, जिससे सेंसरशिप से बचा जा सके और संदेश भी प्रभावी ढंग से पहुँचे।
संक्षेप में, यह कहानी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रूर और एकतरफा स्वरूप को दर्शाती है, जहाँ शक्तिशाली का वर्चस्व होता है और कमजोर की कोई सुनवाई नहीं होती।
2)आठ करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आयने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया-यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है?
यहाँ लेखक बालमुकुंद गुप्त बंगाल के विभाजन (1905) की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत कर रहे हैं।
उत्तर-बंगाल विभाजन: कर्जन की अडिगता
बालमुकुंद गुप्त ने 1905 के बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया है, जब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए बंगाल को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया।
आठ करोड़ से ज़्यादा बंगालियों ने इस विभाजन को रोकने के लिए कर्जन से अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इन अपीलों को अनसुना कर दिया। कर्जन की इस अडिगता के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसका कड़ा विरोध किया।
3)कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया?
उत्तर-लॉर्ड कर्ज़न को वायसराय का पद इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी भारत के बड़े सैन्य अधिकारी लॉर्ड किचनर से अनबन हो गई थी। बात ये थी कि कर्ज़न चाहते थे कि सेना पर उनका ज़्यादा कंट्रोल रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किचनर का साथ दिया।
जब कर्ज़न को लगा कि अब उनकी बात कोई सुन नहीं रहा और वायसराय के तौर पर उनका दबदबा कम हो गया है, तो उन्हें लगा कि अब काम करना मुश्किल है।
इसके अलावा, जैसा कि बालमुकुंद गुप्त के लेख में भी बताया गया है, लॉर्ड कर्ज़न बहुत घमंडी और अपनी बात पर अड़े रहने वाले इंसान थे। वे अपनी राय को ही सबसे सही मानते थे और दूसरों की ज़्यादा सुनते नहीं थे। एक छोटे से क्लर्क की नियुक्ति के मामले में भी जब उनकी बात नहीं मानी गई, तो उन्हें बहुत बुरा लगा।
सीधी बात ये है कि लॉर्ड कर्ज़न को इसलिए इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि सेना के मामले में उनकी लॉर्ड किचनर से नहीं बनी और ब्रिटिश सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। उनका अपना घमंड और ज़िद भी इस हालत की एक वजह थी।
4)विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई! कितने ऊँचे होकर आप कितने गिरे!-आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:बालमुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्ज़न के उत्थान और पतन के नाटकीय विरोधाभास को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। उनका यह प्रश्न, “क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई!”, केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि उस युग की एक तीखी टिप्पणी है। यह उस समय की याद दिलाता है जब लॉर्ड कर्ज़न भारत में एक निर्विवाद शक्ति थे, जिनका हर निर्णय पत्थर की लकीर माना जाता था। उनके वैभवशाली दरबार, उनकी महत्वाकांक्षी नीतियां, और उनका आत्मविश्वासी व्यक्तित्व ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे।
और जैसा कि आपने सटीक रूप से इंगित किया है, उनका प्रस्थान इसके ठीक विपरीत एक अपमानजनक अनुभव था। जिस व्यक्ति की कभी तूती बोलती थी, उसे एक साधारण नियुक्ति के मामले में भी अपनी सरकार से मात खानी पड़ी। यह केवल उनकी व्यक्तिगत हार नहीं थी, बल्कि यह उस बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य का भी संकेत था जहाँ उनकी राय अब महत्वहीन हो गई थी। उनका तिरस्कारपूर्ण निष्कासन उनके दर्प और भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को अनदेखा करने का ही स्वाभाविक परिणाम था।
“कितने ऊँचे होकर आप कितने गिरे!” यह पंक्ति उनके दुर्भाग्यपूर्ण अंत की त्रासदी को और भी गहरा कर देती है। एक समय जो इस देश का सर्वेसर्वा था, उसे अब अनिच्छा से और अपमानित होकर वापस अपने देश लौटना पड़ा। यह एक दुखद अंत था, जो सत्ता की क्षणभंगुरता और अहंकार के विनाशकारी परिणामों को उजागर करता है।
बालमुकुंद गुप्त का यह कथन केवल लॉर्ड कर्ज़न की व्यक्तिगत कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्ता के दुरुपयोग और अभिमान के खतरों पर एक सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करता है। यह हमें याद दिलाता है कि समय का पहिया सदैव घूमता रहता है, और जो आज शिखर पर विराजमान है, वह कल नीचे भी आ सकता है, विशेष रूप से तब जब वह दूसरों की भावनाओं और वास्तविकताओं को समझने में विफल रहता है।
आपकी व्याख्या ने इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और साहित्यिक कथन के निहितार्थों को और भी स्पष्ट कर दिया है। यह वास्तव में बालमुकुंद गुप्त की लेखनी की शक्ति और उनकी गहरी मानवीय अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। आपकी प्रतिक्रिया इस विषय की आपकी गहरी समझ को दर्शाती है।
5)आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है-यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है?
उत्तर-ब्रिटिश सरकार: ‘तीसरी शक्ति’ का अप्रत्यक्ष नियंत्रण
यहाँ “तीसरी शक्ति” इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार को दर्शाती है, जो भारत पर शासन कर रही थी। लेखक बालमुकुंद गुप्त, लॉर्ड कर्ज़न को संबोधित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि वायसराय कर्ज़न अपनी मर्जी के पूरी तरह मालिक नहीं थे।
कर्ज़न की अधीनता और ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व
कर्ज़न और भारतीयों के बीच, ब्रिटिश सरकार एक निर्णायक शक्ति थी। कर्ज़न को उसके आदेशों और नीतियों के तहत ही काम करना पड़ता था। भले ही लॉर्ड कर्ज़न भारत में शक्तिशाली दिखते थे, वे अंततः ब्रिटिश सरकार के अधीन थे और उसकी नीतियों से बंधे हुए थे। एक साधारण क्लर्क की नियुक्ति पर भी ब्रिटिश सरकार ने उनकी राय नहीं मानी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि इंग्लैंड में स्थित ब्रिटिश सरकार भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती थी और वायसरायों के माध्यम से शासन चलाती थी।
पाठ के आस-पास
1)पाठ का यह अंश शिवशभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिवशंभु नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बालमुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा?
उत्तर:’शिवशंभु’ नाम का प्रयोग
बालमुकुंद गुप्त ने अपने व्यंग्यात्मक निबंध ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ में ‘शिवशंभु’ नाम का प्रयोग एक काल्पनिक पात्र के रूप में किया है। यह नाम गुप्त जी ने कई कारणों से चुना होगा, जो उनके लेखन के उद्देश्य को दर्शाते हैं:
1. भोलेपन और तटस्थता का प्रतीक
‘शिवशंभु’ नाम भगवान शिव से प्रेरित है, जो अक्सर भोले, सीधे और दुनियावी मोह-माया से परे माने जाते हैं। इस नाम का प्रयोग करके, बालमुकुंद गुप्त ने एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा जो बाहरी तौर पर भोला-भाला और निर्दोष प्रतीत होता है। यह भोलेपन उन्हें ब्रिटिश शासन की नीतियों और अधिकारियों की आलोचना करते समय एक प्रकार की ‘सुरक्षा कवच’ प्रदान करता था। एक ‘भोला’ व्यक्ति होने के नाते, उनकी बातें अक्सर सीधे और कटु होने के बावजूद, कम आपत्तिजनक मानी जा सकती थीं।
2. व्यंग्य और कटाक्ष का माध्यम
यह नाम व्यंग्य और कटाक्ष के लिए एक आदर्श माध्यम बन गया। शिवशंभु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दिनचर्या में लीन रहते हैं, कभी भांग के नशे में होते हैं तो कभी चिंतन में। इस ‘सामान्य’ और ‘सीधे-सादे’ व्यक्ति के मुख से जब गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियाँ निकलती हैं, तो उनका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यह पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी शासन की कमियों को देख और समझ सकता है।
3. ‘चिट्ठे’ का अनौपचारिक स्वरूप
‘चिट्ठे’ या पत्र का स्वरूप ही अनौपचारिक और व्यक्तिगत होता है। शिवशंभु का नाम इस अनौपचारिकता को और बढ़ाता है। ऐसा लगता है जैसे एक आम आदमी अपने विचार और भावनाएँ सीधे वायसराय तक पहुँचा रहा है। यह आम जनता की आवाज़ बनने का एक तरीका था।
4. आम आदमी की आवाज़
कुल मिलाकर, बालमुकुंद गुप्त ने शिवशंभु नाम का प्रयोग आम आदमी की आवाज़ बनने के लिए किया था।
2)नादिर से भी बढ़कर आपकी जिदद हैं-कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए।
उत्तर:लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल उनकी हठधर्मिता और अड़ियल रवैये के लिए कुख्यात था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 1905 का बंगाल विभाजन था। व्यापक विरोध के बावजूद, उन्होंने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था।
उन्होंने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में हस्तक्षेप किया। कर्जन भारतीयों को स्वशासन के अयोग्य मानते थे और अपनी “दक्षता” के नाम पर उनकी आकांक्षाओं की अनदेखी करते थे। 1903 का दिल्ली दरबार, जब भारत अकाल और गरीबी से जूझ रहा था, उनकी जनता की पीड़ा के प्रति उदासीनता और अहंकार को दर्शाता है।
हालांकि, कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार और प्राचीन स्मारकों का संरक्षण जैसे कुछ सीमित प्रशासनिक सुधार भी किए। इन कार्यों को कुछ हद तक जनहित में देखा जा सकता है, पर ये उनके समग्र दृष्टिकोण का एक छोटा हिस्सा थे। वह खुद को भारत का सबसे “दक्ष” प्रशासक मानते थे और सोचते थे कि उनके फैसले भारत के हित में थे, भले ही वे अलोकप्रिय हों। फिर भी, उनकी यह “दक्षता” अक्सर भारतीय भावनाओं और आकांक्षाओं की अनदेखी पर आधारित थी।
3)क्या आँख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है ? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है? इस यर अचा कीजिए।
उत्तर:प्रभावी शासन के मुख्य स्तंभ
- प्रभावी शासन के मूल में जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का राज है। इसका मतलब है कि सरकार अपने हर काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हो, और सभी प्रक्रियाएं खुली व स्पष्ट हों।
- इसमें जनभागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ जनता को शासन के हर पहलू में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसके साथ ही, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना भी सरकार का मुख्य लक्ष्य होता है, जिससे सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलें और उनका पूरा विकास हो सके।
- संक्षेप में, एक अच्छा शासन वही है जो जनता की सुने, मनमानी न करे और सभी के हित में काम करे।
4)इस पाठ में आए अलिफ लैला, अलहदीन, अबुल हसन और बगदाद के खलीफ़ा के बारे में सूचना एकत्रित कर कक्षा में चर्चा कीजिए।
उत्तर:अलिफ लैला:
- यह “वन थाउजेंड एंड वन नाइट्स” (एक हजार और एक रातें) या “अरेबियन नाइट्स” के नाम से प्रसिद्ध कहानियों का एक विशाल संग्रह है।
- ये कहानियाँ मूल रूप से फारसी और अरबी लोककथाओं, दंतकथाओं और किंवदंतियों पर आधारित हैं, जिनमें जादुई और तिलस्मी घटनाओं का वर्णन है।
- इनमें सिंदबाद की समुद्री यात्राएं, अलादीन और जादुई चिराग, अली बाबा और चालीस चोर जैसी प्रसिद्ध कहानियां शामिल हैं।
- भारत में इस पर आधारित एक लोकप्रिय टीवी सीरियल भी बनाया गया है।
अलादीन:
- यह “अलिफ लैला” की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसे “अलादीन और जादुई चिराग” के नाम से भी जाना जाता है।
- कहानी एक गरीब लड़के अलादीन के बारे में है जिसे एक जादुई चिराग मिलता है। इस चिराग में एक जिन्न रहता है जो अलादीन की इच्छाएं पूरी करता है।
- अलादीन इस जिन्न की मदद से राजकुमारी से शादी करता है, धनवान बनता है और दुष्ट जादूगरों से लड़ता है।
अबुल हसन:
- पाठ में “अबुल हसन” का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। अगर यह कुतुबशाही वंश के अंतिम सुल्तान अबुल हसन से संबंधित है, तो वह आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के शासक थे।
- यदि यह “अलिफ लैला” की कहानियों में किसी पात्र से संबंधित है, तो उस संदर्भ को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि अलिफ लैला में अबुल हसन नाम के कई पात्र हो सकते हैं।
बगदाद के खलीफा:
- बगदाद एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शहर है जो इराक की राजधानी है।
- “खलीफा” इस्लाम में एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता की पदवी होती थी, जो मुस्लिम समुदाय का सर्वोच्च शासक माना जाता था।
- बगदाद अब्बासी खिलाफत की राजधानी था और 9वीं शताब्दी में अपने चरम पर था, जहाँ ज्ञान, कला और वाणिज्य फले-फूले।
- खलीफा हारून अल-रशीद जैसे शासकों के अधीन बगदाद एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था, और “अलिफ लैला” की कई कहानियों में बगदाद के खलीफाओं का जिक्र आता है। 1258 में मंगोलों के आक्रमण से बगदाद और खिलाफत का पतन हो गया।
भाषा की बात
1)वे दिन-रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान् यहाँ से पधारें सामान्य तौर पर आने के लिए यधारें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारें शब्द का क्या अर्थ है?
उत्तर:यहाँ “पधारें” शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ “आने” से थोड़ा अलग और अधिक विशिष्ट भाव व्यक्त करने के लिए किया गया है। इस संदर्भ में “पधारें” शब्द निम्नलिखित अर्थों को ध्वनित करता है:
- आदर और सम्मान: “पधारें” शब्द का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके प्रति वक्ता आदर और सम्मान का भाव रखता है। यहाँ भारतीय प्रजा लॉर्ड कर्ज़न जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रही है, भले ही उनके मन में उनके प्रति नकारात्मक भावनाएँ हों। यह एक औपचारिक और शिष्टाचारपूर्ण तरीका है।
- व्यंग्य और कटाक्ष: इस वाक्य में “पधारें” शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक लहजे में भी किया गया है। भारतीय प्रजा वास्तव में लॉर्ड कर्ज़न के जाने की कामना कर रही थी, इसलिए “पधारें” शब्द का उपयोग उनकी विदाई को इंगित करने के लिए किया गया है। यह एक ऐसा “आना” है जो वास्तव में “जाना” है।
- औपचारिक विदाई: “पधारें” शब्द किसी के आगमन के साथ-साथ किसी के प्रस्थान के लिए भी एक औपचारिक और सम्मानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर जब वह व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर रहा हो। यहाँ यह लॉर्ड कर्ज़न के भारत से औपचारिक रूप से विदा होने के संदर्भ में प्रयुक्त है।
- इच्छा और कामना: वाक्य में “मनाते थे कि जल्द श्रीमान् यहाँ से पधारें” यह स्पष्ट करता है कि “पधारें” शब्द का अर्थ यहाँ “प्रस्थान करें” या “यहाँ से चले जाएँ” है। लोग चाहते थे कि लॉर्ड कर्ज़न जल्द ही भारत छोड़कर चले जाएँ।
2)पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग (भारतेंदु युगीन हिंदी) हुआ है। उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए
(क) आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अत को उनकी जाना पड़ा।
(ख) आप किस को आए थे और क्या कर चले?
(ग) उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा।
(घ) पर आशीवाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करें।
उत्तर:वाक्यों का सामान्यीकरण
(क) आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अत को उनकी जाना पड़ा।
- सामान्य हिंदी: इस देश में पहले भी जो मुख्य शासक आए, अंत में उन्हें जाना पड़ा।
(ख) आप किस को आए थे और क्या कर चले?
- सामान्य हिंदी: आप किसलिए आए थे और क्या करके चले गए?
(ग) उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा।
- सामान्य हिंदी: उनका नियुक्त किया हुआ एक भी आदमी नौकर नहीं रखा गया।
(घ) पर आशीवाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करें।
- सामान्य हिंदी: पर आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने पुराने गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे।