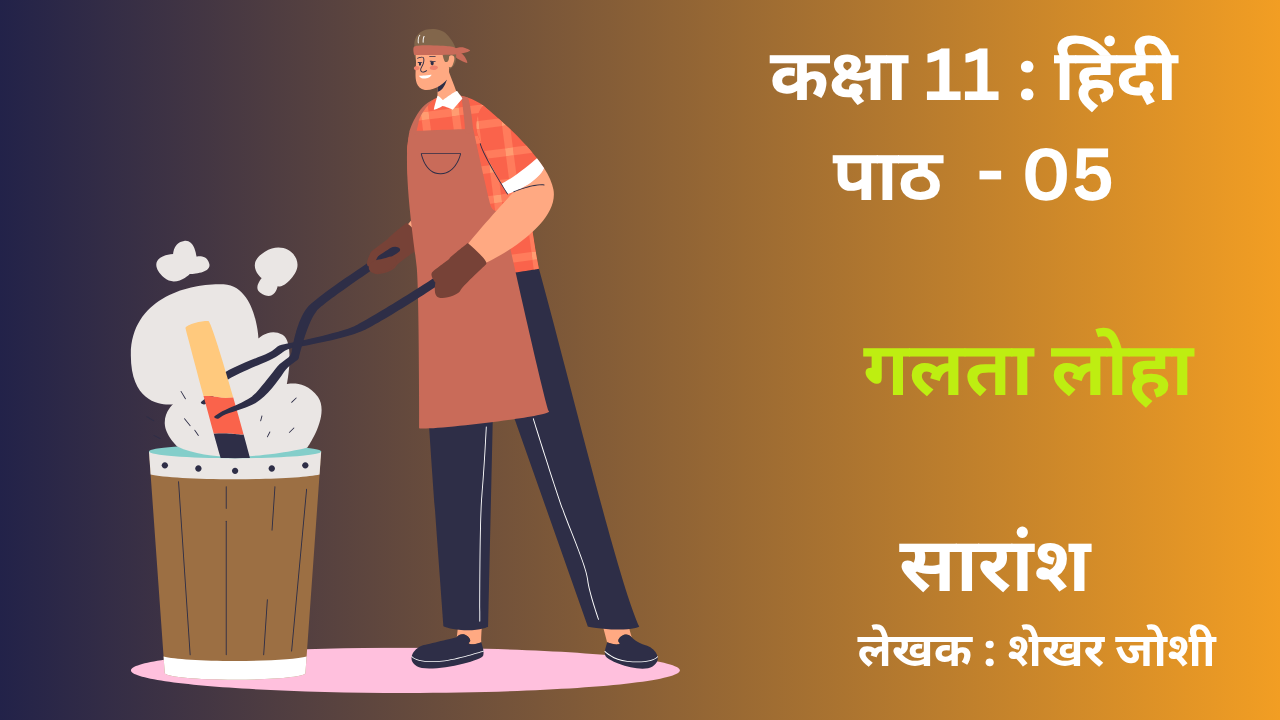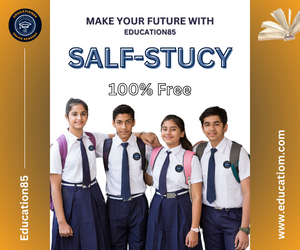मोहन की विवशता और जाति के बंधन की कटु सच्चाई :-
आपने बिल्कुल सही कहा कि मोहन का शिक्षा से वंचित रहना और योग्यता होने के बावजूद अवसर न मिलना उस समय की सामाजिक व्यवस्था का एक दुखद पहलू था। यह केवल मोहन की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह उस पूरे वर्ग की कहानी थी जिसे जन्म के आधार पर शिक्षा और सम्मानजनक पेशे से दूर रखा गया। धनराम के पास उसका जाना केवल पेट भरने की मजबूरी नहीं थी, बल्कि यह उस सामाजिक विभाजन पर भी एक तीखा सवाल उठाता है जो काम को जाति के आधार पर छोटा या बड़ा मानता है।
एक ब्राह्मण का लोहार का काम करना उस सदियों से चली आ रही व्यवस्था को अंदर तक हिला देता है। यह दिखाता है कि कैसे आर्थिक मजबूरियाँ और सामाजिक अन्याय व्यक्ति को ऐसे रास्ते चुनने पर विवश करते हैं जो उसकी पारंपरिक जातिगत पहचान से मेल नहीं खाते। मोहन का यह कदम, भले ही उसकी व्यक्तिगत विवशता से जन्मा हो, पर एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन का संकेत देता है।
लोहे की छड़ का मुड़ना: हुनर और चुनौती का प्रतीक:-
लोहे की छड़ मोड़ने का दृश्य केवल मोहन की शारीरिक ताकत को ही नहीं दर्शाता, बल्कि उसकी समझदारी और काम करने के तरीके को भी सामने लाता है। यह उस संकुचित सोच को चुनौती देता है जो शारीरिक श्रम को कुछ खास जातियों तक ही सीमित मानती है। यह दृश्य स्पष्ट करता है कि प्रतिभा और क्षमता किसी एक जाति की बपौती नहीं होती। मोहन का यह कृत्य उस दकियानूसी विचार पर एक मूक प्रहार है कि ब्राह्मण सिर्फ बौद्धिक कार्य के लिए बने हैं और शारीरिक श्रम उनके लिए वर्जित है। यह दर्शाता है कि कौशल और हुनर किसी भी जाति के दायरे में सीमित नहीं रखे जा सकते, बल्कि वे व्यक्तिगत लगन और समझदारी का परिणाम होते हैं।
‘गलता लोहा’ और सामाजिक बदलाव की उम्मीद :-
मोहन का लोहार का काम अपनाना उस पुरानी व्यवस्था के खिलाफ एक शांत, लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध है। यह एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है जो बिना किसी शोर-शराबे के, व्यक्तिगत स्तर पर घटित हो रही है।
यह कहानी हमें उस बीते हुए समय के कठोर जातिवाद की याद दिलाती है, जो दुर्भाग्य से आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही, यह कहानी बदलाव की एक उम्मीद भी जगाती है, एक ऐसे भविष्य का सपना दिखाती है जहाँ हर व्यक्ति को उसकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार सम्मान मिले, न कि उसकी जाति के नाम पर। शेखर जोशी ने “गलता लोहा” के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिया है – हुनर किसी भी बंधन में बंधकर नहीं रहता और एक न्यायपूर्ण समाज वही है जहाँ हर किसी को अपनी क्षमता दिखाने का समान अवसर मिले।
आपकी गहरी और संवेदनशील व्याख्या ने इस कहानी के छिपे हुए अर्थ और उसके आवश्यक संदेश को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे बदलाव अक्सर व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होते हैं और धीरे-धीरे पूरे समाज को प्रभावित करते हैं।
पाठ के साथ
1)कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें, जिसमें किताबों की विदया और घन चलाने की विद्या का ज़िक्र आया है।
उत्तर:कहानी में एक पात्र ने नायक को बखूबी समझाया कि किताबी ज्ञान हमें सिर्फ सिद्धांतों से परिचित कराता है, पर असली विद्या तो “घन चलाने” यानी हाथों-हाथ अनुभव से आती है। यह बात जीवन में व्यावहारिक ज्ञान के अतुल्य महत्व को दर्शाती है। किताबें हमें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन उस पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुँचना, वास्तविक अनुभव से ही संभव होता है।
2)धनराम मोहन को अपना प्रतिदवंदवी क्यों नहीं समझता था?
उत्तर: धनराम मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था. उसे पता था कि मोहन उससे ऊँची जाति का है और पढ़ाई में भी बहुत तेज़ है. धनराम मोहन का हमेशा सम्मान करता था और उसे लगता था कि मोहन उससे कहीं बेहतर है. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहन कभी उसके स्तर पर आ पाएगा.
3)धनराम को मोहन के लिए व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों?
उत्तर:धनराम को मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि मोहन ने उसकी दुकान पर बैठकर, बिना किसी हिचकिचाहट के, अपनी लोहार जाति के काम में मदद की। मोहन एक ब्राह्मण जाति का था, और उस समय समाज में जाति-पाति का भेद बहुत गहरा था। ब्राह्मणों का लोहारों के साथ बैठकर काम करना या उनकी सहायता करना सामान्य बात नहीं थी। मोहन का यह व्यवहार, जिसमें उसने जातिगत बाधाओं को पार करके मित्रता और सहयोग दिखाया, धनराम के लिए अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक था।
4)मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है?
उत्तर:मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि इस दौरान उसके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जो उसके पहले के जीवन से बिल्कुल अलग थे। ये बदलाव निम्नलिखित हैं:
- भौगोलिक परिवर्तन: मोहन अपने गाँव की परिचित और सीमित दुनिया से निकलकर एक बड़े शहर, लखनऊ, में आया। यह उसके लिए एक नया और विस्तृत परिवेश था, जहाँ उसे नई चीजें देखने और नए लोगों से मिलने का अवसर मिला।
- शैक्षणिक परिवर्तन: लखनऊ में मोहन का दाखिला एक तकनीकी विद्यालय में हुआ, जहाँ उसे किताबी ज्ञान के साथ-साथ तकनीकी कौशल भी सीखने का मौका मिला। यह उसके गाँव के पारंपरिक स्कूल की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न था।
- सामाजिक परिवर्तन: लखनऊ में मोहन का संपर्क विभिन्न पृष्ठभूमि और विचारों वाले छात्रों से हुआ होगा। शहरी जीवनशैली और सामाजिक मानदंडों का उस पर प्रभाव पड़ा होगा, जो उसके गाँव के सरल जीवन से अलग था।
- व्यक्तिगत विकास: नए माहौल और नई शिक्षा के कारण मोहन के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में बदलाव आया होगा। उसने नए कौशल सीखे होंगे और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया होगा।
- भविष्य की नई दिशा: लखनऊ में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने से मोहन के भविष्य के लिए नई संभावनाएं खुलीं। अब उसके पास गाँव के पारंपरिक व्यवसायों तक ही सीमित रहने की बजाय, तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने का विकल्प भी था।
- अतीत से अलगाव: लखनऊ में रहने के दौरान मोहन अपने गाँव और बचपन के जीवन से दूर हो गया। यह दूरी उसे अपने अतीत को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखने और अपने भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने का अवसर प्रदान करती है।
5)मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने ज़बान के चाबुक कहा है और क्यों?
उत्तर:लेखक ने मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन को “ज़बान के चाबुक” कहा है:
“तुम लोगों को पढ़ाना बैल के सींग में घंटी बाँधने के समान है।”
कारण: यह कथन तीखा और चुभने वाला था, जो छात्रों की मंद बुद्धि पर करारा प्रहार करता था। इसमें व्यंग्य और आलोचना का पैनापन था, जो चाबुक की तरह दर्द देता था।
6)
( 1 ) बिरादरी का यही सहारा होता है।
(क) किसने किससे कहा?
(ख) किस प्रसंग मं कहा?
(ग) किस आशय से कहा?
(घ) क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है?
उत्तर:(क) यह वाक्य कहानी में किसी बिरादरी के सदस्य ने दूसरे सदस्य से कहा होगा।
(ख) यह संभवतः किसी मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देने या सहारा बनने के प्रसंग में कहा गया होगा।
(ग) इसका आशय यह है कि बिरादरी के लोग ही मुसीबत में एक-दूसरे की मदद करते हैं।
(घ) हाँ, कहानी में यह आशय स्पष्ट होता है कि बिरादरी का सहारा ही महत्वपूर्ण होता है।
(2) उसकी अखिों में एक सजक की चमक थी-कहानी का यह वाक्य-
(क) किसके लिए कहा गया हैं?
(ख) किस प्रसग में कहा गया हैं?
(ग) यह पात्र-विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है?
उत्तर:(क) यह वाक्य मुख्य पात्र (नायक/नायिका) के लिए कहा गया है, जिसकी आँखों में सपनों या आशाओं की चमक दिखाई देती है।
(ख) यह किसी महत्वपूर्ण या प्रेरणादायक पल के संदर्भ में कहा गया है, जब पात्र किसी लक्ष्य, सच्चाई या भावना से जुड़ा होता है।
(ग) यह पात्र के आशावाद, संवेदनशीलता, दृढ़ संकल्प और स्वप्नदर्शी पहलुओं को उजागर करता है।
पाठ के आस-पास
1)गाँव और शहर, दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन-संघर्ष में क्या फ़र्क है? चर्चा करें और लिखें।
उत्तर: मोहन: ग्रामीण और शहरी जीवन का संगम
मोहन का जीवन गाँव के सहयोग और सादगी से शहर की प्रतिस्पर्धा और एकाकीपन की ओर मुड़ गया। जहाँ गाँव में शारीरिक श्रम और मिलजुलकर काम करना था, वहीं शहर में मानसिक तनाव और कड़ी दौड़ का सामना हुआ। गाँव में साधनों की कमी थी, पर लोग साथ थे; शहर में अवसर थे, पर हर कोई अपनी धुन में खोया था। मोहन ने इन दोनों ही अलग-अलग दुनियाओं में खुद को अनुकूल बनाया।
2)एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकीखूबियों और खामियों पर विचार करें।
उत्तर:त्रिलोक सिंह एक आदर्श अध्यापक की छवि प्रस्तुत करते हैं। उनका व्यक्तित्व समर्पित, अनुशासित और छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है।
खूबियाँ:
वह छात्रों को समझने का प्रयास करते हैं और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनते हैं।
पढ़ाने का तरीका रोचक और प्रभावी है, जिससे विषय सरल लगता है।
अनुशासन पर जोर देते हैं, लेकिन सख्ती के साथ न्यायसंगत भी हैं।
खामियाँ:
कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासन पर बल देने से छात्र डर सा जाते हैं।
नए शिक्षण तरीकों को अपनाने में थोड़ा संकोच करते हैं।
3)गलत लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चचा करें?
उत्तर:’गलत लोहा’ कहानी का वर्तमान अंत, जहाँ मोहन धनराम का प्रस्ताव स्वीकार करता है, जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़कर मानवीय संबंधों की जीत का प्रतीक है। राजेंद्र यादव ने इस अंत के माध्यम से सामाजिक बदलाव और आपसी सौहार्द को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, जो इसे कहानी के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। यह मानवीय मूल्यों की विजय और सामाजिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
भाषा की बात
1)पाठ में निम्नलिखित शब्द लौहकर्म से सबंधित हैं। किसका क्या प्रयोजन हैं? शब्द के सामने लिखिए
(क) धोकनी …………………………………….
(ख) दराँती …………………………………….
(ग) सड़सी …………………………………….
(घ) आफर …………………………………….
(ङ) हथौड़ा …………………………………….
उत्तर: धोकनी: यह आग को तेज़ करने के लिए हवा देने वाला उपकरण है, जिसका उपयोग भट्टी की आग को सुलगाने और धधकाने के लिए किया जाता है।
दराँती: यह फसल काटने या घास छीलने का एक मुड़ा हुआ और धारदार औजार है।
सड़सी: यह गर्म धातु को पकड़ने वाला चिमटा जैसा औजार है, जिससे उसे सुरक्षित रूप से हटाया या हेरफेर किया जा सके।
आफर: यह लोहे को गरम करने वाली भट्टी या अंगारे रखने की जगह होती है, जहाँ धातु को पिघलाने या नरम करने के लिए गरम किया जाता है।
हथौड़ा: यह किसी चीज़ को ठोकने, पीटने या तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। लोहार इसका उपयोग धातु को आकार देने के लिए करते हैं।
2)पाठ में ‘काट-छाँटकर’ जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई पाँच शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
उत्तर:पाठ “गलता लोहा” में प्रयुक्त पाँच संयुक्त क्रिया शब्द और उनके वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं:
- झुँझलाकर – (झुँझलाना + कर) – अध्यापक ने शोर मचाते बच्चों को झुँझलाकर डाँटा।
- बैठ गया – (बैठना + गया) – थक हारकर वह पेड़ की छाँव में बैठ गया।
- देख रहा था – (देखना + रहा था) – धनराम आश्चर्य से मोहन की ओर देख रहा था।
- मारना शुरू किया – (मारना + शुरू किया) – मोहन ने लोहे की छड़ पर हथौड़े से चोटें मारना शुरू किया।
- बना लेता था – (बनाना + लेता था) – धनराम हर तरह के औजार बड़ी कुशलता से बना लेता था।
3)‘बूते का’ प्रयोग पाठ में तीन स्थानों पर हुआ है उन्हें छाँटकर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है, उन संदर्भों में उन्हें स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:पाठ में ‘बूते का’ का प्रयोग तीन स्थानों पर हुआ है, जो सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाता है:
- “यह मेरे बूते का नहीं।”: इस संदर्भ में, ‘बूते का’ का अर्थ है किसी कार्य को करने की क्षमता या सामर्थ्य। मोहन यह स्वीकार करता है कि अमुक कार्य उसकी शक्ति से परे है।
- “उसके बूते का काम होता।”: यहाँ ‘बूते का’ से तात्पर्य है ऐसा काम जो व्यक्ति की योग्यताओं और कौशल के अनुकूल हो। यदि काम उसकी क्षमता के भीतर होता तो वह उसे आसानी से कर पाता।
- “अब यह उसके बूते से बाहर था।”: इस प्रयोग में ‘बूते का’ का अर्थ है किसी स्थिति या समस्या को संभालने या नियंत्रित करने की क्षमता। जब स्थिति उसके वश से बाहर हो जाती है, तो यह दर्शाता है कि वह उसे अब और नहीं संभाल सकता।