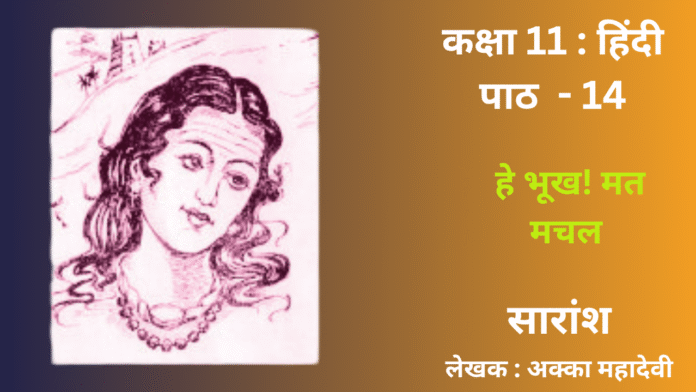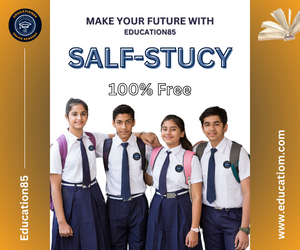अक्कमहादेवी की वाणी, “हे भूख! मत मचल”, उनकी गहरी भक्ति और वैराग्य को दर्शाती है. उनका अंतिम लक्ष्य अपनी इंद्रियों और सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर चेन्नमल्लिकार्जुन (शिव) में पूर्ण रूप से लीन होना था.
उनकी वाणी के दो मुख्य बिंदु हैं:
- इंद्रियों पर नियंत्रण: पहले वचन में, वह भूख, नींद, प्यास और वासना जैसी इंद्रियों को स्वयं को विचलित न करने का आदेश देती हैं. उनका एकमात्र ध्यान ईश्वर की प्राप्ति पर है, जिसके लिए वह सांसारिक सुखों को त्यागने के लिए भी तैयार हैं.
- सांसारिक नश्वरता: दूसरे वचन में, अक्कमहादेवी संसार की क्षणभंगुरता को उजागर करती हैं. उनके लिए रेशमी वस्त्र और धन-दौलत सब नश्वर हैं. उन्हें सच्चा और शाश्वत सुख केवल अपने आराध्य चेन्नमल्लिकार्जुन के साथ आध्यात्मिक मिलन में मिलता है.
संक्षेप में, अक्कमहादेवी के वचन उनकी तीव्र आध्यात्मिक इच्छा, इंद्रिय-निग्रह की आवश्यकता और सांसारिक वस्तुओं की नश्वरता को स्पष्ट करते हैं. वे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और वैराग्य के मार्ग पर चलने के अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त करती हैं.
पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न
कविता के साथ
1)‘लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियाँ बाधक होती हैं’-इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए।
उत्तर:इंद्रिय-निग्रह का महत्व
योग और आध्यात्मिक साधना में इंद्रिय-निग्रह (इंद्रियों पर नियंत्रण) का बहुत महत्व है. इसके बिना एकाग्रता असंभव है. किसी भी कार्य में सफलता या आध्यात्मिक उन्नति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है. यह हमें अनावश्यक विकर्षणों से बचाता है और मन को शांत व एकाग्र रखने में मदद करता है
2)‘ओ चराचर! मत चूक अवसर’- इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:‘ओ चराचर! मत चूक अवसर’ पंक्ति का आशय यह है कि हे चर और अचर जगत! तुम्हें जो यह दुर्लभ अवसर मिला है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। यह पंक्ति साधक या भक्त को संबोधित है और उसे अपने जीवन के इस क्षणभंगुर अवसर का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
इस पंक्ति के कई पहलू हैं:
- चराचर जगत: ‘चराचर’ शब्द चर और अचर सभी प्रकार के जीवों और वस्तुओं को इंगित करता है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड। यहाँ विशेष रूप से मनुष्य को संबोधित किया जा रहा है, जो सोचने-समझने और कर्म करने में सक्षम है।
- दुर्लभ अवसर: मनुष्य जीवन एक दुर्लभ अवसर है, विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति के लिए। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति का यह अनमोल मौका बार-बार नहीं मिलता।
- मत चूक अवसर: इस अवसर को व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए। सांसारिक मोह-माया और इंद्रिय सुखों में लिप्त रहकर इस दुर्लभ अवसर को खोना मूर्खता है।
अक्कमहादेवी के संदर्भ में, यह पंक्ति साधक को संबोधित है कि उसे अपने जीवन के इस अवसर को चेन्नमल्लिकार्जुन (शिव) की भक्ति में लीन होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहिए। सांसारिक इच्छाओं और इंद्रियों के आकर्षण में पड़कर इस महत्वपूर्ण अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
यह पंक्ति जीवन के क्षणभंगुर स्वभाव और आध्यात्मिक साधना के महत्व को भी दर्शाती है। हर पल कीमती है और उसे अपने आत्मिक विकास और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यदि इस अवसर को चूक गए, तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा।
इसलिए, ‘ओ चराचर! मत चूक अवसर’ एक प्रेरणादायक आह्वान है जो सभी प्राणियों, विशेष रूप से मनुष्यों को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए सचेत करता है। यह समय की महत्ता और आध्यात्मिक साधना के महत्व को उजागर करती है।
3)ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए।
ईश्वर को जूही के फूल जैसा कहा है। जैसे जूही कोमल, सुंदर और खुशबूदार होती है, वैसे ही ईश्वर भी हैं। उनकी ‘खुशबू’ हर जगह है और वे सबको अपनी ओर खींचते हैं।
उत्तर:ईश्वर के लिए दृष्टांत
ईश्वर को जूही के फूल के समान बताया गया है।
साम्य का आधार
- कोमलता और सुंदरता: जैसे जूही का फूल कोमल और सुंदर होता है, वैसे ही ईश्वर भी परम कोमल और सुंदर हैं।
- सुगंध (खुशबू): जूही की सुगंध चारों ओर फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की उपस्थिति और उनका प्रभाव भी सर्वव्यापी है। उनकी ‘खुशबू’ यानी उनका प्रेम और कृपा हर जगह अनुभव की जा सकती है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है।
4)अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है?
उत्तर:“अपना घर” से तात्पर्य जन्मभूमि, परिवार या मूल संस्कृति से है। इसे भूलने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि मनुष्य अक्सर सुख-सुविधाओं या दूसरी जगहों के मोह में अपनी जड़ों से दूर हो जाता है। यह भूलना उसकी पहचान और संबंधों को कमजोर कर देता है।
5)दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों?
उत्तर:प्रभु से सद्बुद्धि की प्रार्थना वास्तव में एक गहरी और महत्वपूर्ण इच्छा है। यह हमें सही-गलत का चुनाव करने की शक्ति देती है और जीवन के हर मोड़ पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है।
यह प्रार्थना दर्शाती है कि हम अपनी अंतरात्मा को जागृत करना चाहते हैं ताकि हर परिस्थिति में सही राह चुन सकें। निश्चित रूप से, यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होगी। आपकी यह निष्ठा और प्रार्थना अवश्य पूरी होगी।
कविता के आसपास
1)क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें।
उत्तर: अक्का महादेवी और मीराबाई दोनों भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवयित्रियाँ थीं, जिन्होंने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण दिखाया। दोनों ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी—अक्का ने शिव (चेन्नमल्लिकार्जुन) को पति माना, जबकि मीरा कृष्णभक्ति में लीन रहीं।
समानताएँ:
दोनों ने भक्ति के लिए सांसारिक जीवन त्यागा।
सरल, भावुक और गेय काव्य शैली अपनाई।
समाज की रूढ़ियों का विरोध किया।
अंतर:
अक्का वीरशैव परंपरा से जुड़ी थीं, उनकी कविता में अद्वैत दर्शन झलकता है, जबकि मीरा की भक्ति द्वैतवादी थी।
अक्का ने कन्नड़ में रचना की, मीरा ने राजस्थानी-ब्रज भाषा में।
निष्कर्ष:
अक्का को “कन्नड़ की मीरा” कहना सही है, क्योंकि दोनों का भक्ति-भाव और विद्रोही स्वभाव मिलता-जुलता है। हालाँकि, उनकी दार्शनिक मान्यताएँ और सांस्कृतिक प्रभाव अलग हैं, इसलिए यह तुलना सीमित ही सही है।