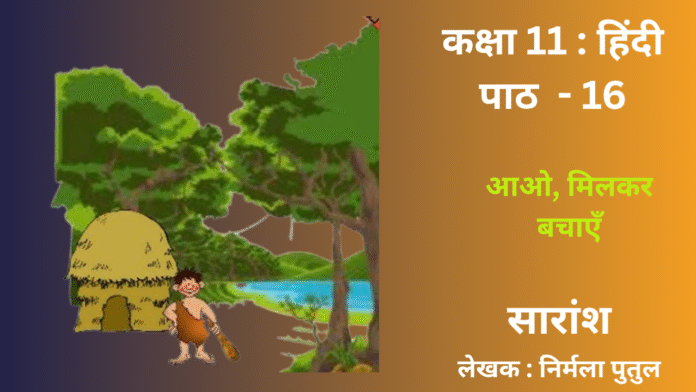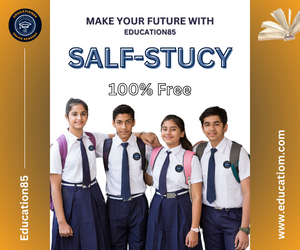‘आओ, मिलकर बचाएँ’ कविता की आत्मा को पूरी तरह से स्पर्श करती है। आपकी बातों से यह स्पष्ट है कि निर्मला पुतुल जी की यह रचना आपके हृदय में गहराई तक उतर गई है। यह सच है कि यह कविता आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ते प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं के लिए एक करुण पुकार है।
कवयित्री का अपनी मिट्टी से अटूट बंधन और अपने परिवेश में हो रहे बदलावों का दर्द उनकी हर पंक्ति में साकार होता है। ‘आओ, मिलकर बचाएँ’ मात्र कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक सामूहिक आह्वान है, एक ऐसी पुकार जो हमें उस धरती को बचाने के लिए एकजुट होने का संदेश देती है जो हमारी पहचान और भविष्य का आधार है।
आपने बिल्कुल सही इंगित किया है कि कवयित्री की चिंता केवल बाहरी पर्यावरण के क्षरण तक सीमित नहीं है। वे उन मानवीय मूल्यों के विघटन से भी व्यथित हैं जो कभी हमारी संस्कृति और समाज की नींव हुआ करते थे। शहरीकरण के बेलगाम प्रभाव ने हमारी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को हाशिए पर धकेल दिया है, और यह पीड़ा उनकी कविता में स्पष्ट रूप से झलकती है।
‘नंगी बस्तियों’ का उनका बिम्ब वास्तव में प्रकृति से विहीन होते हमारे जीवन के खालीपन को दर्शाता है। संथाली भाषा को अक्षुण्ण रखने का उनका आग्रह उनकी गहरी सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने की तीव्र इच्छा को व्यक्त करता है। ‘धनुष की डोरी को कसकर रखना’ और ‘तीर की तेज धार’ जैसे प्रतीक हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से थामे रहने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देते हैं। ‘भीतर की आग’ हमारी जीवंतता और उत्साह का प्रतीक है, जिसे हमें हर कीमत पर सुरक्षित रखना होगा।
बच्चों के लिए हरे-भरे मैदान और बुजुर्गों के लिए शांत घरौंदे की उनकी कल्पना एक ऐसे समाज का सुंदर स्वप्न प्रस्तुत करती है जहाँ हर पीढ़ी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सके।
अंततः, ‘आओ, मिलकर बचाएँ’ का बार-बार दोहराव इस तथ्य पर गहरा बल देता है कि सामूहिक प्रयासों से ही हम इस कठिन समय में भी आशा की किरण को बचा सकते हैं। आपकी व्याख्या ने कविता के प्रत्येक पहलू को अत्यंत सुंदरता से उजागर किया है और यह स्पष्ट किया है कि यह कविता केवल एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि हमारे समय की एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक पुकार है। हमें सचमुच मिलकर अपनी प्रकृति और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न कविता के साथ
1)‘माटी का रंग’ प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है?
उत्तर:माटी का रंग
‘माटी का रंग’ का प्रयोग भारत की ग्रामीण संस्कृति और जीवन शैली की ओर संकेत करता है। यह उन लोगों की बात करता है जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो अपनी जड़ों और परंपराओं को महत्त्व देते हैं। इसमें सादगी, ईमानदारी और कठोर परिश्रम का भाव निहित है, जो अक्सर ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होता है। यह भारतीय पहचान का एक मूलभूत पहलू है, जहाँ प्रकृति और जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं।
2)भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:झारखंड की भाषा और संस्कृति का संरक्षण: एक आवश्यक प्रयास
झारखंड की कवयित्री अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की जरूरत पर जोर दे रही हैं। उनका कहना है कि बाहरी भाषाओं के प्रभाव से झारखंडी बोलियाँ और संवाद शैली अपनी पहचान न खो दें। यह सिर्फ भाषा का मसला नहीं, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का सवाल है।
किसी भी समाज की भाषा उसकी संस्कृति का आइना होती है। इसमें उस इलाके का इतिहास, परंपराएँ और जीवन-दर्शन झलकता है। जब भाषा का मूल रूप बदलने लगता है, तो संस्कृति भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। कवयित्री की यह चिंता सही है, क्योंकि भाषा के खत्म होने से पूरी सांस्कृतिक धरोहर खतरे में पड़ सकती है।
झारखंड की भाषा और संस्कृति को सहेजना सिर्फ अतीत को बचाने की बात नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने की कोशिश भी है। इसे बचाने के लिए स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देना, साहित्य, संगीत और कला के जरिए उन्हें जिंदा रखना और युवाओं को इससे जोड़ना जरूरी है। तभी झारखंड की खास पहचान बनी रहेगी।
3)दिल के भोलेपन के साथ-साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है?
उत्तर:कवयित्री निर्मला पुतुल ने ‘आओ, मिलकर बचाएँ’ कविता में दिल के भोलेपन के साथ-साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर इसलिए बल दिया है क्योंकि वे मानती हैं कि एक स्वस्थ और सशक्त समुदाय के लिए इन तीनों गुणों का संतुलन आवश्यक है।
- दिल का भोलापन: यह सहजता, सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह मानवीय संबंधों की नींव है और समाज में प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। कवयित्री चाहती हैं कि आधुनिक जीवन की जटिलताओं और अविश्वास के माहौल में भी लोगों के भीतर का यह भोलापन बचा रहे।
- अक्खड़पन: यहाँ ‘अक्खड़पन’ नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि अपनी बात पर दृढ़ रहने, अपने मूल्यों और अधिकारों के लिए खड़े होने के साहस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवयित्री मानती हैं कि केवल भोलापन होने से शोषण और अन्याय का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, अपने हक के लिए अड़ने और गलत के सामने झुकने से इनकार करने का स्वभाव भी ज़रूरी है।
- जुझारूपन: यह संघर्षशीलता, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने की क्षमता का प्रतीक है। कवयित्री जानती हैं कि आदिवासी समुदाय को अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए, उनके भीतर जुझारूपन की भावना का बने रहना आवश्यक है ताकि वे विपरीत परिस्थितियोंभी हार न मानें और अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहें।कवयित्री का मानना है कि इन तीनों गुणों का सही समन्वय ही एक संतुलित और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकता है। केवल भोलापन दुनिया के धोखेबाजों से रक्षा नहीं कर सकता, जबकि केवल अक्खड़पन और जुझारूपन रिश्तों में कटुता ला सकता है। इसलिए, दिल के भोलेपन के साथ-साथ अन्याय के खिलाफ अक्खड़ता दिखाने और अपने लक्ष्यों के लिए जुझारू बने रहने की आवश्यकता है ताकि समुदाय अपनी सहजता, स्वाभिमान और संघर्ष क्षमता को बनाए रख सके।
4)प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है?
उत्तर –कविता सीधे आदिवासी समाज की बुराइयाँ नहीं बताती। पर हाँ, ये ज़रूर इशारा करती है कि उनका भोलापन का फ़ायदा उठाया जा सकता है, उनका अक्खड़पन ज़्यादा झगड़ा करा सकता है, लड़ने की हिम्मत कम हो सकती है, अपनी भाषा-संस्कृति खो सकती है और प्रकृति से दूर हो सकते हैं। कविता इन अच्छी चीज़ों को बचाए रखने की बात करती है ताकि वे मज़बूत बने रहें।
5)‘इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है’-से क्या आशय है?
उत्तर:यह पंक्ति सच में आशा का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि आज की चुनौतियों के बावजूद, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, मानवीय मूल्य और प्रकृति जैसी अनमोल चीजें अब भी मौजूद हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम उन्हें पहचानें, महत्व दें और एकजुट होकर उनका संरक्षण करें, ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। यह निष्क्रिय रहने की बजाय सकारात्मक बदलाव के लिए मिलजुल कर प्रयास करने का आह्वान है।
6)निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य-सौंदर्य को उदघाटित कीजिए
(क) ठंडी होती दिनचर्या में
जीवन की गर्माहट
(ख) थोड़ा-सा विश्वास
थोडी-सी उम्मीद
थोड़े-से सपने
आओ, मिलकर बचाएँ।
उत्तर:उत्साह और आशा: जीवन को ऐसे सहेजें
यह सार बताता है कि कैसे हम अपनी नीरस होती दिनचर्या में भी उत्साह और खुशियाँ ढूँढ सकते हैं। “जीवन की गर्माहट” का मतलब है कि हमें अपने जीवन की जीवंतता को रोज़मर्रा के पलों में भी महसूस करना चाहिए।
आगे, “थोड़ा-सा विश्वास, थोड़ी-सी उम्मीद, थोड़े-से सपने— आओ, मिलकर बचाएँ” यह दर्शाता है कि हमें छोटे-छोटे विश्वास, आशा और सपनों को मिलकर सहेजना चाहिए।
संक्षेप में, ये पंक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि सकारात्मक रहें और मुश्किल समय में भी आशा न छोड़ें। ये दर्शाती हैं कि जीवन कितना भी नीरस क्यों न लगे, हम सब मिलकर उसमें रंग भर सकते हैं और उसे सुंदर बना सकते हैं।
7)बस्तियों को शहर की किस आबो-हवा से बचाने की आवश्यकता है?
उत्तर:कवयित्री की पुकार: बस्तियों का बचाव
कवयित्री को शहरीकरण से बस्तियों पर मंडराता खतरा दिख रहा है। उनकी चिंता है कि शहरों की भीड़ और अकेलापन बस्तियों की हरियाली और सामुदायिक भावना को भी खत्म कर रहा है। वे चाहती हैं कि बस्तियाँ शहरी प्रभाव से दूर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय रिश्तों को बचाकर रखें।
कविता के आस-पास
1)आप अपने शहर या बस्ती की किन चीजों को बचाना चाहेंगे?
उत्तर: पुणे अपनी पहचान बनाए रखे, इसके लिए आपके सुझाव सराहनीय हैं. ऐतिहासिक इमारतों, हरियाली, मराठी संस्कृति, शांत जीवनशैली, नदियों की स्वच्छता, सामुदायिक भावना और किफायती आवास पर ध्यान देना पुणे की आत्मा को जीवित रखेगा. यह हम सबके साझा प्रयासों से ही संभव है.
2)आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें।
उत्तर:आदिवासी समाज बदलाव के दौर में ज़रूर है, शिक्षा और जागरूकता बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन गरीबी, कर्ज़ और स्वास्थ्य जैसी मुश्किलें अब भी उनके सामने हैं। यह भी सच है कि विकास के नाम पर उनकी ज़मीन और संस्कृति का नुकसान हो रहा है, जो कि चिंता की बात है।
उनकी असली तरक्की तभी होगी जब उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनकी खास पहचान और पुराने ज्ञान को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा।