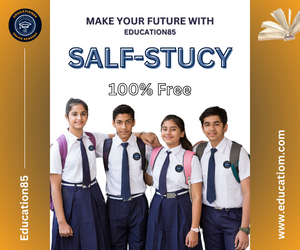सीता स्वयंवर में शिवधनुष को तोड़ने के बाद, राम और लक्ष्मण की मुलाकात भगवान परशुराम से होती है। परशुराम को यह जानकर क्रोध आता है कि किसने शिवधनुष को तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस धनुष को तोड़ा था। राम और लक्ष्मण के साथ उनकी तीखी बहस होती है। परशुराम, राम को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं, लेकिन राम शांति से उनका स्वागत करते हैं और उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। अंततः, परशुराम को राम की शक्ति और विनम्रता का एहसास होता है और वह शांत हो जाते हैं।
प्रश्न- अभ्यास
1. परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए?
उत्तर :
लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि शिवधनुष उन्हें एक साधारण धनुष जैसा ही लगा और राम को इसके महत्व का पता नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राम ने जानबूझकर धनुष को नहीं तोड़ा, बल्कि यह स्वतः ही टूट गया। उन्होंने यह भी कहा कि राम बचपन में कई धनुष तोड़े हैं और उन्हें इस बात का अहसास नहीं था कि यह कोई विशेष धनुष है। इन तर्कों के माध्यम से लक्ष्मण ने परशुराम को समझाने की कोशिश की कि राम ने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया है। लक्ष्मण का मुख्य उद्देश्य परशुराम को शांत करना और अपने भाई राम की रक्षा करना था। उन्होंने सत्य बोलते हुए परशुराम को समझाया कि राम को शिवधनुष के महत्व का पता नहीं था। लक्ष्मण के इन तर्कों के कारण ही परशुराम अंततः शांत हुए और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया।
2. परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएँ हुईं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएँ अपने शब्दों में लिखिए ।
उत्तर :
परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं से उनके स्वभाव की विशिष्ट विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं। राम, अपनी शांति और धैर्य के लिए जाने जाते थे, परशुराम के क्रोध से अचंभित नहीं हुए। उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, परशुराम के ज्ञान और अनुभव को स्वीकार करते हुए। राम का दृष्टिकोण ज्ञान, संयम और धर्म के गहन समझ पर आधारित था। इसके विपरीत, लक्ष्मण, अपनी वीरता और भाई के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, अधिक आवेगी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने परशुराम को चुनौती देकर अपने भाई की रक्षा के लिए दृढ़ता दिखाई। लक्ष्मण का दृष्टिकोण साहस, वीरता और अन्याय के प्रति असहिष्णुता से प्रभावित था। दोनों भाइयों ने अपने-अपने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया – राम की शांति और संयम, और लक्ष्मण का साहस और वीरता। यह प्रकरण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांति और दृढ़ता दोनों के महत्व को उजागर करता है।
3. लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए।
उत्तर :
परशुराम: “हे राजकुमार! तुमने शिवधनुष को तोड़कर एक महान अपराध किया है। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलना चाहिए!”
लक्ष्मण: “हे मुनि! क्या आपने कभी बचपन में कोई खिलौना तोड़ा नहीं? हम तो छोटे बच्चे हैं, हमने जान-बूझकर ऐसा नहीं किया।”
परशुराम: “तब तुमने धनुष को तोड़ने से पहले इसकी महत्ता क्यों नहीं पूछी?”
लक्ष्मण: “हे मुनि! धनुष तो धनुष ही होता है। क्या हर धनुष को तोड़ने पर इतना क्रोध करना चाहिए?”
परशुराम: “यह कोई साधारण धनुष नहीं था! यह शिवजी का धनुष था।”
लक्ष्मण: “शिवजी तो महान देवता हैं। वे हमारे क्रोध से नाराज नहीं होंगे।”
4. परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या-क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए-
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । बिस्वबिदित क्षत्रियकुलद्रोही ।।
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ।।
सहसबाहुभुज छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा ।।
मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर ।
गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ।।
उत्तर :
इस पद्यांश में परशुराम ने अपने बारे में कहा है कि वे एक बाल ब्रह्मचारी हैं और क्षत्रियों के कुल के शत्रु हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कराया है। उन्होंने सहस्त्रबाहु जैसे शक्तिशाली राजा को भी मार डाला था। उन्होंने अपने इस फरसे का वर्णन करते हुए कहा कि यह इतना भयानक है कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। इस पद्यांश के माध्यम से परशुराम ने अपनी शक्ति, क्रोध और क्षत्रियों के प्रति घृणा को व्यक्त किया है। उन्होंने खुद को एक महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है जिन्होंने क्षत्रियों का सर्वनाश किया है। यह पद्यांश हमें परशुराम के चरित्र के बारे में बताता है कि वे क्रोधी स्वभाव के हैं, अहंकारी हैं, क्षत्रियों से नफरत करते हैं और धार्मिक कर्मठ हैं। यह पद्यांश हमें रामायण के उस संदर्भ को समझने में मदद करता है जब परशुराम राम को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। परशुराम का यह अहंकारी और क्रोधी स्वभाव ही इस संघर्ष का कारण बनता है।
5. लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या – क्या विशेषताएँ बताईं ?
उत्तर :
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक सच्चा योद्धा विनीत होता है और अपनी वीरता का ढिंढोरा नहीं पीटता। वह धैर्यवान होता है और आवेश में आकर कोई भी काम नहीं करता। एक सच्चा योद्धा अहिंसक होता है और निर्दोषों को कभी हानि नहीं पहुँचाता। वह सभी का सम्मान करता है, चाहे वे शत्रु ही क्यों न हों। एक वीर व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और हमेशा सत्य और न्याय का साथ देता है। वह अपनी शक्ति पर कभी अभिमान नहीं करता। लक्ष्मण ने यह भी कहा कि एक सच्चा योद्धा ब्राह्मणों, गायों और निर्दोष लोगों पर कभी अपना बल नहीं दिखाता। वह हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है। लक्ष्मण के अनुसार, एक सच्चा योद्धा अपनी वीरता को अपने कार्यों से सिद्ध करता है, न कि शब्दों से। वह शांतिपूर्ण रहता है और केवल युद्ध के मैदान में ही अपना पराक्रम दिखाता है।
6. साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए।
उत्तर :
“साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है” – यह कथन जीवन के एक मूल सत्य को प्रतिबिंबित करता है। साहस और शक्ति हमें चुनौतियों का सामना करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की जटिलताओं को पार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये गुण हमें मजबूत बनाते हैं और हमें कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि, अकेले शक्ति अहंकार को जन्म दे सकती है और दूसरों को दबा सकती है। विनम्रता इस शक्ति को संतुलित करती है। यह हमें दूसरों का सम्मान करने, उनके विचारों को महत्व देने और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करती है। जब साहस, शक्ति और विनम्रता एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति एक सच्चा नेता बन जाता है। वह दूसरों को प्रेरित कर सकता है, चुनौतियों का सामना कर सकता है और समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे महान नेताओं ने साहस, शक्ति और विनम्रता का सफल समन्वय किया। उनके जीवन ने हमें सिखाया कि विनम्रता शक्ति को दिशा देती है और उसे सार्थक बनाती है।
7. भाव स्पष्ट कीजिए-
(क) बिहसि लखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनीसु महाभट मानी ।।
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूँकि पहारू ।।
(ख ) इहाँ कुम्हड़बतिया कोड नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं । ।
देखि कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना ।।
उत्तर :
8. पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर दस पंक्तियाँ लिखिए।
उत्तर :
तुलसीदास जी की भाषा का सौंदर्य उनकी रचनाओं में अद्वितीय है। उन्होंने सरल और सहज अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जो जन-जन तक आसानी से पहुंचती है। उनकी भाषा में भावुकता और संगीतात्मकता का सम्मिश्रण है, जो पाठक को गहराई से प्रभावित करता है। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से जीवंत चित्रण किए हैं और अनेक अलंकारों का प्रयोग कर अपनी भाषा को और भी समृद्ध बनाया है। उनकी भाषा में ध्वन्यात्मकता भी विद्यमान है, जहां शब्द अर्थ के साथ-साथ गहन भावों को भी व्यक्त करते हैं। तुलसीदास जी की भाषा में भक्ति भावना की गहरी धारा बहती है, जो पाठकों को भगवान राम के प्रति आकर्षित करती है। इस प्रकार, तुलसीदास जी की भाषा सरलता, भावुकता, संगीतात्मकता और आंचलिकता के सम्मिश्रण से युक्त है, जिसने उनकी रचनाओं को अमर बनाया है।
9. इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर :
(क) देव दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं, उनके परिवार और दरबारी समाज को प्रसन्न करने के लिए आकर्षक और चमकदार चित्रण प्रस्तुत किए। उनके काव्य में जीवन के दुःखों का नहीं, बल्कि वैभव-विलास और सौंदर्य का वर्णन मिलता है। उनके सवैयों में कृष्ण का दूल्हा-रूप चित्रित है, तो कवित्तों में वसंत और चाँदनी को राजसी वैभव और विलास से समृद्ध दिखाया गया है।
(ख) देव की कविताओं में कल्पना-शक्ति का अद्भुत विलास दिखाई देता है। वे नवीन कल्पनाएँ प्रस्तुत करते हैं। वृक्षों को पालना, पत्तों को बिछौना, फूलों को झिंगूला, वसंत को बालक और चाँदनी रात को आकाश में बना ‘सुधा-मंदिर’ कहना उनकी सृजनात्मकता का परिचायक है।
(ग) देव ने अपने काव्य में सवैया और कवित्त छंदों का प्रयोग किया है। ये दोनों ही छंद वर्णिक हैं और छंद की कसौटी पर देव पूर्णतः खरे उतरते हैं।
(घ) देव की भाषा संगीत, प्रवाह और लय के दृष्टिकोण से अत्यंत मनमोहक है।
(ङ) देव ने अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे अलंकारों का सहज और स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है।
(च) उनकी भाषा में कोमलता और मधुरता से भरपूर शब्दों का चयन किया गया है।
10. निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए-
(क) बालकु बोलि बधौं नहि तोही ।
(ख) कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा ।
उत्तर :
(क) ‘ब’ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार।
(ख) कोटि-कुलिस – उपमा अलंकार।
कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। – उपमा अलंकार।
रचना और अभिव्यक्ति
11. “सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर- निवृत्ति का उपाय ही न कर सके।”
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता बल्कि कभी-कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए ।
उत्तर :
मेरा मानना है कि क्रोध एक जटिल भावना है। यह एक तरफ जहां अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देता है, वहीं दूसरी तरफ यह हिंसा और विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए, क्रोध को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें क्रोध को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि एक हथियार के रूप में।
12. अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएँ लिखिए ।
उत्तर :
मेरा एक मित्र है, जिसका नाम रोहन है। रोहन बेहद शांत स्वभाव का है। वह शायद ही कभी घबराए या उत्तेजित हो, भले ही परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। यह शांति उसके दूसरों के साथ के व्यवहार में भी परिलक्षित होती है, जिससे वह एक धैर्यवान और समझदार श्रोता बनता है। रोहन अत्यंत ही अवलोकनशील भी है, वह अक्सर ऐसे विवरणों को नोटिस करता है जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। उसे अपनी क्षमताओं पर एक शांत आत्मविश्वास है और उसके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति उसे समस्याओं को स्पष्ट और केंद्रित मन से देखने और रचनात्मक एवं प्रभावी समाधान खोजने में सहायता करती है।
13. दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए- इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए।
उत्तर :
दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए
एक छोटे से गाँव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह हमेशा कक्षा में सबसे पीछे रह जाता था। उसके शिक्षक और साथी छात्र उसे मूर्ख कहते थे। मोहन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता था।
एक दिन, गाँव में एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। मोहन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। जब उसके दोस्तों ने सुना तो उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा, “तू तो पढ़ाई में भी फेल हो जाता है, तू चित्रकला में क्या करेगा?”
मोहन ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और चुपचाप घर चला गया। उसने रात भर चित्र बनाने में लगा दी। अगले दिन, उसने अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता में जमा कर दी। सभी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने मोहन की पेंटिंग देखी। उसकी पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी। सभी ने उसकी तारीफ की।
मोहन ने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। उस दिन मोहन ने सबको यह साबित कर दिया कि उसे कम आंकना गलत था।
14. उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो ।
उत्तर :
“एक बार स्कूल में, कक्षा में एक लड़के को अन्य छात्र लगातार चिढ़ा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह बहुत दुखी लग रहा था और रोने लगा। मैंने देखा कि वह अकेला और असहाय महसूस कर रहा है। मैंने उस लड़के के पास जाकर उससे बात की और उसे समझाया कि वह अकेला नहीं है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैंने उन छात्रों को भी समझाया कि उनका व्यवहार गलत है और किसी को भी इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बाद, मैंने उस लड़के को अन्य छात्रों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया।”
15. अवधी भाषा आज किन-किन क्षेत्रों में बोली जाती है?
उत्तर :
उत्तर प्रदेश: अवध क्षेत्र के अधिकांश जिले जैसे लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती तथा फतेहपुर 1 में अवधी भाषा बोली जाती है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से: अवधी भाषा का प्रभाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है।